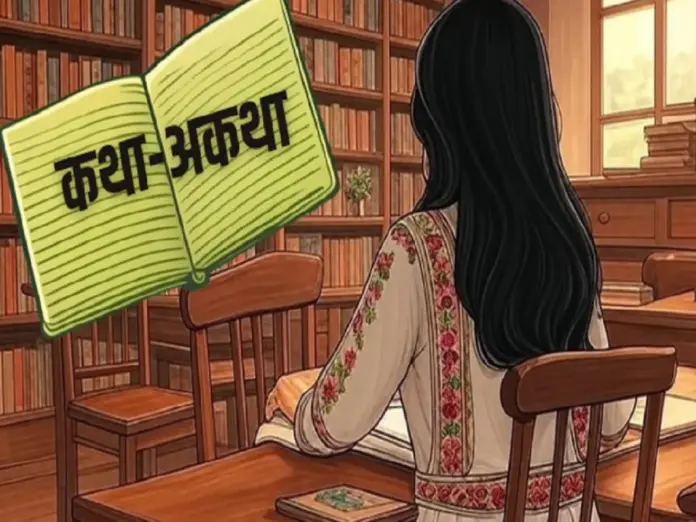आज 140 करोड़ भारतीय, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस ऐतिहासिक जीत पर नतमस्तक हैं। यह भारत की महिलाओं की जीत है। छोटे गांवों और गरीब घरों से निकली ये लड़कियां अब भारत की करोड़ों महिलाओं में उत्साह का संचार कर देंगी और उन्हें इस बात के लिए हमेशा प्रेरित करेंगी कि मुश्किलें चाहे कितनी भी आ जाएं हिम्मत नहीं हारनी है।
लेकिन एक लम्बी अंधेरी सुरंग को पार करने के बाद उन्हें मिली है यह उजली-धुली सुबह। सत्तर-अस्सी के दशक तक महिला क्रिकेटरों को पेशेवर न मानते हुये, उन्हें नौसिखुए या फिर शौकिया खिलाड़ियों की तरह ट्रीट किया जाता था। उनके पास न ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त जगह होती थी, न माहौल और न अच्छे ट्रेनर। उनके पास पूरी किट नहीं होती थी, सबका बल्ला नहीं होता था। उन्हें ठहरने को होटल नहीं मिलते थे, वे अपना बेडिंग साथ लेकर चलती थीं। और यहां बात सिर्फ साधनों के अल्पता या न्यूनता भर की नहीं थी, सम्मान और समानता की कमी उन्हें साधनों के कमी से भी ज्यादा खल और तोड़ रही थी।
उन्हें परिवार की मर्यादा के नाम पर, उनके लड़की होने की दुहाई दे देकर, दूसरे घर जाने, अपना परिवार बसाने और उसे बनाये रखने की महत्ता बता-बताकर हर कदम पर रोका और टोका गया। उनके कदम- कदम पर कांटें ही नहीं बिछाये गयें ,खाइयां भी खोदी गयीं। लेकिन यह उनकी हिम्मत ही थी कि वे फिर भी रुकी नहीं, पीछे नहीं मुड़ी, किसी हार को उन्होंने सर चढकर बोलने नहीं दिया। तो अंतत: यह तय था कि अन्य तमाम क्षेत्रों और खेलों की तरह यहां भी उनके नाम की तूती बोलनी ही थी। यह जीत प्रतीकात्मक तो है ही, एक पूरी विकास यात्रा का भी द्योतक है।.
परंपरा के नाम पर थोपी जानेवाली सारी रूढ़ियाँ वस्तुतः स्त्रियों की योग्यता और उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को चहारवारी के भीतर कैद कर देने की एक पूर्व नियोजित योजना होती है। सबसे बड़ा यही कारक है कि हमारे देश के विकास की गति इतनी क्षीण है क्योंकि हमारा समाज अपने देश की आधी आबादी का, उसके शारीरिक-मानसिक श्रम का उचित इस्तेमाल ही नहीं करता। परंपरा, धर्म, रीति-रिवाज आदि के नाम पर स्त्रियों को घर की देहरी के भीतर कैद रखना और देखना पितृसत्ता की साजिश है। जो स्त्रियाँ खुद से लड़-भिड़कर, समाज के सारे ताने सहते हुये आगे आती हैं, अपने अस्तित्व का दावा करती हैं, इस समाज में उनके शारीरिक-मानसिक श्रम को कम करके आँका जाता है। उनके कार्य का उचित मूल्य और अवदान उन्हें नहीं मिलता क्योंकि वो एक स्त्री है।
दूसरी बेड़ी जो डलती है उनके पांव में, या फिर जिसमें वे एक मेंटल कंडीशनिंग के तहत खुद ही बंधती जाती है, वह प्यार के नाम की होती है। परिवार के नाम की होती है।
गीता में एक जगह ये कहा गया है-‘ प्रेम एक ऐसी भावना है जिसमें त्याग और निस्वार्थता हो। इसमें किसी को पाने की चाहत नहीं होती, बल्कि उसमें खो जाना होता है, खुद को उसे दे देना या सौंप देना भी। प्रेम में किसी को बांधने की ज़रूरत नहीं होती। प्रेम में त्याग करने से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं।
मूल रूप से ‘प्रेम’ का मतलब यह होता है कि अब कोई और है जो आपके लिए आपसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। जब आप वाकई किसी के प्रेम में होते हैं तो आप अपना व्यक्तित्व, अपनी पसंद-नापसंद, अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही हम किसी से प्रेम करने लगते हैं तो उसकी हर जरूरत, हर पसंद के अनुसार खुद को ढालने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन साथ ही यह भी कि यह प्रेम आपको अपने भीतर के चक्रवात में खींचता चला जाता है। आप लाचार होते हैं। अपने मन से मजबूर भी। आप पर आपका वश नहीं चलता।
जब आप प्रेम में डूब जाते हैं तो आपके सोचने का तरीका, आपके महसूस करने का तरीका, आपकी पसंद-नापसंद, आपका दर्शन, आपकी विचारधारा सब कुछ बदल जाती है। प्रेम अपने आप में एक शानदार रूपान्तरण कि प्रक्रिया है। प्रेम में जब व्यक्ति होता है तो वह अपना सर्वोत्तम संस्करण होता है। क्योंकि इस तरह आप लचीले होते जाते हैं। प्रिय की बेहतरी के लिए आपका हर कदम हुआ जाता है। स्त्रियों ने तो जरूर इसे आत्मसात कर लिया, लेकिन इसे समझने और ग्रहण करने में पुरुषों को अभी भी समय लगनेवाला है।
लेकिन जैसे ही स्त्रियां ये कहती या स्वीकार करती हैं- ’मैं तुमसे प्रेम करती हूं’, अपनी पूरी आजादी खो देती है। आपके पास जो भी है, आप उसे खो देती हैं। जीवन में आप जो भी करना चाहती हैं, अब आप बिला-शर्त वह नहीं कर सकतीं। ‘बेल हुक्स अपनी किताब ‘ऑल अबाउट लव’ में कहते हैं- ‘पुरुष प्रेम के बारे में ‘लिखते’ हैं पर स्त्रियाँ प्रेम को ‘जीती’ हैं। अधिकतर पुरुषों को पता है कि प्रेम पाना क्या होता है, क्योंकि उन्हें प्रेम ‘मिलता’ है, मिलता रहा है। वहीं दूसरी ओर स्त्रियां अक्सर प्रेम पाने की उम्मीद में तरसती हैं, उन्हें प्रेम ‘मिलता’ नहीं। बल्कि उनसे अक्सर प्रेम ‘देने’ की उम्मीद की जाती है। ‘ इस किताब के एक छोटे से हिस्से का यह अनुवाद क्या किसी भी यथार्थ से कहीं बड़ा और गाढ़ा यथार्थ नहीं?
एक स्त्री की खातिर प्रेम और गृहस्थी और उसकी स्वाधीनता दोनों जितने धुर विरोधी शब्द हैं, उतने ही ज्यादा उसके जीवन का पूरक याकि मानक आधार। उनका सपना कह लीजिये इसे याकि यूटोपिया भी… एक स्त्री प्रेम चाहती है जीवन में। एक चुटकी भर आजादी भी। जिसमें अपने होने का अहसास, किसी का उसके लिए अपना होने का अहसास, अपने एक निजी स्पेस की कामना, जिसे वह अधिकतर अपने घर की कामना के रूप में व्यक्त करती याकि करना चाहती है भी शामिल होता है। इसी कामना और चाहना के इर्द-गिर्द बीतता और भटकता रहता है उसका तमाम जीवन।
लेकिन स्त्रियों को ये एक साथ अधिकतर नहीं मिलता। उसके लिए ‘प्रेम’ का यह घर सचमुच ‘खाला का घर नाही‘ होता है। अक्सर उसे इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, अब यह उसका चुनाव है कि वह क्या चुनती है। चुटकी भर स्पेस, याकि एक सुरक्षित चहारदीवारी? दोनों में से कुछ भी आसान नहीं और दोनों ही स्थिति मुश्किल है। चुटकी भर आजादी की कीमत जहां ढेरों असुरक्षा, असुविधा, अनिश्चित भविष्य आदि-आदि होते हैं वहीं पारिवारिक जीवन और तथाकथित प्यार की उपलब्धता की शर्त है, मुफ्त की चाकरी, ताने-उलाहने, जिम्मेदारियाँ और उसके श्रम और संयम को सहज उपलब्ध समझ कर बिना किसी झिझक और शर्म के ग्रहण किए चले जाने का अशेष चक्र। ये दोनों हीं स्थितियाँ दारुण हैं।
डूबकर प्रेम करने उसमें बार-बार छले जाने के बावजूद ये स्त्रियां प्रेम से अपना भरोसा और विश्वास नहीं खोती। ये अगनपाखी स्त्रियां प्रेम में तिल-तिल करके जीती हैं।मर-मरकर जीती हैं। और फिर शुरू होती है उनके जीवन में प्रेम की वही तलाश। प्रेम उनके जीवन की वह धूरी है, वो दिवा-स्वप्न, जिसे पाये बिना उनका जीवन अकारथ है।
परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व, प्यार-परिवार और स्वतंत्रता का द्वैत दरअसल स्त्रियों को एक खास परिधि के भीतर देखने की पारंपरिक जिद और स्त्रियों द्वारा अपनी आजादी और अस्तित्व की लड़ाई के लिए खड़े होने और उसके लिए संघर्ष का द्वंद है। परंपरा और आधुनिकता के बीच नैतिकता जैसे मूल्य हमेशा से हीं मौजूद रहे हैं। नैतिकता का कोई निश्चित पैमाना नहीं होता। समाज, व्यक्ति याकि समुदाय अपने-अपने ढंग से अपनी नैतिकता तय करते आए हैं। सोचिए कि जो एक के लिए नैतिक है, वो दूसरे के लिए अनैतिक कैसे हो सकता है?
नैतिक-अनैतिक, परंपरा और आधुनिकता या फिर मूल्यों की स्थापना और उसके विखंडन की बातें अपनी जगह पर जायज हैं। पर जमाने से दबाई गयी औरतों का अपने मन का कुछ चुन याकि कर पाने की सांघातिक विकलता में छिपे बदलाव के बीजों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता।
परंपरा और आधुनिकता को समझने के बहुत सारे संदर्भ हो सकते हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख संदर्भ स्त्री-पुरुष-संबंध है, उसमें आनेवाले बदलाव हैं। किसी भी समाज में परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व वहाँ के सामाजिक परिवर्तन में स्पष्ट देख जा सकता है। सच तो यह है कि जिस समाज में औरत और उसकी यौन-शुचिता को देखने और समझने के नैतिक आग्रह ज्यादा गहरे हैं, उसके पास आधुनिकता का जवाब देने के लिए कोई सही तर्क या वैचारिक औज़ार उतने ही कम हैं। इसलिए वे तर्क की अनुपलब्धता में औरतों पर और ज्यादा प्रतिबंध लगाकर, उनके प्रति कड़ा, क्रूर, विद्वेषपूर्ण और हिंसक रवैया अपनाकर उन्हें अपने काबू में रखने की जिद पर ज्यादा आमादा दिखते हैं।
हिंदू स्त्री का जीवन’ में पंडित रमाबाई कहती हैं- ‘जीव जन्तु से लेकर पेड़-पौधों तक में प्रकृति की यह मांग है कि सभी जीवित प्राणी स्वतंत्र रूप से अपनी वृद्धि की परिस्थितियों के साथ अनुकूल विकास करें, अन्यथा वे अपने उस रूप को नहीं पा सकेंगे, जो मूलतः उनका आकार है। फिर इस नियम का उल्लंघन क्यों? औरतें हीं परदे में क्यूँ रहें? घर की चहारदीवारी में सीमित अपनी पूरी ज़िंदगी खुली हवा में सांस न ले पाने को मजबूर, वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी कमजोर होती जाती हैं। उनकी शारीरिक बनावट क्षीण से भी क्षीणतर होती जाती है। उनकी भावनाएं समाज के अंधविश्वासों एवं मान्यताओं के बोझ तले दब जाती हैं और उनका मस्तिष्क किसी भी तरह के विचारों एवं ज्ञान से वंचित रह जाता है। जिससे वह विश्व को देखने और समझने के काबिल नहीं रह जाती हैं।‘
सच कहें तो सामान्य तौर पर आधुनिकता एक प्रक्रिया है- नवीन के सतत खोज याकि नए के आगमन की। यह समय सापेक्ष भी है, व्यक्ति सापेक्ष भी। आज जो नवीन है वो कल नवीन नहीं रहेगा। पुरातन हो जाएगा। उस पुरातन में से भी बेहतर को संभाले रखना और रूढ़ को छोडते जाना ही आधुनिकता है।
‘आधुनिकता की पहली और अनिवार्य शर्त स्व-चेतना है। ‘स्व-चेतना’ को पहचान लेने और जान लेने वाली स्त्रियाँ किसी जड़ समाज के लिए प्रश्न्चिह बनकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी चेतना, उनके प्रश्न किसी ठहरे हुये समाज के लिए भयावह और डरावने होते हैं, यदि सभी स्त्रियाँ ऐसी ही हो गईं तो…? यदि सभी ऐसे ही सवाल करने लगीं तो…? इसका एक ही जबाब होता है उनके पास -इन औरतों के मनोबल को तोड़ने की कोशिश…इनमें दहशत और कुंठा भरने की जिद… यह उनके झुझलाहट और बेचैनी के सिवा और क्या है? यह पुरुषवादी समाज का डरा हुआ चेहरा है, जो अपनी कमजोरी को क्रूरता और नृशंसता के औजारों से ढकना चाहता है। ये वो ही लोग हैं, जिन्हें स्त्री के आधुनिक सोच से, उसकी आधुनिकता से भय लगता है।
यह सही है कि न तो आधुनिकता में सबकुछ श्रेयस्कर है और न ही परंपरा में सबकुछ निकृष्ट। लेकिन इनदोनों के बीच का संतुलन और समाहार ही हमें सच्चे अर्थों में कहीं आधुनिक होने की ओर ले जाता है। इसके लिए जो विवेक और दृष्टि चाहिए वह स्वयं से लगातार जिरह करने से, लड़ते और जूझते रहने से आता है। कोई द्वंद्वहीन व्यक्ति आधुनिक नहीं हो सकता। द्वंद्वहीन होकर परम्पराओं का अनुसरण करना किसी आधुनिक समाज की निशानी नहीं हो सकती। पुरातन की दुष्प्रवृत्तियों से मुक्ति और उनकी अच्छाइयों के संरक्षण के बीच सामंजस्य की जरूरत ही आधुनिकता है।
किसी शायर ने यह ठीक ही कहा है कि ‘अबके सफर में दर्हद के पहलू अजीब है/ जो लोग हमखयाल न थे, हमसफर हुये।’आज अधिकतर शादियां ऐसी ही होती हैं। लोग हमसफर तो होते हैं पर हमखयाल नहीं। हमखयाल होने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि रिश्ता दोस्ती का हो, बराबरी का हो।हर रिश्ता एक सामंजस्य और सहभागिता खोजता है। लेकिन मैं यह भी मानती हूं कि विवाह अगर सही न हुआ, (जोकि अक्सर नहीं ही होता है) तो वह स्त्री के लिए जीते जी रौरव नर्क है। फिर झेलते रहने और उसमें मरते दम तक घुटते रहने के सिवा साधारण स्त्रियों के पास और कोई चारा नहीं बचता है।
मैं सिर्फ तोड़ने में भरोसा नहीं रखती और न किसी को इसका सलाह दे सकती हूं…खासकर तब जबकि खुद ही इस संस्था का हिस्सा हूँ। विवाह ही नहीं, दुनिया का कोई भी संबंध टूटना नहीं चाहिए। संबंध के बीच आये व्यतिक्रम को यदि परस्पर संवाद और सहमति से सुलझा लिया जाय तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? पर, तमाम कोशिशें करने के बाद भी यदि स्थितियां बेहतर नहीं होतीं तो मैं विच्छेद या अलगाव के निर्णय के साथ खड़ी होना चाहूंगी। अलगाव के बाद उस सम्बन्ध के हितधारकों के हितों की सुरक्षा के सवाल भी यहाँ जरूरी हैं।
उनके पास जिनके पास न कोर्ट कचहरी जाकर अपने हिस्से की लड़ाई लड़ने की ताकत है और न उतने पैसे। सम्भव है यह स्थिति कुछ पुरुषों की भी होती हो, पर सामान्यतः स्त्रियां ही इसकी भुक्तभोगी होती हैं। ऐसी स्थिति में मुझे साहिर लुधियानवी हमेशा याद आते हैं-‘तआल्लुक बोझ बन जाये तो उसको छोड़ना बेहतर/तआर्रुफ रोग बन जाये तो उसको भूलना अच्छा/वो अफसाना जिसे तकमील तक लाना न हो मुमकिन। उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।’ पर अधिकतर तो यही होता है कि वह मोड़ खूबसूरत कभी नहीं होता, बदसूरत से भी कहीं ज्यादा किसी बदनुमा दाग की तरह टंका रहता है दोनों के चेहरे पर, मन पर।
मेरे लिए पूरा पुरुष वर्ग मेरा दुश्मन नहीं, वहां मेरे साथी और सहयात्री भी हैं। इसलिए ब्रेकअप से ज्यादा जोर मैं प्री प्रीवेंटिग और मेंटिनेंस पर दूंगी। विवाह संस्था का विकल्प खोजने की बजाय उसकी टूट फूट और दरारों की मरम्मत तथा कटे-फटे हिस्से की रफू और तुरपाई की जरूरत आज ज्यादा है, इसके लिए जरूरी है कि लड़ाई पितृसत्ता से हो न कि पुरुषों से। दोस्त और साथी पुरुषों को खोजना और चिन्हित करना इसके लिए बहुत ही जरूरी है।और सबसे जरूरी है वैसे रिश्ते की तलाश जहां शादी भी मुहब्बत की नींव पर खड़ी हो। ‘जिस तअल्लुक में न हो मुमकिन तलाक/हो मुहब्बत, वो कोई शादी नहीं।’
मैं अपने और अपने जैसी तमाम दूसरी स्त्रियों के अनुभव के आलोक में यह कह सकती हूं कि वर्तमान स्वरूप में ‘लिव इन’ विवाह संस्था का कोई मुकम्मल विकल्प नहीं है, न हो सकता है। हाँ, कई बार यह यह एक तात्कालिक व्यवस्था या जरूरत अवश्य हो सकती है, जिसमें रहते हुए अपने साथी को जाना, समझा और कुछ हद तक परखा जा सकता है। हालांकि हमारी सामाजिक और वैवाहिक व्यवस्था को देखते हुये यह भी कोई छोटा कदम नहीं। जरूरी नहीं कि मेरा अनुभव सबका अनुभव हो, पर स्वयं ‘लिव इन’ में रहते हुये हमने इस विकल्प की सुविधाओं के साथ इसकी चुनौतियों और दिक्कतों को भी नजदीक से महसूस किया है।
वरिष्ठ लेखिका मन्नू जी (मन्नू भंडारी) ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था मुझसे- ‘न कुंआरी रहना विकल्प है, विवाह संस्था का, न लिव इन में रहना। इसके दूरगामी प्रभावों को सोचो…सभी लड़कियां अगर शादी से इंकार करती गयीं तो एक दिन मानव जाति और दुनिया ही खत्म समझो! और अगर ‘लिव इन’ में रहीं तो रिश्ता टूटने पर बच्चे की जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? स्त्री की ही न? इस क्रांतिधर्मिता का भी आखिरी निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, वही न जो अक्सर असफल शादियों में होता है? उल्टे शादी से निकलने से भी ज्यादा असुरक्षाबोध, दायित्व और आर्थिक तंगियां और जिम्मेदारियां आ जाती हैं उसके हिस्से। ‘ मुझे उनकी ये बात बिलकुल सही लगी थी।
तो जरूरत इतनी भर है कि आनेवाली पीढ़ियों को अपने हक और अधिकार के प्रति सचेत किया जाये। उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाया जाये क्योंकि सिवाय शिक्षा और आत्मनिर्भरता के इस संस्था की खामियों और कमियों से निकलने और जूझने का दूसरा विकल्प नहीं स्त्रियों के सामने।
उन्हें एक ऐसी परवरिश दी जाय जिसमें न सिर्फ उन्हें अपना करियर, जीवनशैली और साथी चुनने की आज़ादी और बराबरी हो, बल्कि किसी कारणवश अपने निर्णय के असफल होने पर उन्हें किसी अपराधबोध या समाजप्रदत्त अकेलेपन से न गुजरना पड़े… संबंध कैसे निभाए जाएं, इस पर बात होनी चाहिए। घुटन कम कैसे की जाए इस पर बात होनी चाहिए। सम्मानजनक अवसरों और सुरक्षा पर बात होनी चाहिए। रास्तों और विकल्पों पर बात होनी चाहिए। नीतियों पर बात होनी चाहिए। व्यापक और व्यावहारिक नजरिए से बात होनी चाहिए। क्योंकि बहुत जरूरी बहस है यह। इस पर लगातार बात होनी चाहिए।ताकि समाज और सरकार की समझ बेहतर हो और सबसे जरूरी बात तो यह कि जब तक बच्चों की जिम्मेदारी राष्ट्र की नहीं होगी, मतलब जब तक समान और मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया नहीं करायी, जाएंगी स्त्री की मुक्ति असंभव है।
यूं भी आज की स्त्रियाँ अपने वजूद को लेकर सजग हो रहीं। अपने स्पेस, अपनी चाहतों और खुशियों को लेकर भी। प्रेम के माने अब उनके लिए वही नहीं, जोकि पहले थे। इन्हें ‘स्व’ की कीमत पर प्रेम नहीं चाहिए। अपनी स्वायत्तता और आजादी की कीमत पर भी नहीं। वे एक दोस्ताना और समादर वाले समाज की कल्पना करती हैं, उसकी चाहना भी। इन्हें न इससे कुछ कम चाहिए और न ज्यादा। जबकि अब भी एक बड़ा तबका पुरुष वर्ग का वही अटका पड़ा है, बल्कि पहले से ज्यादा जिसे स्त्री से ‘सबकुछ’ चाहिए। उसे सुंदर भी होना है, सुशील भी, आज्ञाकारी भी होना है, नौकरीधारी भी। उन्हें परंपरागत भी होना है और मौकानुसार आधुनिक भी। वर्तमान समय में स्त्रियों से हमारी मांग और जरूरतों की फेहरिस्त जितनी लंबी होती गयी, पुरुष के प्यार का फ्रेम उतना ही सिकुड़कर छोटा होता गया है। उनके देय की फेहरिस्त भी उतनी ही कम होती गयी। स्वार्थ और अहं उतना ही प्रबल।
इस मानसिकता में बदलाव की जरूरत सबसे पहले है, वर्ना एकाकी होने और रह जाने की त्रासदी सिर्फ स्त्रियों के ही नहीं पुरूषों के हिस्से भी आयेगी।
क्योंकी अब स्त्रियां भी ये समझने लगी हैं कि उस कस्तूरी को भला बाहर-बाहर, क्या ढूंढना, जो दरअसल उनकी ही नाभि में है। प्रेम पात्र मिल जाये, हमसफर यदि मिलता है, साथ चलता है तो बेहतर। वरना खुद के लिए ही जीना और खुद से प्यार करना उनके लिए एक सर्वश्रेष्ठ चुनाव है।