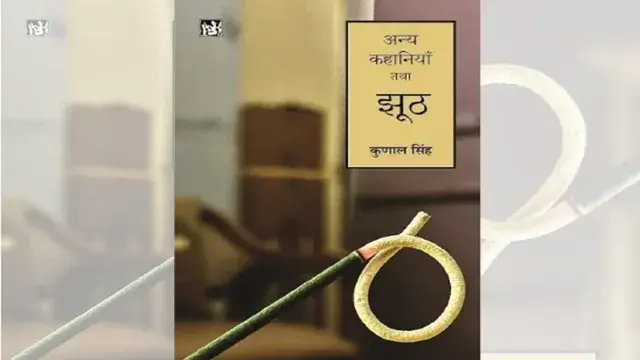स्पेनिश कथाकार इसाबेल एलिंदे कहती हैं, कहानियाँ कई तरह की होती हैं। कुछ का जन्म उन्हें सुनाते समय होता है और भाषा ही इनकी जान होती है। जब तब कोई इन्हें शब्दों में नहीं ढालता, वे महज़ एक आभास, एक हल्का-सा आवेग, एक बिंब या फिर अस्पष्ट याद-सी होती हैं। कुछ दूसरी कहानियाँ मुकम्मल होती हैं, किसी समूचे सेब जैसी, जिन्हें अर्थ बदले जाने का ख़तरा उठाए बग़ैर, अनंत काल तक बार-बार दोहराया जा सकता है। कुछ कहानियाँ यथार्थ की सच्चाई से ली गई होती हैं और प्रेरणा के सहारे इन्हें आकार मिलता है, जबकि कुछ प्रेरणा के किसी एक क्षण में जन्म लेतीं और सुनायी जाने के बाद एकदम सच्ची हो उठती हैं। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ भी होती हैं जो मन की परछाइयों में छिपी रह जाती हैं, किसी जीवाणु की तरह ये हिलती-डुलती हैं और कई बार वक्त के साथ-साथ इनकी बदसूरत सूंडें उगने लगती हैं और आख़िरकार ये ग़ंदगी या परजीवी तत्वों से ढंक जाती हैं। स्मृति के इन प्रेतों को मारने के लिए कभी-कभी उन्हें कहानी की शक्ल में सुनाना ज़रूरी होता है,(सोचो साथ क्या जाएगा, संपादक- जितेन्द्र भाटिया, पहला खण्ड) से।
कुणाल सिंह के संग्रह ‘अन्य कहानियाँ तथा झूठ’ को पढ़ते हुए बार-बार लगा कि उनकी कहानियाँ किसी एक तरह की नहीं हैं। कई बार उनकी कहानियाँ सुनाए जाते समय (लिखते समय) जन्म लेती हैं तो कई बार बाहर की दुनिया में दिखाई दे रहे यथार्थ को ट्रेस करने के लिए वह कहानी के पीछे भागते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वह अपने मन की कन्दराओं में प्रवेश करके पाठक को भी उस प्रेत से मिलवाते हैं, जो उनके भीतर कहानी की शक्ल में बैठा हुआ है।
कुणाल कहानी के परम्परागत शिल्प में यक़ीन नहीं करते, हर कहानी में उनका अपना शिल्प है, जो आख्यान के करीब जान पड़ता है। कह सकते हैं कि कुणाल ने आख्यान को ही शिल्प के रूप में चुना है। कुणाल के पास स्मृतियाँ हैं, स्वप्न हैं, फंतासी है, अध्ययन है, अनुभव है, समय है, अवचेतन है, और चेतन तो है ही। कुणाल इन सबके बीच कहीं कहानी की तलाश करते दिखाई देते हैं। जैसे धुंध में कोई चेहरा पहचानने की कोशिश कर रहे हों। हाँ, इतना साफ़ दिखाई देता है कि वह कोई ऐजेंडा तय करके कहानियाँ नहीं लिखते।
कभी-कभी, ऐसा भी आभास होता है कि उनके पास कहानियों तक जाने की कोई कुंजी है। इसके ज़रिये कभी वह तिलिस्मी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, कभी स्वप्न और फंतासी की दुनिया में। कभी-कभी तो यह भी लगता है कि वह कहानियों की खोज करते हुए कहानी तक पहुँचना चाहते हैं-पहुँचते हैं या नहीं, यह कहा नहीं जा सकता। उनके पास जबरदस्त किस्सागोई है, किस्से हैं, भाषा है, प्रेम है, स्त्री देह है, उसके प्रति आकर्षण है, जीवन है, बदल रहा समाज है, आपसी रिश्तों की सघनता है, बेरोजगारी है…यायावरी है…सबसे महत्वपूर्ण बात इन सबका ‘सिन्क्रोनाइजेशन’ है।
आख्यान की तरह लिखी गई ये कहानियाँ नितांत मौलिक लगती हैं। मौलिकता क्या है? मुझे लगता है मौलिकता का अर्थ यही है कि लेखक ‘फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस’ से कहानियाँ लिख रहा है, बेशक कि उसमें कल्पनाशीलता, स्वप्न और फंतासी का भी प्रयोग किया गया हो। ऐसी कहानियाँ, जो जीवन की परिधि से बाहर खड़े होकर लिखी जाती हैं आमतौर पर बनावटी होती हैं। इतना तय है कि कुणाल की कहानियाँ बनावटी नहीं हैं।
कुणाल की कहानियों के विषय में एक और बात। ‘अन्य कहानियाँ तथा झूठ’ संग्रह की सभी कहानियों का कालखण्ड 2004 से 2011 है। संग्रह की तेरह कहानियों में से सात कहानियाँ 2004-2005 के बीच लिखी गईं। शेष कहानियाँ 2008-9-11 में लिखी गईं। यह वह समय था, जब भारत में आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण और आर्थिक सुधार लागू हुए लगभग डेढ़-दो दशक बीत रहे थे। इस दौरान भारतीय समाज पर इनका प्रभाव भी साफ़ दिखाई देने लगा था।
बेरोजगारी कम होने के बजाय बढ़ रही थी, विदेशी कंपनियों के आने से हमारी संस्कृति में भी खुलापन आ रहा था। फिल्में समाज पर बहुत अधिक प्रभाव डालने लगीं थीं, बल्कि प्रेम भी फिल्मी होता जा रहा था। सोई हुईं यौन इच्छाएँ यकबयक जागृत हो गई थीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात अधिक से अधिक पैसा कमाने की इच्छा सर्वोपरि होती जा रही थी-चाहे इसके लिए विदेश ही क्यों ना जाना पड़े या कुछ भी क्यों न करना पड़े।
इन कहानियों को पढ़ने के लिए पार्श्व में भारतीय समाज में आ रहे बदलावों को ध्यान में रखना होगा। कुणाल की दो कहानियाँ हैं-‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे’ और ‘प्रेम कथा में मौजे की भूमिका का आलोचनात्मक अध्ययन।’ दोनों कहानियाँ इसी परिवेश से उपजी कहानी हैं। पहली कहानी में स्पेनिश सिखाने वाला इंस्टीट्यूट है, युवा लड़के-लड़कियाँ हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे फिल्म का ‘ऑफ्टर इफेक्ट’ है, शाहरुख़ ख़ान के प्रति लड़कियों की दीवानगी है, आपसी संवाद में खुलापन है। लड़कों में सिमरन जैसी प्रेमिकाओं की आकांक्षा है।
ग़ौर फरमाइयेः ‘फ्रैंकली स्पीकिंग, शी इज़ ए बुलशिट!’ पद्माशा बिफिर रही थी। ‘वह बॉस राहुल के साथ…यू नो न! लेकिन यह सब वह शादी से पहले करना ग़लत समझती है, बस इसलिए शादी कर रही है।’‘अरे ऐसा न कहो।’ मैंने कं सोलेशन के स्वर में कहा।
‘नहीं इसे मैं ग़लत नहीं मानती। इस उम्र में किसके साथ ऐसा नहीं होता!’ बायोलॉजिकल नीड है, इसे डिनाई नहीं करना चाहिए। लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि बस इसी वजह से शादी…गॉड!…और तुम कहते हो ऐसा न कहूँ! क्यों न कहूँ जब ऐसा ही है। (पृष्ठ 175)।’ ज़ाहिर है कहानी में एक खुली दुनिया या खुल रही दुनिया है। दफ्तर में आर्थिक मन्दी पर, राजनीतिक निर्णयों, घोटालों, आईपीएल, मल्लिका शेरावत, तसलीमा नसरीन, कास्टिंग काउच पर बातें हैं। यानी भारतीय समाज में यह सब घटित हो रहा था।
कुणाल समाज में हो रहे बदलाव को सलीके से चित्रित करते हैं। इन कहानियों की एक और ख़ास बात है कि इनके नायक-नायिका का खुलासा कुणाल नहीं करते। कहानियों में वह ख़ुद भी मौज़ूद रहते हैं और उनके मित्र भी। कहीं चन्दन है तो कहीं मनोज कुमार पाण्डे। कहानी लगातार खुलेपन की तरफ़ बढ़ती है लेकिन अंत में सामंती मूल्यों और पितृसत्तात्मक मूल्य ही जीत जाते हैं! कहानी में कुणाल के भीतर इन मूल्यों के जीत जाने का डर दिखाई देता है।
दूसरी कहानी ‘प्रेम कथा में मौज़े…’ भी एक युवक से शुरू होती जिसकी उम्र 18 साल के लगभग है, जो कविताएँ लिखता है, जिसके साहित्यिक मित्र हैं और जिसके ईर्दगिर्द लड़कियाँ बनी रहती हैं। नायक (कुणाल) बिपाशा नाम की एक लड़की से प्रेम करने भी लगता है (यह फिल्मी बिपाशा नहीं है)। कहानी के बीच में ही लेखक के मित्र इस कहानी की मार्क्सवादी व्याख्या करते हैं।
यहाँ यह बता देना अनुचित नहीं होगा कि नायक, नायिका के मुकाबले ग़रीब है। नायक अपने मन की इच्छाओं (प्रेम) को प्रकट करने के लिए सलमान रुश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रेन, मिलान कुन्देरा, द बुक ऑफ लाफ्टर एण्ड फोरगेटिंग (अनुवाद कुणाल सिंह), डच उपन्यासकार सेस नोटेबोम के उपन्यास-‘दो प्रेमियों का अजीब किस्सा’ (इसका अनुवाद विष्णु खरे ने किया है) का उद्धरण देते हैं। कहानी के पृष्ठ 143 पर फुटनोट्स में वह लिखते हैं-हालांकि जब की यह कहानी है तब भारत की अर्थ प्रणाली में ‘उदारीकरण’ को लान्च हुए, सात-आठ साल हो चुके थे, लेकिन स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गाँधी जी ने जिस ‘गरीब आदमी’ (साभार, अशोक सेकसरिया) का मॉडल खड़ा किया था और उसके प्रति आस्था और आदर की जो साख थी, वह अभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं हुई थी।
एमएनसीज़ व लाखों के सालाना पैकेज के दौर के शुरू होने में अभी वक्त था और अब भी पैसे ने विद्या को अपदस्थ नहीं किया था-ख़ासकर कलकत्ते में।…यह उद्धरण काफ़ी लम्बा है। आशय यही है कि समाज उस और तेजी से बढ़ रहा था। नायक और बिपाशा की प्रेम कहानी भी आगे बढ़ रही थी। लेकिन मित्रों के साथ जब नायक भी बिपाशा के साथ घूमने जाता है तो नायक मन्दिर में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके मौज़े फटे हुए हैं और सभी दोस्त अपने जूते देखभाल करने वाले को सौंपकर भीतर चले गए हैं।
दरअसल कहानी यहीं हैं। लेकिन कुणाल इकहरी कहानियाँ कम ही लिखते हैं सो इसकी भीतरी परतों का आप स्वयं मूल्यांकन करते रहें या वहाँ तक जा सकते हैं। इसके मार्क्सवादी नज़र से देखें या मोजे फटे होने से नायक के भीतर बैठी हीन भावना से या प्रेम में वर्ग संघर्ष की दृष्टि से! कमोबेश इसी मिज़ाज की कहानी है ‘झूठ तथा अन्य कहानियां।’ यह कहानी भी आख्यान की तरह चलती है। इसमें किशोरावस्था से जवानी की दहलीज़ पर कदम रखते युवा हैं, युवा लड़की है, प्रौढ़ स्त्री है, स्त्री देह को जानने और देखने की इच्छाएँ हैं।
कहानी का नाम कुणाल ने ‘झूठ तथा अन्य कहानियाँ’ क्यों रखा! संभवतः इसलिए कि इस उम्र में युवा लड़के बहुत से झूठ बोलते हैं, इसे कल्पनाशीलता भी कहा जा सकता है। इसके पीछे कहीं प्रेम की खोज होती है तो कहीं स्त्री देह का आकर्षण। नायक नैना को चाहता है, नैना शिबू की बहन है, नैना किसी और को चाहती है, लेकिन नायक को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी नाटकीय अन्दाज़ में खत्म हो जाती है। कहानी में देह के रहस्यों को भरसक खोलने की कोशिश की गई है!
कुणाल की कहानियों की ‘रेंज’ बहुत व्यापक है। कहानी का लोकेल बदलने के साथ ही कुणाल की कहानियों का परिवेश और संवाद भी बदल जाते हैं। ‘डूब’ में पंजाब की दहशत का समय है, तो ‘इतवार नहीं’ में कोलकाता है, ‘उपसंहार’ में एक बार फिर से कोलकाता जीवित हो उठता है तो ‘आखेटक’ में कुणाल सुन्दरवन का सफ़र तय करते हैं।
‘डूब’ एक ऐसी कहानी है, जिसमें दशतगर्दों द्वारा एक परिवार के किशोर का अपहरण होने के बाद का सूनापन है। साथ ही प्रेम की अदृश्य-सी ऐसी रेखाएँ भी हैं, जिनसे कोई ठोस आकार बन सकता था, लेकिन नहीं बन पाया। पंजाब के माहौल के बावज़ूद यह कहानी कहीं से लाउड नहीं होती और घर से अनुपस्थित हो गए, एक किशोर की उपस्थिति को दर्ज़ करती है। ‘आखेटक’ में ऑफिस से ऊब गए नेपाल बाबू जब, मित्रों की सलाह पर सुन्दरवन घूमने जाते हैं। वहाँ मुरशिद से उनकी मुलाक़ात होती है। मुरशिद ‘ऑफ सीजन’ में ‘टूरिस्टों’ को अपना घर किराये पर देता है। गाँव के लगभग सभी लोग अपने घर किराये पर देते हैं। नेपाल बाबू मुरशिद के घर रहने लगते हैं। यहां पता चलता है कि बाघ का शिकार करने की इच्छा लेकर जंगल आए नेपाल बाबू का ‘शिकार’ मुरशिद की भाभी कर लेती है। यह कहानी सुन्दरवन के आसपास के गाँवों में रहने वाले लोगों की उस दयनीय स्थिति को दर्शाती है, जो मजबूरी में टूरिस्टों को अपना घर किराये पर देते हैं, तो उन्हें अपने घर की औरतों को भी उन्हें सौंपना पड़ता है!
‘इतवार नहीं’ एक ख़ूबसूरत कहानी है। नायक एक साहित्यिक पाक्षिक में प्रूफ रीडर है। उसके सामने दो दुनियाएँ हैं-पहली सोमवार से शनिवार के बीच की और दूसरी दूसरी इतवार की दुनिया। पहली दुनिया का जीवन मशीनीकृत है, सुबह साढ़े छह बजे का अलार्म बजना, निबटानादि के बाद नाश्ता, लंच बॉक्स, घर से जल्दी-जल्दी निकलना, आठ 32 की कल्याणी फास्ट। फिर ऑफिस में काम की मारा-मारी। इतवार की दुनिया की देह नायक को एकमुश्त लगती है। इस दिन को लेकर उसकी अपनी एक फंतासी है।
कुणाल ने इन दोनों दुनियाओं का शानदार चित्रण किया है। उन्होंने टाइपिंग को जीवन से जोड़कर बढ़िया ढंग से इस्तेमाल किया है। कहानी में यह भी है कि यदि इतवार की छुट्टी ख़त्म कर दी जाए तो व्यक्ति का जीवन कैसे बदल जाता है। जीवन और फंतासी का बेहतरीन ‘सिंक्रोनाइजेशन’ है इस कहानी में।
संग्रह की एक अन्य महत्वपूर्ण कहा है ‘उपसंहार’। कहानी कोलकाता में रहने वाले चंडीप्रसाद रक्षित के मकान से शुरू होती हैं। रक्षित का भरा-पूरा परिवार है। नव्येन्दु और उसकी ख़ूबसूरत पत्नी झुम्पा है। इनके यहाँ नौ साल का लड़का मीठू है। नव्येन्दु से छोटी एक बहन है जो आठवीं में पढ़ती है, जिसे सब टुसी कहते हैं। घर में और भी सदस्य हैं। लेकिन कहानी उस घटना में कहीं छिपी है, जब नव्येन्दु अपनी पत्नी के साथ मार्केट की एक दुकान पर खरीददारी करने जाता है। भीड़ में एक छोकरा ना केवल झुम्पा से ग़लत तरीके से टकरा जाता है, बल्कि उसके गालों का चुम्बन भी ले लेता है। इसका प्रभाव बहुत विस्फोटक होता है।
झुम्पा नव्येन्दु को नामर्द कह देती है और टुसी को फिजीकली ‘झिंझोड़’ देती है। बाजार में मिला छोकरा मन की बहुत सी गांठों को खोल देता है। झुम्पा का नव्येन्दु को नामर्द कहना, टुसी के साथ फिजीकल होना क्या उसके मन की गांठों को खोल देता है? क्या वह पहले से यही नहीं कहना चाहती थी कि नव्येन्दु नामर्द है, क्या उसके मन में अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए किसी अन्य लड़की के पास जाने का विचार था? कुणाल अपनी इस कहानी में मन की अनेक कन्दराओं तक जाते हैं।
कुणाल की कहानियों में बेरोजगारी है, बियर है, यायावरी है, स्त्री है (स्त्रियाँ), प्रेम है, प्रेम की तलाश है, स्त्री देह है, उसकी चाह है, फंतासी है, जैक लण्डन है, बंगाली साहित्य है (शोकगीत)। प्रेम के समय कुणाल किसी वर्जना में यकीन नहीं रखते बल्कि वह वर्जनाओं को तोड़ने का काम करते हैं। उनकी एक कहानी है ‘साइकिल कहानी’। इसमें युवा हो रहे नायक का अपनी चाची (जो एक विधवा या परित्यक्ता है) के प्रति लगाव हो जाता है। उनकी यह कहानी ब्रिटेन की ब्रिजेट एटकिंसन की कहानी ‘औरत और साइकिल’ की याद दिलाती है।
इस कहानी में साइकिल को स्त्री स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का प्रतीक दिखाया गया है। जबकि कुणाल की कहानी में साइकिल संभवतः लड़कों को खुलेपन की ओर ले जाती है। यह कहानी उन प्रतिबंधों को तोड़ती है, जो परिवारों में लड़कों के साथ अनचाहे लग जाते हैं, जब युवा हो रहे लड़के स्त्री देह के प्रति खिंचते हैं। तब वह साइकिल को ही ‘जानेमन’ कहने लगते हैं।
इस संग्रह की एक अन्य कहानी है-दंगे में बारिश। यह पूरे संग्रह की मिज़ाज से अलग लेकिन महत्वपूर्ण कहानी है। ढाई पेज की इस कहानी में कुणाल ने आख्यान शैली को छोड़कर कहानी को अलग ढंग से ‘ट्रीट’ किया है। यह उस दिन को चित्रित करती है, जब बारिश और दंगे एक साथ आ जाते हैं। दोनों की आमद एक साथ हो, ऐसा पहली बार हुआ। दोनों से आम लोगों को सुरक्षा की दरकार है। दंगा परेशान है कि बारिश रुके तो वह अपना काम करे और बारिश सोच रही है कि दंगा रुके तो जीवन आगे बढ़े। अंततः आम लोगों को सुरक्षा चाहिए-दंगों से भी बारिश से भी। कहानी आम लोगों की इस असुरक्षा को बेहतर ढंग से चित्रित करती है।
‘अन्य कहानियाँ तथा झूठ’ पढ़ने के बाद यह साफ़ तौर पर लगा कि कुणाल के पास स्मृतियाँ हैं, किस्से हैं, सपने हैं, फंतासियाँ हैं और इन सबको वह कहानी की शक्ल देना जानते हैं-बेशक आख्यान के रूप में ही। इन कहानियों की एक और ख़ास बात की इनमें जबरदस्त पठनीयता है। कुणाल अपनी कहानियों में स्वप्न और स्मृतियों के बीच की दूरी ख़त्म करते दिखाई देते हैं।
यही वजह है कि वह कहानियों के किरदारों और वास्तविक जीवन के किरदारों में कोई भेद नहीं करते। यह तक कि विदेशी उपन्यास और लेखक भी इन कहानियों में बरबस चले आते हैं। इन कहानियों को पढ़ना यह देखना और समझना भी है कि ‘फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस’ की कहानियाँ कैसी होती हैं।
किताबः अन्य कहानियाँ तथा झूठ
लेखकः कुणाल सिंह
प्रकाशकः लोकभारती प्रकाशन
मूल्यः 299 रुपये
पृष्ठः 214