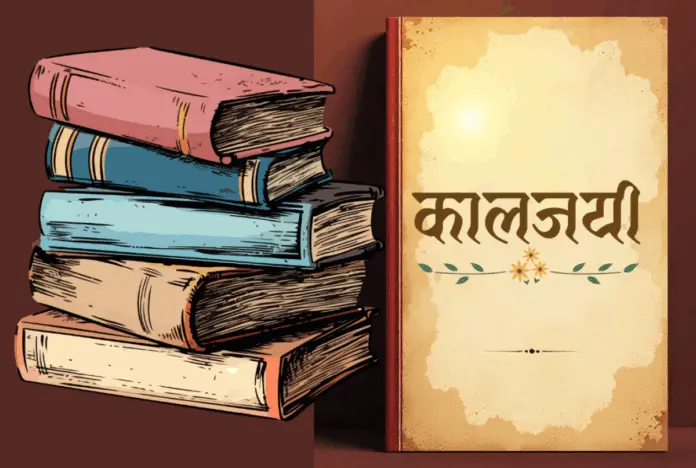बेशक यथार्थवादी साहित्य को ‘तिलिस्म होने से बचना चाहिए। परन्तु अगरचे सामने तिलिस्म आकर खड़ा ही हो जाये, तो क्या कीजियेगा? भेदना तो पड़ेगा ही।
कम-अज़-कम हिन्दी साहित्य की आधुनिक जन्मकुंडली तो इसी काल-सर्प की फांस में बंधी दिखाई देती है। हिंदी उपन्यास के उद्भव-काल में देवकीनंदन खत्री की ‘चंद्रकांता’ जैसी कृतियों को इस निगाह से देखेंगे, तो कह सकेंगे कि वे हिंदी नवजागरण की एक लहर भी हैं। उस दौर के ‘तिलिस्म’ को भेदना जैसे हमारी ऐतिहासिक नियति थी, जिसे इन उपन्यासों ने अपना दायित्व मानकर निभाया।
बेशक बात जब तिविस्म की होती है, तो कह सकते हैं कि वह नज़रों का धोखा है। पर उसके पीछे छिपी ठोस ज़मीन को खोजते ही पता चलने लगता है कि पर्दे के पीछे इतिहास के कितने बड़े षडयंत्र सरगर्म हैं। इस संदर्भ में प्रदीप सक्सेना की यह बात गौर-तलब लगती है कि ‘चन्द्रकान्ता’, ‘सन्तति’ और ‘भूतनाथ’ गहरी यथार्थवादी ज़मीन वाले उपन्यास हैं। इतना ही नहीं, उनकी ”गहन संरचनाएं’ रूपान्तरणात्मक’ हैं। इससे वे ‘साम्राज्यवाद विरोधी चेतना’ वाले ‘कालजयी, क्लासिक और महाकाव्यात्मक उपन्यास’ माने जा सकते हैं।
इस तरह की ये जो स्थापनाएं हैं, हमारे सामने अनेक सवाल खड़े करती हैं। हम यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि इन उपन्यासों की यह संभावनापूर्ण ज़मीन और रूपांतरकारी चेतना, अपने परवर्ती साहित्य में, इस रूप में क्यों दिखाई नहीं देती?
सवाल यह भी उठता है कि अगर वह संभावना बाद में बिखर और भटक गयी, तो उसके क्या कारण हैं? और इसके लिए यह तिलिस्मी साहित्य बज़ाते-खुद, कहाँ और कितना ज़िम्मेदार है?
फिर हमें यह पुनर्विचार भी करना पड़ेगा कि अगर देवकीनन्दन खत्री उस उत्स-काल में प्रकट हुए एक महान शिखर की तरह हैं, तो प्रेमचन्द की क्या जगह है? फिर ऐसा क्यों है कि प्रेमचंद उस ‘ज़मीन’ के ‘तिलिस्म’ को वहाँ पीछे अतीत में ही छोड़ कर, आगे निकल जाते हैं? उस साहित्य के बेहद जिज्ञासु पाठक होने के बावजूद?
इसके अलावा हम यहाँ इस सवाल से भी टकराते हैं कि क्या तिलिस्मी उपन्यासों के विवेचन-विश्लेषण के लिए नए साहित्यशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र के विकास की ज़रूरत है? अगर ऐसा है, तो यह काम अभी तक क्यों मुल्तवी पड़ा है?
ये सारे सवाल हमें एक अन्य बड़े और बुनियादी सवाल तक ले जाते हैं। वह यह है कि हमारे यहाँ आधुनिकता किस रूप में आती है? उसका साम्राज्यवाद विरोधी रूप, स्वयं आधुनिकता के अन्तर्विरोध के रूप में, क्या उसकी पुनर्व्याख्या की ज़रूरत तक नहीं ले जाता? तो, पहले इस आखिरी सवाल को ही उठाते हैं।
फ्रेडरिक जेम्सन उत्तर-आधुनिकता को ‘काल’ या ‘इतिहास’ जैसी सामान्य धारणाओं की बजाय, ‘देश’ की ज़मीन में ‘स्थित’ (सिचुएटिड) ‘समसमय’ की घटना के रूप में देखते हैं। उनकी यह समझ, पीटर ऑस्वर्न की आधुनिकता की व्याख्या के नज़दीक लाती है। वे उसे ‘भूगोल-राजनीति’ (जियो-पोलिटिक्स) की तरह ‘देखते हैं। इससे आधुनिकता, दुनिया के ‘स्पेस’ में फैलती औपनिवेशिकता के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है।
ये व्याख्याएँ अल्यूसे के इस मत को साबित और स्थापित कर देती हैं कि आधुनिकता परम्परागत उत्पादन-विधियों के विनाश के रूप में जनपक्षीय-‘इतिहास’ को विनष्ट करती हुई फैलती है। इस तरह वह ‘प्रगति’ को एकरेखीय बनाती है। इसमें हम सीन होमर (1999) की इस धारणा को भी शामिल कर सकते हैं कि ‘आधुनिकता एक मात्रात्मक धारणा नहीं, गुणात्मक घटना है’।
पर हम अपने यथार्थ के मद्दे-नज़र सीन होमर की इस धारणा को आंशिक रूप में ही स्वीकार कर सकते हैं। आधुनिकता का साम्राज्यवादी विस्तार, अगर एक ‘जियो-पोलिटिकल’ घटना है, तो वह मात्रात्मक विस्तार जैसी अधिक लगती है। पर उसके आधार पर जब पराजित राष्ट्रों की परंपरागत उत्पादन पद्धतियों को नष्ट किया जाता है और दावा किया जाता है कि इससे उनका पिछड़ापन दूर होगा, तो वह बात ऊपर से देखने पर गुणात्मक विकास की छलांग जैसी लग सकती है। जबकि दर-हकीकत वह प्रगति का तिलिस्म रचती है। फिर उसकी आड़। में उपनिवेशों का खुलकर दोहन-शोषण करती है।
आधुनिकता की इन व्याख्याओं के आलोक में अब हम ‘चंद्रकांता’ की ओर आ सकते हैं।
प्रदीप सक्सेना, 2004 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ‘तिलिस्मी साहित्य का साम्राज्यवादविरोधी चरित्र’ में एक ज़रूरी ऐतिहासिक तथ्य पर प्रकाश डालते हैं। उनका मत है कि ‘चन्द्रकान्ता’ के लेखन-काल तक चुनार एक जीवित यथार्थ था, न कि कोई परित्यक्त खंडहर। उसका इतिहास लिखते हुए ड्रेक ने दूसरी चीजों के उल्लेख के अलावा वहां दुर्गाकुंड, झिरना नाला, गुफाओं, नदी, कुंओं के साथ चट्टानों पर सिंहों, घोड़ों और हाथियों के उत्कीर्णनों का जिक्र किया है। इनकी विशालता और भव्यता रोमांच पैदा करती है। मुगल-काल से पहले का इतिहास अर्ध-पौराणिक है। किले की पंजे की तरह की आकृति, ऐड़ी की तरह का पृष्ठ भाग, पिंडली और तिल्लियों से सादृश्य, उसकी विष्णु के रूप में कल्पना, भर्तृहरि की समाधि, भैरों का बुर्ज, दुर्गा की गुफा, विक्रमादित्य का आसन, तीर्थ की मान्यता – ये सब चुनार के ‘चरणाद्रिगढ़’ के पौराणिक विवेचनों में निहित हैं। ‘चन्द्रकान्ता’ के वर्णनों में जो चुनारगढ़ के तिलिस्मी भवन हैं, प्रकृति, मार्ग और जीवन के चित्र हैं, वे सब इन पौराणिक उल्लेखोंसे, बहुत दूर तक सादृश्य रखते हैं।
इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि जब तक हम ‘चंद्रकांता’ जैसे उपन्यासों के महत्व को ठीक से समझ नहीं पाते, उसके आगे के भारतेन्दु काल और नवजागरण-काल की समझ सन्देह के घेरे में रहेगी।
हिंदी आलोचना में इस तरह के दावे अक्सर देखने को मिलते हैं। पर ये दावे तभी अर्थपूर्ण हो सकते हैं, जब हम यह बता पाएं कि रचनात्मक कृतियों में वस्तु और रूप के द्वन्द्वात्मक रिश्ते क्या हैं? कि ‘वस्तु’ और ‘रूप से हम क्या समझते हैं? जहां तक इस अध्ययन का संबंध है, यहां ‘वस्तु’ के मायने हैं- यथार्थ की अभिव्यक्ति’। इस आधार पर इन उपन्यासों को हिंदी में ‘यथार्थवाद का प्रथम उत्थान’ मान लिया गया है।
दूसरी ओर॔ यहा ‘रूप’ के मायने हैं – ‘आख्यान में ढल गया तिलिस्मी स्थापत्य’।
यानी इन उपन्यासों में यथार्थ की अभिव्यक्ति ‘इतिहास चेतना’ के रूप में नहीं, ‘समय के स्थापत्य’ के रूप में हुई है।
इसमें कोई शक नहीं कि यह स्थापत्य बहुस्तरीय है और इसीलिए वह अपने भीतर इतिहास और समय की अनेक पर्तों को अश्मीभूत रूप में समाये रहता है। यह एक नई प्रविधि है, जिसके तहत, गोया हम शहर के बीचों-बीच खड़े रह गए किसी खंडहर को पढ़ते और उसमें गहरे उतरते हुए अपने समय को, अपने विकास और प्रगति को, उसके सन्दर्भ में व्याख्यायित होता पाते हों और उस खंडहर को अब अपने रहने लायक भी नहीं समझते हैं।
‘चन्द्रकान्ता’ और ‘सन्तति’ ऐसे ही ‘आधुनिक’ कालीन खंडहरों’ की तरह हैं। आधुनिक, लेकिन अतीत को दर्शनीय बनाने वाले किसी ‘बाहरी समय के टुकड़े’। एक अर्थ में वहां हमारे ‘स्रोत’ हैं। या ऐसे पुल हैं, जिनकी मदद से हम वहां लौट सकते हैं। लेकिन वे उपेक्षित पड़े रहने की नियति का शिकार हैं और हमारे भय व कौतूहल के आधार भी हैं।
तो, इन उपन्यासों की बाबत वस्तु और रूप की यह जो समझ है, वह भी क्या उतनी ही यथार्थवादी’ है, जितनी कि इसकी बाबत किये गये दावे के तहत दिखाई देती है? यह सवाल इसलिये विचारणीय है, क्योंकि यह हमसे उपन्यासों के लिए एक नए साहित्यशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र की माँग करता है।
यह माँग इसलिए उठती है, क्योंकि ‘वस्तु’ का जो रूप-स्थापत्य होता है, शह उस वस्तु के पार चला जाता है। स्थापत्य, उससे पूर्व भी, अपनी तरह के एक अलग सभ्यता-मूलक यथार्थ की तरह, अपनी परंपरा के साथ, मौजूद देखा जाता है। कोई ‘वस्तु’ (कंटेंट ) जब एक ‘स्थापत्य’ में बदलती है, तो वह उसे एक ‘अलग वस्तु’ बना देती है। फिर बाद में जब हम उसके खंडहरों को देखते हैं, तो वह उस वस्तु-मात्र के खंडहर नहीं होते। उन खंडहरों के साथ, प्रकृति और भूगोल से उनके रिश्ते भी खंडहर हो जाते हैं। तब उसका पाठ, किसी सभ्यता के उत्थान-पतन के इतिहास की तरह मुमकिन हो जाता है। तब स्थापत्य, सभ्यता के ठोस, पर कलात्मक निर्माणों का आख्यान बनकर मुखर हो जाता है। वह अपने भीतर निवास करने वालों की अनकही दास्तानों का पुलिंदा हो जाता है।
किसी उपन्यास के रूप-विधान को जब हम उसके स्थापत्य की तरह पढ़ते हैं, तो हमारे उस पाठ को कायदे से ‘सभ्यता का पाठ’ होना चाहिये। पर हिंदी आलोचना में अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता। स्थापत्य की चर्चा, एक उल्लेख या सूचना भर होकर रह जाती है। फिर उसे भुला दिया जाता है। उसके बाद कृति की समाज-राजनीतिक या सांस्कृतिक ‘अंतर्वस्तु’ तक पहुंच कर, वह चर्चा निपट जाती है। जैसे ‘चंद्रकांता’ के साथ हुआ है। ‘चरणाद्रिगढ़’ सं संबंधित पौराणिक विवरण, विवरण भर होकर रह जाते हैं। फिर उन्हें भुला दिया जाता है। निष्कर्ष के तौर पर हमें वहां मौजूद ‘साम्राज्यवाद विरोधी चेतना’ ही मिलती है। वह अधिक से अधिक उसका राजनीतिक ‘कंटेंट’ है। पर आप उस सबको अपने समय की राजनीति में तब्दील करके, उसका ‘कंटेंट’ कैसे बना सकते हैं? जबकि यहां मौजूद वास्तविक और आख्यान-गत स्थापत्य, एक अलग तरह का ‘यथार्थ’ है। इसे हम केवल ‘समय’ या ‘इतिहास’ के अक्ष पर ही नहीं नाप सकते। यह ‘वस्तु-स्थापत्य’ निरी समाजेतिहासिक चेतना का पर्याय नहीं है।
इसलिए, कृति-गत स्थापत्य, विकास और प्रगति के तयशुदा सिद्धान्तों द्वारा व्याख्यायित नहीं हो सकता। वह किसी अन्य तरह के यथार्थ की मौजूदगी की ओर इशारा करता है।
यहाँ समय या इतिहास, ठोस या स्थानीय हो जाता है। इसलिये इसके रहस्य को खोजने के लिए हमें ‘ऐयारी’ या ‘जासूसी’ करनी पड़ती है। या एक मानवशास्त्री अथवा भूगर्भ-विज्ञानी की तरह का उत्खनन करना पड़ता है।
स्पष्ट है कि ‘चंद्रकांता’ के सम्यक विवेचन-विश्लेषण के लिये एक भूगोलशास्त्री और मानवशास्त्री इतिहासकार हो जाने से आप खुद को बचा नहीं सकते। इससे इस तिलिस्मी साहित्य का ‘यथार्थवाद का प्रथम उन्मेष’ होना और उसमें ‘साम्राज्यवादविरोधी चरित्र का केन्द्रीय होना – एकमात्र ‘इतिहास’-सम्मत निष्कर्ष नहीं है।
यहां हमारे विवेचन का सम्यक आधार यह होता चाहिये कि तिलिस्मी साहित्य की इतिहास वस्तु, एक तरह की ‘स्थापत्य वस्तु’ में कैसे बदल जाती है। तब हम देख पाएंगे कि इस उपन्यास का यथार्थ, किस अर्थ में ‘जमीनी’ और ‘देशज’ है। किस रूप में वह, ‘समय’ के विविध कालखंडों की, ‘समकालीन एक-देशीयता’ का यथार्थ है।
स्थापत्य, किसी भी सभ्यता के सर्वाधिक ठोस निर्माणों में से एक होता है। किसी उपन्यास की सभ्यतामूलक ज़मीन की प्रकृति को जानने-समझने के लिये स्थापत्य एक कुंजी का काम कर सकता है। यह एक साथ बहुत से समयों और इतिहासों को जीने लायक बनाता है। इसलिए खंडहर, ‘इतिहास’ के विलोपन की प्रक्रिया के आरम्भ होने का पर्याय हो जाते हैं। यहाँ इतिहास के विलोपन का अर्थ, इतिहास का अन्त नहीं, अपितु उसके जर्जर होने पर, उसकी बहु-स्तरीयता का उघड़ आना है। वह इतिहास के निश्चित, मानकीकृत और वर्चस्वी रूपों का ‘विलोपन’ है। परन्तु साथ ही इतिहास की नीचे दबी-ढकी विविध परतों का पुनः प्रकट होना भी है।
इस जटिल स्थिति को समझने के लिए ‘चंद्रकांता’ के दौर के हालात की व्याख्या ज़रूरी है। तब अंग्रेजी साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के रूप में, हम अपने सामने इतिहास की एक बर्चस्वी धारा को देखते हैं। परन्तु ‘पूँजीवाद की विजय’ के पर्याय के रूप में यह इतिहास, यूरोप में अपने जिस रूप में उपस्थित है, उसका ठीक वही रूप ‘उपनिवेशितों के इतिहास का पर्याय’ नहीं होता।
यह ‘ठीक वही’ न होने वाला जो इतिहास है, दरअसल उस वर्चस्वी इतिहास से एकदम उलट या विरोधी इतिहास की तरह का है। वर्चस्वी इतिहास प्रजातन्त्र की ओर उन्मुख होता है, ‘उलट इतिहास’ प्रजातन्त्र के नाम पर सामन्तों से हाथ मिलाने वाली एक नई तरह की तानाशाही है। यानी उपनिवेशित इतिहास वर्चस्वी इतिहास की दोनों बुनियादी बातों से एकदम उलट है। वर्चस्वी इतिहास सामन्तवाद को उखाड़ते और ‘रिप्लेस’ करते हुए, तानाशाही के विकल्प को लाता है। जबकि उसी की कोख से निकला उपनिवेशवादी इतिहास, इन्हीं दोनों, इतिहास वाह्य घोषित कर दी गई चीज़ों, की मदद लेकर आगे बढ़ता है। इससे होता क्या है?
होता यह है कि हम अपने यहां इतिहास की ‘विकासधारा’ के विलोपन को घटित होता पाते हैं। वह हमारे यहाँ ‘सभ्यता के आरोपित विकास’ के सह-समांतर, किसी भूत की तरह दिखाई देता है और हमें डराने लगता है। इसलिये यह अकारण नहीं है कि खत्री भूतनाथ जैसे पात्रों से घिरे हुए दिखाई देते हैं। ‘चंद्रकांता’ में ‘जिंदा हो गये भूतहा खंडहर’ मौजूद हो जाते हैं। उनके भीतर, दफन हालात में भी, अनेक रहस्य साँसें लेते मिलते हैं।
यहां आरोपित विकास और खंडहरों के जीवित हो उठने के बीच का साजिशी संबंध, हमें डराता है। इसके बावजूद, इतिहास के इन दोनों रूपों के भीतर से, उनके अपने प्रतिरोधी पक्ष भी उभरते हैं। वे एक नए इतिहास को भी जन्म देते दिखाई देते हैं।
यह तीसरा इतिहास ही, हमारा वास्तविक इतिहास है। वह इन खंडहरों की तरह स्थानीकृत और जड़ीभूत होने से इनकार करता है। परन्तु उसे स्वीकृति नहीं मिलती। उसे इतिहास का दर्जा भी नहीं दिया जाता। उसे अधिक से अधिक स्थानीय राष्ट्रवादी लहरों की तरह प्रस्तुत किया जाता है। या गदर या विद्रोह का नाम दिया जाता है। यह उत्तर-औपनिवेशिक इतिहास है, जो औपनिवेशिक इतिहास के सह और समांतर, उसके मौजूद होते ही, तत्काल उसके प्रतिपक्ष की तरह मौजूद हो जाता है। लेकिन वह जो औपनिवेशिक इतिहास है, वह अपना दबदबा बनाये रखता है। वह अपने ही विरोध में खड़े सकारात्मक पूँजीवाद और वैज्ञानिक-जनतान्त्रिक चेतना के बीजों को छिपाता रहता है। अपने इस अन्तर्विरोध पर लज्जित भी नहीं होता। अपितु ढिठाई के साथ आगे बढ़ता रहता है।
वर्चस्वी इतिहास, उपनिवेशितों की तरह हमारा देशीकरण करता है। वह स्वदेशी के उलट, नागर आधुनिकता के देशज रूप की तरह, हमारे यहां पांव पसारता है। वह मूलतः नगर-सीमित शिक्षित मध्यवर्ग-केन्द्रित रूप में सामने आता है। वह हमारी ‘चेतना के निर्माण’ से ज्यादा, उधार के तौर-तरीकों, भाषा व्यवहारों, वेशभूषाओं, फैशनों आदि में ही अधिक दिलचस्पी दिखाता है। वर्चस्वी इतिहास की यह खासियत उसके दोनों रूपों, यानी यूरोपीय पूँजीवादी और रूसी समाजवादी में, यकसां दिखाई देती है। दोनों हमारे साथ उपनिवेशितों जैसा व्यवहार करते हैं। वे हमारे यहाँ आयातित रूप में आते हैं और हमें मज़बूती देने की बजाये, अपने वर्चस्व को स्थापित करने में अधिक सक्रिय नज़र आते हैं।
तो, यह जो उपनिवेशित इतिहास है, वह हमारी ‘चेतना’ की तरह नहीं, हमारे इतिहास के खंडहरों में स्थानीभूत हुआ रहता है। और ‘चंद्रकांता’ जैसे उपन्यासों की अंतर्कथा हो जाता है।
ठिर उत्तरऔपनिवेशिक प्रतिरोधी चेतना, हमारे यहां एक वैकल्पिक इतिहास की रचना आरम्भ करती है। पर उसे इतिहास भी नहीं समझा जाता। तीसरी दुनियां में इतिहास के इस विलोपन को समझने के लिये इस तरह के उपन्यास हमारे लिये बहुत अर्थपूर्ण हो सकते हैं।
पर इस तरह के उपन्यासो में वह जो औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक इतिहास की सह और समांतर मौजूदगी है, उस पर सजग रूप में विचार कम ही किया जाता है। तथापि राजेन्द्र यादव की स्थापनाओं में, इस संदर्भ में एक ‘भिन्न या उत्तर प्रस्थान’ दिखाई देता है।
राजेन्द्र यादव ‘चन्द्रकान्ता’ और ‘सन्तति’ को ‘नवजागरणकाल में एक अँगड़ाई लेकर जागते हुए भारतीय समाज की दयनीय महानता की दास्तान’ मानते हैं।
‘महानता’ का ताल्लुक सामन्ती इतिहास से है, जिसके ‘महान’ होने पर सन्देह होता है। गदर में सामन्ती इतिहास की अन्तिम पराजय के बाद उसमें मौजूद महानता के अवशेषों पर यह सन्देह, औपनिवेशिक वर्चस्वी इतिहास की रणनीति का एक हथियार भी था। सामंतवाद की सियासी पराजय के बाद अब उसे सांस्कृतिक मोर्चे पर भी शिकस्त देने की कोशिश हो रही थी। तो राजेन्द्र यादव की यह जो टिप्पणि है, वह एक तल पर औपनिवेशिक मानसिकता की अनुगूँज लिये हुए हमारे सामने आती है। वह औपनिवेशिक इतिहास की आत्म-विरोधी धूर्तता को छिपाती है। अगर सामन्तीय महानता का तत्कालीन रूप, उसकी ‘दयनीयत्ता’ है, तो अंग्रेज़ अपने इतिहास का झंडा फहराने के लिए उसी की सहायता क्यों लेते हैं? उसी के साथ ज़मीनी धरातल पर दूर तक समझौता क्यों करते हैं?
इस तरह की टिप्पणियां इसे अंग्रेज़ों की रणनीति मानकर टालने का काम ही अधिक करती हैं। परन्तु इससे रजवाड़ों, किलों, ऐयारों और न जाने किन-किन के इतिहास के खंडहरों की अंतर्कथा भी गौण और ‘दयनीय’ होकर रह जाती है।
राजेन्द्र यादव इस ज़मीनी हकीकत को ”मनोवैज्ञानिक संरचना’ बनाकर, ‘एक प्रतीक’ मात्र बना डालते हैं।
“अकसर ही उपन्यास पढ़ते हुए मुझे लगता रहा है कि ये टेढ़े-मेढ़े रास्ते, चट्टानें, धने जंगल, नाले, झाड़ियाँ, गुफाएँ, खोह, मुहाने, सुरंगें और ऊँची- नीची खौफनाक पहाड़ियाँ, अपने चेहरे छिपाये किसी न किसी घात में लगे ऐयार – ये सभी वास्तव में कहीं बाहर नहीं हैं। वे जैसे भारतीय मानस के भीतर ही कहीं उग आए हैं। ये सब उस मनोवैज्ञानिक दुनिया का हिस्सा हैं, जो तुड़-मुड़कर विकृत और कुंठित हो गई है। मुझे लगता रहा है कि ये पहाड़ और घाटियाँ उसी मनो-जगत में उग आए थे, जहाँ अनपहचानी नकाबपोश वृत्तियाँ सन्देहास्पद ढंग से घूमा करती हैं।”
इस पर प्रदीप सक्सेना की टिप्पणी है,
“यह जो मनोविज्ञान, फैटेसी या आद्यविम्बात्मक सामग्री है, यह उतनी ही यथार्थ है, जितनी दिल्ली या बिहार।”
इस उद्धरण से दो बातें साफ हो जाती हैं एक यह कि देवकीनंदन खत्री के उपन्यासों के बहाने से नवजागरण को समझने-खोजने के लिए हमारे पास कम-अज-कम दो बुनियादी दृष्टिकोण मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि यही दृष्टिकोण, हिन्दी साहित्य के आधुनिक दौर के ‘नएपन’ की व्याख्या के लिए, दो तरह के साहित्यशास्त्रों और सौन्दर्यशास्त्रों के अन्तर्विकास की जरूरत पर बल दे रहे हैं।
यह पूरी व्याख्या-पुनर्व्याख्या, गोकि अपने विकास के आरम्भिक दौर में ही दिखाई देती है, परन्तु इसलिए अहम और विचारणीय है, क्योंकि वह हिन्दी में पहली दफा हिन्दी के ‘अपने’ साहित्यशास्त्र के विकास की दिशा में कुछ कदम आगे रखती है। इस तरह वह हमें रूपवाद-मार्क्सवाद या आधुनिकतावाद-प्रगतिवाद जैसे आयातित ध्रुवायित आधारों और सिद्धान्तबद्धताओं से भी उबारती है।
पर आधुनिकतावाद-प्रगतिवाद में विभाजित ये बहसें हमारे यहाँ वर्चस्वी इतिहासधाराओं के आरोपण से जुड़ी चीज़ें हैं। वे दोनों ही साम्राज्यवादी साहित्यशास्त्र का हिस्सा हैं।
दूसरी ओर हमारे पास या कहें तीसरी दुनिया के पास, जो विकल्प बचता है, उसका अन्तर्तनाव अलग है। वह इस ‘उपनिवेशितों के सभ्यता-मूलक साहित्यशास्त्र’ के रूपों में सामने आता है।
औपनिवेशिक साहित्य-शास्त्र, साहित्य को पढ़ने-समझने के लिए, आधुनिकीकरण की और देखता है। वह साम्राज्यवादी सभ्यता-विस्तार’ को चुनौति की तरह देखता है। अपने प्राच्यवादी सभ्यता विमर्श को, प्रासंगिक बता कर हमें परोसता है। उसी आधार पर वह हमारे साहित्य की व्याख्या करता है।
वह हमें दिखाता है, जैसे कि हमारा साहित्य अतीतोन्मुख ‘दयनीय महानता की अभिव्यक्ति करने वाला साहित्य हो। ऐसा करके वह हमें हमारे ही इतिहास के खिलाफ कर डालता है और हमें उससे मुक्ति पाने की राह पर डाल देता है। ऐसा करने के लिए वह विवेचित साहित्य के यथार्थ को किन्हीं प्रवृत्तियों के प्रतीकों की तरह देखने की ओर ले जाता है। इससे हमारा अभिव्यक्त यथार्थ मनोकल्पित रूपों या आद्यविम्बों में रूपान्तरित होने लगता है। विशिष्ट पात्रों से उद्घाटित हो सकने वाले यथार्थ को इस तरह संदेहास्पद बना दिया जाता है। उनकी जगह, ऐसे हालात में सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले ‘टाईप्स’ का खांचा-बद्ध यथार्थ, ज़्यादा अहम या उल्लेखनीय माना जाने लगता है।
औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक साहित्य चिंतन की प्रविधियां अलग अलग प्रतीत होती हैं, पर ऐसा न होकर वे गहरे में एक ही हैं। ये हमारे साहित्य को अपने वर्चस्वी इतिहास से संचालित करने की कोशिश करती हैं। हमारी कृतियों को, ‘पूर्व-पश्चिम में विभाजित सभ्यताओं’ के नज़रिये से, हीन या दयनीय बनाती हैं। हमारे पात्रों की ‘वर्गमूलक’ टाईप्स में बंधी व्याख्या करके, वहां मौजूद समरसता को बर्ग-विभाजित बरती हैं और अंततः संदेहास्पद बना देती हैं।
इस तरह का आयातित साहित्य-चिंतन, हमारे लिये ज़रूरी ‘उपनिवेशितों के साहित्यशास्त्र’ के अन्तर्विकास के रास्ते में रुकावट बना रहता हैं।
राजेन्द्र यादव के खत्री के विवेचन पर इस साहित्य-चिंतन की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। वे खत्री के महत्व को ‘अपने तरीके से’ रेखांकित करते हुए भी, अंततः उसे रद्द या खारिज ही करते हैं। ऐसा करने के लिये वे कभी उसे ‘दयनीय’ पाते हैं, तो कभी समझौतावादी’ बना डालते हैं। जैसाकि भूतनाथ की उनकी व्याख्या में हुआ है।
उधर प्रदीप सक्सेना, जिसे अपनी ‘देशभक्ति और नवजागरण मूलक दृष्टि’ कहते हैं, वह मूलतः उत्तर-औपनिवेशिक वस्तु है। उसका संबंध हमारे यहाँ के तत्कालीन औपनिवेशिक हालात पर, समसमय में पुरातात्विक दृष्टि से पुनर्विचार करने से है। औपनिवेशिक गुलामी की प्रतिक्रिया में पैदा हुई प्रतिरोधी चेतना के रूप को समझना, इसका उद्देश्य है। उनका मार्क्सवाद उन्हें यहीं तक ले जा पाता है। इसलिये वे उस दौर में साम्राज्यवादी पूंजी के पाव पसारने से पैदा हुए अंतर्विरोधों को तो पहचान पाते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते। वे यह नहीं देख पाते कि इस तरह का मार्क्सवाद भी अंततः एक आयातित आलोचना पद्धति ही है। उसका ठीक से अतिक्रमण या अंतर्विकास न कर पाना भी, एक तरह की औपनिवेशिक मानसिकता ही है।
पर इस औपनिवेशिक मानसि से उबरना संभव है। वे जहां तक पहुंचे हैं, वहां से आगे बढ़ने पर एक रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। इये इसके लिये एक छोटी सी शुरुआती कोशिश करते हैं।
चुनारगढ़ के पौराणिक संदर्भों की मार्फत हम भारत के ज़मीनी सभ्यता-मूलक यथार्थ को एक विकल्प की तरह, चाहें तो खोज सकते हैं। बात उस गढ़ की आकृति के विष्णु की काया से सादृश्य रखने भर की नहीं है। वह भारतीय सभ्यता का उदात्त या संभ्रांत पक्ष है। हमें इसके सह-समांतर, उसका जन-पक्ष भी अभिव्यक्त होता दिखाई देता है। ऐयार लोग, जब वन में किसी गुफा या झोंपड़ी में नज़र आते हैं, तो अपनी एक अलग जीवन-शैली वाले लोग मालूम पड़ते हैं। ऊपर वीतराग, भीतर से सजग और चाक चौबंद। वे अपनी चेतना में उस आचरण में मुब्तिला दिखाई देते हैं, जो भारतीय सभ्यता की विरासत की तरह उन्हें मिली है। उनकी ये गुफाएं और झोंपड़ियों, गढ़ों के महान सामंतीय स्थापत्य का जन-धर्मी विकल्प हैं।
इस तरह के विवेचन को हम भारतीय उपन्यासों की सम्यक व्याख्या करने वाली’भारतीय सभ्यता मूलक आलोचना-पद्धति’ कह सकते हैं। इसका एक खास रूप खत्री के उपन्यासों की व्याख्या के लिये यहां अपनाया गया है। इसे हम इस आलोचना-पद्धति की ‘स्थापत्यवादी संरचना’ कह सकते हैं।
हिंदी आलोचना की एक सीमा है, जो हमारा रास्ते रोककर खड़ी रहती है। हम अपनी आलोचना पद्धतियों को अपनी कृतियों के भीतर से खोजने की बजाय, आयातित आलोचना-पद्धतियों के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। नतीजतन हमारे यहां आने वाला अस्तित्ववाद हमें अपनी महायानी ज़मीन का अंतर्विकास करने की ओर नहीं ले जाता। न ही मार्क्सवाद के आयातित रूपों से उबर कर हम किसी ‘अपने भारतीय मार्क्सवाद’ को ही खोज पाते हैं।
अब इधर पिछले कुछ दशकों में प्रवासी ‘डायस्पोरा’ के उभार के बाद, प्राच्यवाद ने ज़रूर औपनिवेशिक गुलामी की इस मानसिकता को बेनकाब करना आरंभ किया है। प्राच्यवाद हमारी उत्तर-औपनिवेशिकता की लम्बी इतिहासधारा के सीमान्त पर उभरा है। पर वह एक सीमित महत्त्व का दर्शन या वाद ही है।
खत्री के उपन्यासों की नई व्याख्या के संदर्भ में राजेन्द्र यादव और प्रदीप सक्सेना के बीच एक बुनियादी फर्क है। प्रदीप सक्सेना खत्री के उपन्यासों को ‘इतिहास सम्मत’ मानते हैं, जो उन्हें यथार्थवादी सिद्ध करने का मुख्य आधार है। इस कसौटी पर वे राजेन्द्र यादव के प्रतीकवाद के भरभराकर गिर जाने की बात को स्वयं-सिद्ध मान लेते है। जबकि ऐसा है नहीं।
वस्तुएँ, यथार्थ और प्रतीक दोनों एक साथ होती हैं। साहित्य की सृजनशीलता में ये दोनों पक्ष एक-दूसरे में गुँथे हुए रूप में विद्यमान रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि ‘चन्द्रकान्ता’ और ‘सन्तति’ के ज़रिये हम जिस साम्राज्यवाद प्रतिरोधी चेतना की पहचान तक चले आये हैं, उसे गहरा कर हम अभी तक एक नए साहित्यशास्त्र और सौन्दर्यशास्त्र के विकास की भूमिका नहीं बना पाये है। यह काम चुनारगढ़ की बाबत ज़मीनी स्तर के ‘वैज्ञानिक शोध अन्वेषण’ से पुष्ट तो होता है, परंतु वहीं तक सीमित नहीं है।
औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक साहित्यशास्त्र का बुनियादी फर्क इस पहचान में नहीं है कि हम भाषा के प्रतीक-निबद्ध इस्तेमाल से, यथार्थ आधारित इस्तेमाल की ओर उन्मुख होते हैं।
औपनिवेशिक साहित्यशास्त्र, सामाजिक आधार को अपना कर कृतियों की व्याख्या करता है। कथा के संदर्भ में वह अपना पूरा ध्यान उभरते हुए मध्यवर्ग पर केन्द्रित कर देता है। यह वर्ग स्वयं को समाज के एक नये प्रतिनिधि’ के रूप में स्थापित करता है। वह मध्यकालीन नायक (उच्चवर्गीय / सामन्तीय) को विस्थापित कर देता है। इस प्रक्रिया में शेष समाज को सीमान्तीय बना देता है। शेष समाज उसके सामाजिक पर्यावरण में बदल जाता है। तब उसकी मौजूदगी कृतियों में एक प्रतीक की तरह दिखाई देने लगती है। ऐसा करके मध्यवर्ग हाशिये के समाजों का प्रतिनिधि हो जाता है। देश और इतिहास के विविध स्थानीकृत रूप इसी बहुस्तरीय प्रतीकीकरण का आधार बनते हैं।
इसके बाद विकसित हुआ उत्तर-औपनिवेशिक साहित्यशास्त्र, सामाजिक यथार्थ की व्याख्या थोड़े अलग रूप में करता है। पर दोनों में कोई बड़ा बुनियादी फर्क नहीं है। वह पहले की तरह ‘मध्यवर्ग के उभार’ को केन्द्र में रखने के बावजूद, यह भी देखता है कि उसकी स्थिति संकट-ग्रस्त हो गयी है। पर उसका मुकाबला उच्चवर्गीय नायकों या बुर्जुआ के नव-उभार से नहीं है। अपितु वैश्विक बाज़ार की सूचना-तांत्रिक और उपभोक्तावादी, गिरफ्त से है। वह उसे द्विभाजित और विखंडित करती है। वह उसके सामाजिक और सांस्कृतिक वजूद तक को संकटग्रस्त बनाये रखती है। वह उसे निरन्तर निम्न और सीमान्तीय जन-समूहों की ओर भी धकेलती है। इस आपसदारी से हाशिये के समाजों की अस्मिताओं में जो उभार दिखाई देता है, वह उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं को बढाता है, पर समाज को और छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित भी करता है। इससे इतना ही पता चलता है कि हालात पहले के मुकाबले जटिल हो गये हैं। पर इससे मध्यवर्ग का मूल चरित्र बहुत नहीं बदलता। वह सत्ता से समझौता करके खुद को पहले की तरह बचाता रहता है। उसके बीच से निकला ‘कुशल श्रमिक’ ही ऐसा जन-समूह दिखाई देता है, जो हालात के दबाव से थोड़ी राहत पा सका है। यह मध्यवर्ग, बाज़ारवादी नव-साम्राज्यवाद की जकड़बंदी को तोड़ पाने लायक, अभी तक तो दिखाई नहीं देता।
परंतु इस तरह के उत्तर-औपनिवेशिक विमर्श को भूतनाथ में खोजने की बात बहुत तर्क-संगत नहीं लगती। उसकी व्यक्तिवादी पतनशीलता को मध्यवर्ग की उत्तर-औपनिवेशिक स्थिति का पूर्वाभास कराने वाला नहीं माना जा सकता। अधिक से अधिक हम उसे, यथार्थ के खंडहर मे भटकती, कोई समकालीन रूह ही कह सकते है। तथापि वह खत्री के कथा साहित्य की यथार्थवादी व्याख्या न होकर, उसके प्रतीकीकरण का प्रयास ही अधिक होगी। अगर ऐसा है, तो भी यह इस कथा साहित्य के, सीधे न सही, पर एक परछाई की तरह, मौजूदा समय पर डोलते रहने की बात तो है ही।