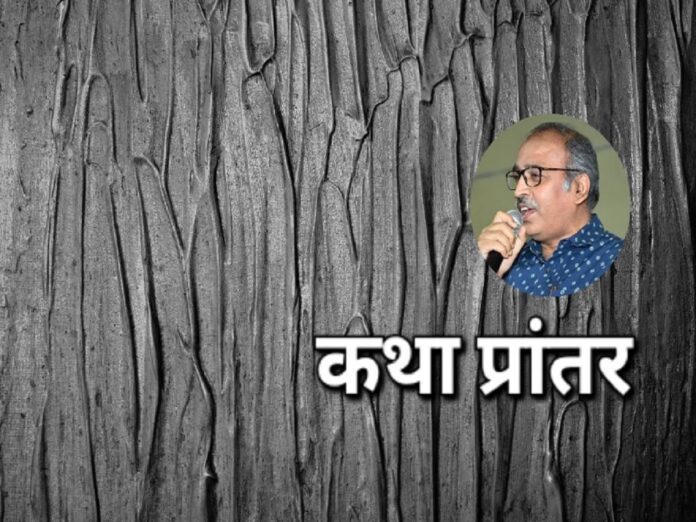“हमारे समय की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि ऊर्जा के भौतिक रूपों के रूपांतरण की लगभग असीमित तकनीकी क्षमता के बावजूद, हमने उन ऊर्जा-रूपांतरणों के नैतिक और पारिस्थितिक परिणामों की उपेक्षा की है। हमने पारिस्थितिक तंत्रों को असंतुलित कर दिया है, जिसमें मिट्टी, जल और वायु के साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रणालियाँ भी शामिल हैं। मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध- चाहे भौतिक हो या सांस्कृतिक, मूलतः पारिस्थितिक ही होता है। जब हम इस संतुलन को बिगाड़ते हैं, तो विनाश केवल बाह्य नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। अतः साहित्य और पारिस्थितिकी का मिलन केवल एक सैद्धांतिक या रूपकात्मक प्रयोग नहीं है बल्कि अस्तित्वगत अनिवार्यता है।”
प्रसिद्ध अमेरिकी आलोचक विलियम रुकेर्ट की ये पंक्तियाँ उनेक प्रसिद्ध निबंध Literature and Ecology: An Experiment in Ecocriticism से उद्धृत है, जो ‘आयोवा रिव्यू’ नामक पत्रिका में 1978 में प्रकाशित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि साहित्यिक कृतियों को पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पढे जाने की जरूरत को प्रस्तावित करते हुए उन्होंने पारिस्थितिक आलोचना (Ecocriticism) पद का प्रथमतः उपयोग इसी निबंध में किया था। उक्त निबंध में विलियम रुकेर्ट ने इस बात पर खासा जोर दिया है कि साहित्य और पारिस्थितिकी दोनों हमें यही सिखाते हैं कि जीवित प्रणालियाँ परस्पर पोषण पर आधारित होती हैं, न कि दोहन पर। इस पोषण की प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करना साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण दायित्व है ताकि ऊर्जा का रचनात्मक प्रवाह अवरुद्ध न हो तथा मनुष्य और संसार के बीच पुनः वह संवाद स्थापित हो सके जिसे आधुनिक औद्योगिक सभ्यता लगातार क्षतिग्रस्त करती आ रही है। आज जब पर्यावरण और पारिस्थितिकि का संकट मानव सभ्यता के अस्तित्व के समक्ष लगभग सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आ खड़ा हुआ है, विलियम रुकेर्ट के ये विचार दुनिया की हर भाषा के साहित्य और उसकी आलोचना के लिए लगभग अपरिहार्य हो चुके हैं।
इक्कीसवीं सदी की कहानियों से गुजरते हुए मेरी यह धारणा लगातार मजबूत हुई है कि हिन्दी कहानी में मानवेतर प्राणियों की उल्लेखनीय वापसी हुई है। कहानियों में मानवेतर प्राणियों की इस वापसी को मैं पर्यावरण और पारिस्थितिकि के संकट के विरुद्ध एक रचनात्मक प्रतिरोध की तरह देखता हूं। कथा साहित्य में पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रति इस संवेदनात्मक हस्तक्षेप को देखते हुए यह प्रश्न सहज ही सामने आ खड़ा होता है कि क्या समकालीन कथालोचना हरित कथा साहित्य की इन आहटों को ठीक-ठीक पहचान पा रही है? कुछेक छिटपुट आलेखों और समीक्षाओं को छोड़ दें तो यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि हिन्दी कहानी में हो रहे इन बदलावों की तरफ आलोचना का पर्याप्त ध्यान जाना अभी बाकी है।
अपने मूल अर्थ-स्वरूपों में साहित्य की हर विधा, ऊर्जा का संचरण ही है, वह ऊर्जा- जो भाषा, कल्पना, विचार और कौतूहल के संयुक्त माध्यम से मानव सभ्यता की क्षीण हुई जाती आत्मा को पुनर्जीवित करता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आलोचना, जो रचना के साथ संवाद करने के अपरिहार्य गुणसूत्रों के कारण अंततः और अनिवार्यतः रचना ही होती है, अपनी पारिस्थितिक भूमिका को पहचाने। इसके लिए उसे संपूर्णतः रचनाश्रित (परजीवी) होने की भूमिका का अतिक्रमण करना होगा। अन्यथा रचना से सिर्फ अर्थ निकालने या उसके सार-संक्षेपण का उपक्रम आलोचना को प्रथमतः रचना के विशिष्ट उपभोक्ता और अंततः उसके संहारकर्ता की भूमिका में परिसीमित कर देगा। किसी रचना के प्रति यही दायित्वबोध आलोचना को अर्थ निरूपण की सीमा से बाहर लाकर ‘फीडबैक मैकेनिज़्म’ के बृहत्तर वृत्त में दाखिल करवाता है। अर्थ निरूपण से अर्थ निर्माण की दिशा में उद्यत इस प्रक्रिया में रचनाकार और आलोचक समान रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं। कथादेश (अक्तूबर- 2023) में प्रकाशित नवीन कुमार नैथानी की कहानी ‘लैंडस्लाइड’ पारिस्थितिकि तंत्र के पोषण और दोहन की द्वन्द्वात्मकता के बीच सर्जक और आलोचक के दोहरे दायित्व की पारस्परिकता को गहरे रेखांकित करती है।
‘सारिका’ के दिनों से अपनी कथा यात्रा शुरू करनेवाले नवीन कुमार नैथानी ‘भरी गगरिया चुप्पे जाय’ की तर्ज पर खामोशी से रचनारत रहनेवाले कहानीकार हैं। गति और शोर के विरुद्ध ठहराव और मौन के सांद्र सौन्दर्य का अर्थगर्भी रचाव इनकी कहानियों के मूल में रहा है। अमूमन इनकी कहानियां पहाड़ी अंचल की लोक कथाओं के बहुआयामी विस्तार में अपने लिए खाद पानी का प्रबंध करती हैं। नवीन कुमार नैथानी की एक कहानी से दूसरे कहानी के बीच पहाड़ और उसके जीवन का नैरंतर्य जिस शृंखलाबद्ध तरीके से सांसें लेता है, वह एक कहानी में कई कहानियों या कई कहानियों में एक कहानी के होने के संरचनात्मक अनुभव विरल नमूना है। मिथक और आंचलिकता के उपकरण के बजाय यथार्थ को उसकी संवेदनात्मक कलात्मकता के साथ बरतने के हुनर के कारण, पहाड़ी जीवन पर केंद्रित होने के बावजूद ‘लैंडस्लाइड’ अनुभव और यथार्थ के नैरंतर्य को उनकी अबतक प्रकाशित कहानियों के ढांचे में ही आगे नहीं बढ़ाती। लेकिन अर्थ संधान या अर्थ निर्माण की दृष्टि से यह कहानी उनकी पूर्ववर्ती कहानियों की तरह ही संश्लिष्ट और बहुपरतीय है। ‘लैंडस्लाइड’ का पाठ्यानुभव इन अर्थों में अलभ्य और विलक्षण है कि इसकी संवेदनाओं को गहराई से महसूस करने के बावजूद इसकी व्याख्या करना आसान नहीं है। कहानी को महसूस करने और उसका अर्थ स्पष्ट करने की दो प्रक्रियाओं के बीच स्थित इस अंतराल का कारण ‘कहे’ और ‘अनकहे’ के बीच की वह सघन आवाजाही है, जिसमें इस कहानी का मर्म बसता है। इस कहानी को बार-बार पढ़ते हुए, मुझे नवीन कुमार नैथानी के उस वक्तव्य का एक अंश याद आता रहा, जो उन्होंने कोई दो वर्ष पूर्व (संभवतः 2023 में) ‘ओम प्रकाश मालवीय-भारती देवी स्मृति सम्मान’ ग्रहण करते हुए इलाहाबाद में दिया था- ‘मैं नहीं जानता, मैं अपनी कहानियों में ठीक-ठीक क्या कहना चाहता हूं, यदि जानता होता तो लेख लिखता, कहानियां नहीं।’ आत्मसंशय के धूसर में लिपटा यह वाक्य महज लेखकीय विनम्रता के तकाजे से उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कथा और कथाकार के बीच निरंतर घटित होनेवाले वाले उन अंतर्द्वंद्वों की भूमिका है, जो किसी रचना की संश्लिष्टता के लिए एक जरूरी अवयव है।
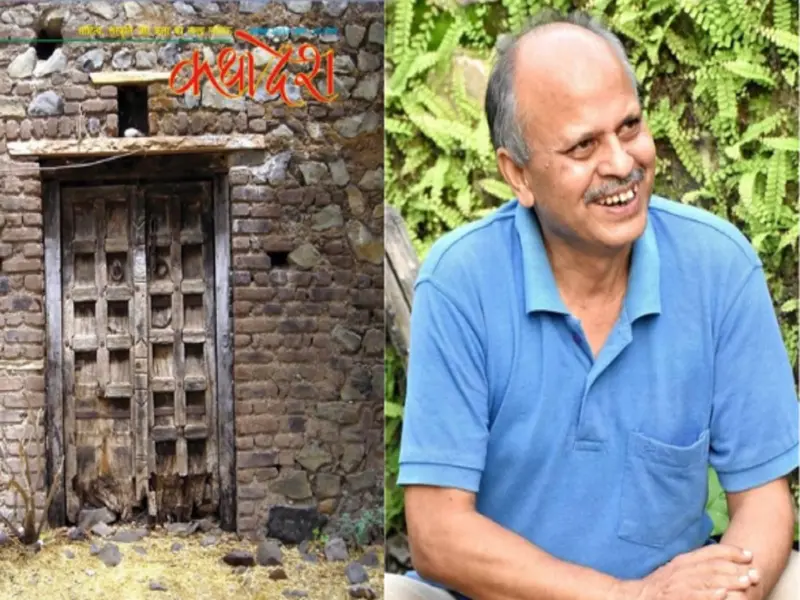
नवीन कुमार नैथानी
पिछले कुछ वर्षों में चर्चित और प्रशंसित कहानियों का एक बड़ा हिस्सा सूचना-संचार क्रांति की पृष्ठभूमि में विकसित हो रहे समय-समाज की सांस्कृतिक-राजनैतिक समीक्षा करता है। रचना और आलोचना की दृष्टि सामान्यतया उन कहानियों तक नहीं पहुँचती या कम पहुँचती है, जो यथार्थ को महज भौतिक गुणसूत्रों के दायरे में नहीं देखते हैं। भौतिकी विज्ञान के अध्येता और अध्यापक नवीन कुमार नैथानी हिन्दी कथा परंपरा में इसलिए विशिष्ट हैं कि भौतिक और पारभौतिक की द्वन्द्वात्मकता को रचनात्मकता के सूक्ष्मतम अनुभवों में तब्दील करते हुए वे वायवीय अमूर्तन का शिकार नहीं होते। अति यथार्थ के निरूपण को ही रसाई का मानक माने बगैर यथार्थ की डोर को थामे हुए रचना की कलात्मकता को साध पाना नैथानी के कहानीकार की दूसरी बड़ी विशेषता है। इसलिए अंधेरा, अकेलापन, चुप्पी, खूबसूरत लैंडस्केप, फैन्टेसी और जादूई यथार्थ के अभिलक्षणों से संपृक्त होने के बावजूद ‘लैंडस्लाइड’ को ठीक उसी तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जिस तरह हम निर्मल वर्मा या विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं को पढ़ने-समझने के अभ्यस्त रहे हैं। इस कहानी के प्रकाशन के बाद कतिपय अध्येताओं और आलोचकों द्वारा उन्हीं उपकरणों से इस कहानी को परखने का नतीजा रहा कि किसी ने ‘लैंडस्लाइड’ को प्रेम कहानी में परिसीमित कर दिया तो किसी ने इसे ‘स्थूल यथार्थ’ और ‘रूपवाद के गड्ढे’ के बीच तनी रस्सी पर निष्कंप चलने वाले निर्दोष शिल्प की कहानी के रूप में विवेचित किया। नतीजतन, जीवन और जगत तथा मनुष्य और पारिस्थितिकि के अंतःसंबंधों की जरूरत को यह कहानी संवेदना के जिस सूक्ष्मतम धरातल पर संबोधित करती है, उसकी चर्चा नहीं या लगभग न के बराबर ही हुई।
यह भी पढ़ें- कथा प्रांतर 3: द्रष्टा और भोक्ता के अनुभूति-अंतरालों के बावजूद
थोड़े से संवाद और ढेर सारी चुप्पी, हल्की सी रोशनी और नीम गाढ़ा अंधेरा, थोड़ी सी अधीरता और असीम धीरज, क्षणिक मुलाकात और अंतहीन प्रतीक्षा, अत्यल्प उद्घाटन और सुदीर्घ गोपन, महीन सी उम्मीद और विस्तृत उदासी के बीच अपना स्थापत्य ग्रहण करती ‘लैंडस्लाइड’ में वाचक ‘मैं’ और कथानायिका ऋचा के बीच जिस बाह्यांतरिक संवाद सेतु का विनिर्माण होता है, वह मनुष्य और पर्यावरण की पारस्परिकता का नतीजा है, जिसके मूल में पारिस्थितिकि के पोषण और दोहन की वही द्वन्द्वात्मकता निहित है, जिसका उल्लेख इस आलेख के शुरुआती हिस्से में किया गया है।
जिस तरह अर्थ स्पष्ट करनेवाली समीक्षा प्रविधि ‘लैंडस्लाइड’ के मर्म तक नहीं पहुँच सकती, उसी तरह सार-संक्षेपण वाली समीक्षा शैली इसकी आत्मा को विनष्ट कर सकती है। इस बात का संज्ञान लेते हुए, जिन लोगों ने यह कहानी नहीं पढ़ी है, उनकी सुविधा और कथानक की बाहरी काया को स्पष्ट करने के लिए यह बताना जरूरी है कि यह कहानी एक पहाड़ी कस्बे में स्थित वाचक के अंधेरे कमरे से शुरू होती है, कई दिनों की धारासार बारिश के कारण, जहाँ से बाहर नहीं निकल पाने को वह विवश है। मकान मालिक जयदत्त और जल विभाग के कर्मचारी दानू जी की उपस्थिति तथा अतीत और वर्तमान की आवाजाही के बीच पता चलता है कि कथावाचक, जो ऋचा से गहरे प्रेम करता है, उसके अनकहे इंतजार में है। इस क्रम में पाठकों को दो और बातें पता चलती हैं, जो लगभग रहस्य की तरह कहानी में आद्योपांत विद्यमान हैं और जिनके सहारे कहानी ने अपना स्वरूप मुकम्मल किया है- एक बात यह कि दानू जी ने वाचक को एक लिफाफा लाकर दिया है। कहानी के ब्योरे इस बात को पुष्ट करते हैं कि वह लिफाफा वाचक के लिये ऋचा ने ही भेजा था। दूसरी बात यह कि ऋचा मूलतः जेनेटिक्स की शोधार्थी थी और उसने अचानक ही ईकोलॉजी को अपना अध्ययन क्षेत्र बना लिया है और लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों की सेवा और देखभाल के लिये समर्पित हो गई है। ‘लिफ़ाफ़े में बंद खत में क्या लिखा है’ के कौतूहल के बीच वाचक के असीम धैर्य और उसे लगभग एक किरदार की तरह रचने का लेखकीय कौशल ही यहाँ उन कहे-अनकहे और व्याख्येय-अव्याख्येय उपादानों का संयोजन-प्रबंधन करता है, जिसने इस कथानक को ‘कहानी’ की काया प्रदान की है। इस बात को रेखांकित किया जाना चाहिए कि कहानी ‘खत में क्या लिखा है’ के कौतूहल में नहीं, बल्कि उस कौतूहल को जीवंत बनाए रखने की प्रक्रिया में उकेरी गई स्मृतियों से उत्पन्न द्वंद्वों की परछाइयों, बेचैनियों और एक अन्य लिफ़ाफ़े में बंद मजमून में उपस्थित है, जिसे कहानी के उत्तरार्ध में खुद ऋचा ने वाचक को उसी अंधेरे कमरे में घटित संक्षिप्त मुलाकात में सौंपा है। कहानी का लगभग सार-संक्षेप प्रस्तुत करने की विवशता के बीच इस आलेख के पाठकों से मेरा यह आग्रह है कि यदि उन्होंने यह कहानी नहीं पढ़ी है, तो इसे खोज कर जरूर पढ़ें। इस तरह कहानी के वास्तविक रस प्रभाव को तो वे महसूस कर ही सकेंगे, साथ में उन्हें यह भी स्पष्ट हो सकेगा कि सार-संक्षेपण वाली समीक्षा कहानी के सौन्दर्य और वैभव को किस तरह क्षतिग्रस्त व प्रभावहीन बनाती है।
नवीन कुमार नैथानी की एक अन्य कहानी ‘पारस’ में सौरी नामक एक ऐसे गाँव का जिक्र आता है, जो मर्दों का जंगल है, जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं और जहाँ अब किसी स्त्री का जन्म नहीं होता। सुखद है कि वह कहानी एक लड़की के जन्म के साथ खत्म होती है। स्त्री की उपस्थिति को जीवन और संभावनाओं के प्रतीक की तरह स्थापित करने का जो भाव उस कहानी में दिखा था, ‘लैंडस्लाइड’ तक आते-आते वह भाव और मजबूत और उदात्त हुआ है। वाचक ऋचा को लिखे अपने पत्र में कहता है-
“स्त्रियाँ गर्भ में ही जीवन को नहीं रोपतीं, वे उसे वहाँ भी अंकुरित करती हैं, जहाँ वे किसी के खयालों में पहुँच चुकी होती हैं।”
वाचक के ये शब्द प्रेम में डूबे किसी पुरुष का भावोच्छवास नहीं, बल्कि स्त्री और मातृत्व की उदात्तता का स्वीकार हैं। यहाँ स्त्रीत्व की उदात्तता को रेखांकित करनेवाले वाचक से, पूर्व में कहे गए ऋचा के शब्दों को भी याद किया जाना चाहिए-
“तुम इसे पहाड़ों का मलबा कह रहे हो। यह मलबा नहीं है। ये पहाड़ की मृत्यु के निशान हैं। ये पहाड़ लगातार अपनी मौत जी रहे हैं। इनकी साँसों को महसूस तो करो।”
ख्याल में पहुँच कर भी जीवन को अंकुरित करने की स्त्री की ताकत का एक पुरुष द्वारा सहज स्वीकार और एक स्त्री द्वारा मलबा को पहाड़ की मृत्यु का निशान कहा जाना, जीवन और मृत्य के इन दोनों रूपकों को एक साथ देखने पर ऊर्जा परिवर्तन चक्र का जो बृहत्तर स्वरूप खड़ा होता है, उसमें पर्यावरण और मनुष्य की अनवरत पारस्परिकता की अनिवार्यताओं की कई अर्थ छवियाँ शामिल हैं। इस तरह यह कहानी एक ऐसी रचनात्मक घटना के रूप में उपस्थित होती है, जहाँ मनुष्य और पदार्थ तथा जीव और जगत के बीच एक पारिस्थितिक संवाद और संतुलन की आवश्यकता सहज ही रेखांकित हो उठती है।
वाचक एक पत्रकार है। ऋचा की प्रेरणा से न सिर्फ वह इस पेशे में आया बल्कि भूस्खलनों की रेपोर्टिंग भी की। कहानी के आखिरी हिस्से में देवलधार में हुए भीषण भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के लिए निकलते हुए उसके अंधेरे कमरे से बाहर निकलती हुई ऋचा उसे एक नया लिफाफा पकड़ाती है-
“इसे सिर्फ तुम्हारे हाथों में पड़ना चाहिए। इसे आराम से पढ़ लेना फुर्सत में। कल बहुत सुबह निकल जाऊँगी। फिर यहाँ नहीं आऊँगी। अगर ठीक समझोगे तो मुझसे मिलने आ सकते हो। लेकिन तब, जब लिखना फिर से शुरू कर सको।”
अपने भीतर व्याप्त प्रेम की बेचैनी को वाचक पत्र के माध्यम से पहले ही ऋचा तक पहुंचा चुका है। कहे-अनकहे, भीतर और बाहर, प्रकट और गुप्त तथा उदासी जैसी हँसी और जलतरंग जैसी आवाज की संवेदनात्मक पारस्परिकता के बीच सांस ले रहे संबंध की ऊष्मा पाठक तक हर कदम पहुँचती है, लेकिन कहानी के आरंभ से अबतक मौजूद वे दोनों कौतूहल अब भी अनावृत होने की प्रतीक्षा में हैं। पाठक की जिज्ञासा और वाचक की बेसब्री कहानी के अंतिम पड़ाव पर एक हो उठते हैं-
“लिफ़ाफ़े के भीतर एक कागज है जिसमें बिना किसी सम्बोधन के चार पंक्तियाँ लिखे हुई हैं। बहुत सारे फासले के साथ। जैसे वे अलग-अलग वक्तों में लिखी गयी हों। मैं पढ़ने लगता हूँ।
मैंने भी प्रेम किया था लेकिन वह लैंडस्लाइड की चपेट में खो गया।
अब इस उखड़ी हुई धरती से मुझे प्यार है।
शायद वह वनस्पति कभी धरती पर उग सकेगी।
अगर हो सके तो अपने मन में उसे रोप लो और समवेदनाओं की बारिश में पनपने दो।”
लिफ़ाफ़े सी निकली इन चार पंक्तियों को वाचक से कहे ऋचा के आखिरी शब्दों के साथ जोड़ कर एक बार पुनः पढ़ा जाना चाहिए- “अगर ठीक समझोगे तो मुझसे मिलने आ सकते हो। लेकिन तब, जब लिखना फिर से शुरू कर सको।”
ऋचा ने लैंडस्लाइड में अपना प्रेम खोया था। उसने लैंडस्लाइड को ही अपना जीवन समर्पित कर दिया। लैंडस्लाइड की चपेट में खो चुके प्रेम की वनस्पति के पुनः उगने का उसे इंतजार है, जिसके लिए संवेदनाओं की बारिश चाहिए। उसके अभियान में वाचक का सहभागी हो जाना ही उसके लिए प्रेम का पुनराविष्कार होगा। उसकी उम्मीदों में जो ऊर्जा संचरित हो रही है उसी में जैविक और सांस्कृतिक संतुलन के बीज मौजूद हैं। ‘लैंडस्केप’ पारिस्थितिक संतुलन के उसी बीज के संरक्षण की कहानी है।
यह भी पढ़ें- रहस्यलोक की यात्रा का हासिल