भारतीय रंगमंच की दुनिया में एक श्रापित स्वप्न है- रंगकर्मी का जीवन जीना और जीवन भर नाटक करना। इसी श्रापित स्वप्न की एक कथा है विजय कुमार का नाटक “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं”, जिसकी 997वीं प्रस्तुति 11, अक्टूबर, 25 को पटना के हाउस ऑफ वेरायटी में हुआ। यह कथा सिर्फ एक नाटक की नहीं, बल्कि हर उस भारतीय रंगकर्मी की है जो अपने सीमित साधनों से एक नयी रंग-भाषा की खोज करना चाहता है। इस श्रापित स्वप्न में इब्राहीम अलकाज़ी का थिएटर-स्वपन भी शामिल है कि रंगकर्मी केवल अभिनेता नहीं, समाज के बीच काम करने वाला एक सांस्कृतिक कारक बने।
इस श्रापित स्वप्न के केस स्टडी के रुप में विजय कुमार का नाटक “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” का अध्ययन आवश्यक है। इस नाटक की प्रस्तुतियों में व्यावसायिक सुविधा या भव्य तकनीक नहीं थी, केवल अभिनेता का शरीर और उसकी चेतना थी।
यह नाटक हरिशंकर परसाई के 1967ई में रचित व्यंग्य “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” की रंगमंचीय पुनर्रचना है। यह नाटक रूप, भाषा और संवाद के स्तर पर पारंपरिक रंगमंच की सीमाओं को तोड़ते हुए एक ऐसी संरचना रचता है, जिसमें एक ‘आधुनिक-लोक’-रंगमंच की संकल्पना का निर्माण होता और इस निर्माण की प्रक्रिया को समझना इस नाटक को समझने के लिए आवश्यक है।

नाटक की जन्म कथा और अलकाजी का सपना
इब्राहीम अलकाजी का एन एस डी के पीछे का एक सपना था कि यहाँ से प्रशिक्षित अभिनेता अपने स्थानीय क्षेत्र में जाकर रंगमंच को मजबूत करेंगे, अलकाजी के उस सपने का जमीनी रूपांतरण की एक कथा है, विजय कुमार की “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं”।
कहते हैं, कभी-कभी अच्छा थिएटर एक दुर्घटना या संयोग से जन्म लेता है और इस नाटक “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” की जन्मकथा भी कुछ ऐसी ही आकस्मिक है, कुछ संयोग से बुना है। एकल नाटक के रुप में प्रसिद्ध यह नाटक आरंभ में एकल नाटक नहीं था, एक समूह नाटक था। विजय कुमार बताते हैं कि “मेरे दोस्त सत्यजीत शर्मा की शादी हुई थी और शादी में मिले समान की तरह मैं भी उसके साथ उसके घर में रह रहा था, वहाँ एक किताब मिली-‘हिंदी-उर्दू हास्य-व्यंग्य संग्रह, जिसे रवीन्द्रनाथ त्यागी ने सम्पादित किया था। उसी में था परसाई की ‘हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं’। हमने पढ़ा, हंसी भी आई और भीतर कुछ जागा भी और लगा इस पर कुछ करना है।” शुरुआत की पाँच प्रस्तुतियों में सत्यजीत शर्मा और विजय कुमार ने मिलकर काम किया। इस तरह यह एक एकल नाटक नहीं था, इसका स्वरुप भी एकदम अलग था, पाश्चात्य रंग शैली की परंपरा में।
अब पहले शो की कथा। 1995 में “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” का पहला शो दिल्ली एम्स के आडोटेरीयम में हुआ। तय यह था कि सत्यजीत शर्मा को इंट्रोड्यूस करना था, फिर नाटक शुरु होता। मगर इतना टेंशन था कि एम्स के एसी-युक्त आडोटेरीयम में भी पसीना आ रहा था। इतने में लाइट्स जली और सत्यजीत शर्मा ने विजय कुमार को इंट्रोड्युस करते हुए बोला-
“यह सत्यजीत शर्मा है…” फिर सत्यजीत शर्मा ब्लैंक।
फिर विजय कुमार ने बोला-
“मैं सत्यजीत शर्मा एंड हि इज विजय कुमार!” दर्शक में जो उनके क्लासमेट्स थे, वो हंस पड़े। और उस हंसी ने एक अजीब-सी राहत दी, जैसे कि सारा तनाव उड़ गया हो, वो लाफ्टर बहुत काम आया। फिर नाटक आगे बढ़ा। पहला शो इस तरह हुआ और अच्छा हुआ।
बकौल विजय कुमार एन एस डी के बाहर यह पहला शो था और अभी तक जो भी किया था, ज़्यादातर एन एस डी के सरकारी खर्च पर किया था, तो उसकी आदत-सी पड़ गई थी। अब यह कुछ अलग अनुभव था, थोड़ा भारी, थोड़ा डराने वाला।
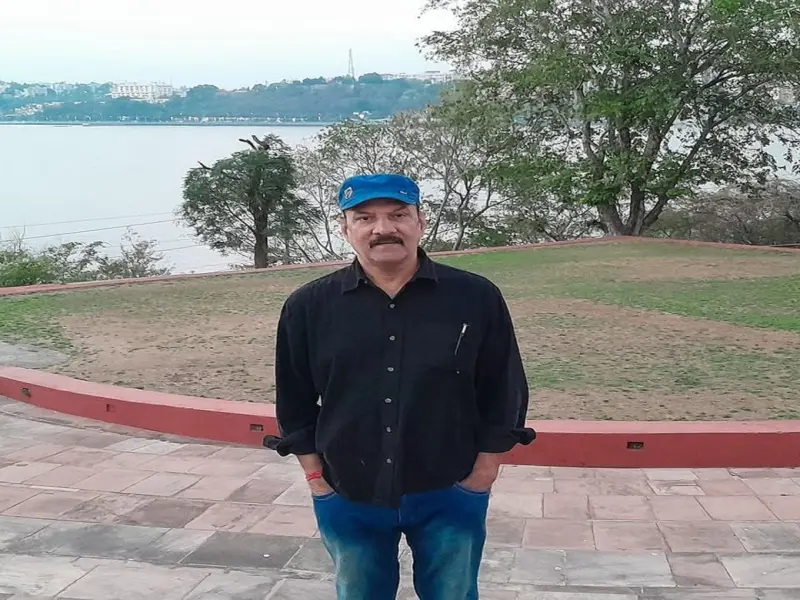
जैसा कि होता है कि हर नाटक की परिपक्वता असफलताओं से होकर निखरती है। बाद में सत्यजीत शर्मा का बंबई जाना हुआ। फेलोशिप में नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करने का अवसर का मिलना और खोना, पैसों की तंगी, फेलोशिप का मोह और पिता के साथ हादसा इन अनुभवों ने विजय कुमार को तोड़ा भी और गढ़ा भी। तब विजय कुमार ने यह नाटक एन एस डी के फेलोशिप के तहत कीर्ति जैन और उतरा बाउकर के अंदर किया, इन प्रस्तुतियों में भी यह नाटक समूह नाटक ही था। प्रगति मैदान में “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” के दो शो डिजास्टर साबित हुए, कीर्ति जैन और उतरा वाउकर ने कहा ये बेकार नाटक है, बंद करो। अगर ऐसा हुआ होता, तो इस नाटक की कथा वहीं समाप्त थी।
धीरे-धीरे विजय कुमार के सारे सहपाठी फिल्मों में चले गए – यशपाल शर्मा, कुमुद मिश्रा, मुकेश तिवारी – वह अकेले रह गए। पर उसी अकेलेपन ने इस नाटक को एकल नाटक बना दिया। इन सब के बीच उनका पटना लौटना हुआ और पटना में जब कालिदास के बाहर पहला शो एकल नाटक की तौर पर हुआ और दर्शकों से जो प्रतिक्रियाएँ और तालियाँ मिलीं, उससे आत्मविश्वास लौट आया।
यहीं से विजय कुमार का बिहार लौटना समाज में रगंमंच के प्रसार का एक प्रयोग बन गया। वह समय था जब थिएटर और भूख दोनों साथ चलते थे, बकौल विजय कुमार “जब भी पैसों की ज़रूरत होती, हम गांधी मैदान चले जाते थे। लगातार शो करते। एक बार हमें नाल खरीदना था और हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने एक दिन में छह-सात शो किये और कुल पचहत्तर रुपए जुटा और उसी दिन जाकर हमने अपना पहला नाल खरीदा था।”
थिएटर अब ‘इवेंट’ नहीं था, यह जीविका भी थी, प्रतिरोध भी और लोकसंपर्क भी। बिना संसाधन के नाटक करने की दृष्टि से और बतौर अभिनेता अपना विकास करने की दृष्टि से नाटक का यह स्वरूप अध्ययन की वस्तु है, जो नुक्कड़ पर और मंच पर एक साथ खेला जा सकता था। इस नाटक का यह स्वरूप पिछले 30 साल में एक सा नहीं रहा है। इस नाटक के वर्तमान स्वरुप के विकास की प्रक्रिया विशेष है। इस स्वरूप में ही अलकाजी के सपने, बिना संसाधन के नाटक करने और अभिनेता के प्रयोग और विकास की कुंजी भी है।
नाट्य रूप की जीवित संरचना : “नो फार्म” का सौंदर्यशास्त्र
इस नाटक में कोई निश्चित प्रारूप नहीं है “इस नाटक का फार्म नो फार्म है।” “फार्म का यह अभाव” इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो नाटक को एक जीवंत, बहती हुई सामाजिक भाषा में बदल देता है। विजय कुमार ने इस नाटक की प्रस्तुति में कई प्रकार के विकल्प की संभावना रखी है, हर बार मंचन के स्थान और दर्शक की प्रवृति समझ कर इस नाटक की प्रस्तुति बदलते रहते हैं। यह नाटक का एक इंटेलिजेंट और जीवित स्वरूप है, जो एक सक्षम और विवेकशील अभिनेता ही संभव कर सकता है। यही विवेकशील अनुकूलन वाला नाट्य स्वरूप इसकी स्थायी पहचान है, जो इसे हर बार एक नया अनुभव बनाता है।
यह जीवित स्वरूप स्थिर नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रक्रिया से प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक मंचनों में विजय कुमार का शरीर नाटक का मुख्य उपकरण था। मंच पर उनका तेज भागना-दौड़ना, देह की गति, सांस का उतार-चढ़ाव सब मिलकर एक राजनीतिक हड़कंप का प्रतीक बनाते थे।
लेकिन समय के साथ उन्होंने अनुभव किया कि यह बाहरी गति भीतर की बेचैनी का पूरा बयान नहीं दे पाती यानी देह की गति से अधिक ज़रूरी हो गया ठहराव और दर्शक की कल्पना में उत्पन्न दृश्य गति। यही वह बिंदु था जहाँ नाटक ने अपने फॉर्म को बदलना शुरू किया।

विजय कुमार के अनुसार “आप रचनात्मक प्रोसेस में हो तो आप बहुत शंका और संदेह में रहते हो। जो बाहर से देखता है, वो जजमेंटल हो जाता है।” स्पष्ट है कि उनका नाटक पूर्णता की ओर नहीं, प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। हर शो उनके लिए प्रयोगशाला है — कभी लाइट कम, कभी पूरा मंच खाली, कभी दर्शक के बीच से अभिनय। लखनऊ के एक शो में उन्होंने खुद को स्टेज के एकदम पीछे साइक्लोरामा के पास ले लिया और सामने मंच पर भी दर्शक थे। यह प्रयोग नाटक के दृश्य आयाम को बदलता रहता है। यह बदलाव बतौर अभिनेता हमेशा कुछ नया और बेहतर करने का अवसर भी देता है। कभी वे खड़े होकर अभिनय करते हैं, कभी अगले शो में वही दृश्य बैठे-बैठे करते हैं। यह निरंतर परिवर्तन ही उनकी शैली की आत्मा है, अस्थिरता ही स्थायित्व है और इस नाटक का जीवित स्वरूप गढ़ती है।
आधुनिक-लोक का निर्माण
विजय कुमार का यह बदलता फॉर्म किसी सिद्धांत से नहीं, लोक के अनुभव और अंतर्ज्ञान के साथ आधुनिक रंगमंच के विलक्षण संगम से संभव हुआ है। उन्होंने स्वीकार किया कि यह धीरे-धीरे, बहुत धीरे, लोक और शास्त्रीय रंगशैलियों से सीखते हुए विकसित हुआ।
पंडवानी की दो मुख्य शैलियाँ हैं: वेदमती और कापालिक। उन्होंने वेदमती पांड़वानी की स्थिरता से संवाद रचना का अनुशासन लिया, जहाँ कलाकार बैठकर कथा कहता है और आवाज़ में दृश्य रचता है। तीजन बाई की खड़ी या कापालिक पांड़वानी से उन्होंने ऊर्जा का ऊर्ध्वाधर प्रवाह ग्रहण किया और दोनों को मिलाकर बना – स्थिर शरीर मगर स्वर में विस्फोट।
फिर आल्हा गायन से लय और दोहराव की शक्ति आई, जिससे वाक्य मंच पर कविता बन गए। मणिपुरी लाइ हरोबा से देह की न्यूनतम गति और प्रतीकात्मक भावभंगिमा की शिक्षा मिली, जबकि बात-फरोश के लोक संवाद से नाटक में एक आत्मीय बातचीत का स्पर्श आया, जहाँ कलाकार सिर्फ कथा नहीं कहता, वह बीड़ी सुलगाते हुए, लोटा थामे, दर्शक से गुफ़्तगू करता है।
इन लोक रूपों ने “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” को विधान नहीं, विकास दिया- एक ऐसा रूप जो हर मंच, हर दर्शक और हर समय में अपने को ढाल लेता है। इन सब लोक-रूपों ने उनके थिएटर को ‘निष्क्रिय अभिनय’ से मुक्त किया।
विजय कुमार का फॉर्म केवल भारतीय लोक से नहीं, वैश्विक रंग परंपरा से भी संवाद करता है। उन्होंने रशियन आर्ट थिएटर की “अंकल वानिया” देखकर उस “धैर्य” को पहचाना, जो अभिनय की सबसे बड़ी कसौटी है। उस नाटक में एक चरित्र लगभग घंटे भर तक स्थिर बैठा वायलिन बजाता रहता है।
दरअसल नाटक की निर्माण और विकास प्रक्रिया में “क्या वर्क कर रहा है, और क्या नहीं कर रहा है” के बीच का जो संदेह है, वही असली प्रोसेस है। कलाकार जब “कर रहा” होता है, तब वह खुद भी संशय में होता है। जब कलाकार “कर रहा होता है”, तब वह किसी सुनिश्चित परिणाम की ओर नहीं बढ़ रहा होता, बल्कि खोज की प्रक्रिया में होता है। इसी खोज में वह स्वयं को और अपने नाटक को परखता है। यह संशय ही उसे बार-बार दृश्य, संवाद, गति और विराम को पुनः देखने के लिए बाध्य करता है। इसलिए प्रक्रिया सृजन से बड़ी होती है। यही अनिश्चितता का सौंदर्य विजय कुमार के इस नाटक भी में प्रवेश करता है।
अब मंच पर वे उतने नहीं भागते, वे ठहरते हैं, सुनते हैं, दर्शक को स्थान देते हैं। नाटक अब फिक्स्ड फॉर्म नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिव परफ़ॉर्मेंस है। प्रकाश, मंच-सज्जा या तकनीकी जुगलबंदी उनके लिए कभी “मुख्य” नहीं रही; उनके नाटक की तकनीक मानव उपस्थिति है।
शारीरिक अभिनय: देह एक संकेत प्रणाली के रूप में
नाटक का शरीर अभिनेता का शरीर है और अभिनेता ही कथा का केंद्र। इस नाटक में विजय कुमार का अभिनय भारतीय रंगकला में देह के प्रयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। एक छोटे से तीन फुट के क्युब जिस पर कोई खड़ा हो, तो लगे अब गिरा, तब गिरा…इस गिरने के डर के बीच विजय कुमार का शरीर कभी छोटा हो जा रहा है, कभी उसका भी विस्तार जा रहा है, कभी सिर छत छूता मालूम होता है , कभी मानो केकडे की तरह जमीन में समा रहा है, वह नेता बनकर फूले हुए, कभी आम आदमी कभी बनकर झुके हुए और कभी व्यंग्य का शिकार होकर सिकुड़ जाते हैं, मानो शरीर नहीं कोई रबड़ का गुड्डा है, जिसे जरूरत के हिसाब से बड़ा-छोटा, आरा-तीरछा किया जा रहा है। उनके अभिनय में एक देह-लय इतना सशक्त है कि शब्द गौण हो जाते हैं। थिएटर यहाँ भाषा से परे अभिनय की संगीतात्मकता में रूपांतरित हो जाता है। शरीर पर यह नियंत्रण किसी भी अभिनेता के लिए दुर्लभ है, मगर एक आदर्श स्थिति है। अभिनेता के शरीर का यह जो जादू है, अभिनेता की एक लंबी और निरंतर तैयारी को दिखाती है।

यह दैहिक अभिनय एंटोनिन आर्तो के“थिएटर ऑफ क्रुएल्टी” वाला शरीर के माध्यम से भाषा के आगे जाकर भाव कहने की बात का भारतीय लोक के हिसाब से अनुकूलन है। नाटक में विजय कुमार की देह कभी खड़े या बैठे पंडवानी के गायन की तरह है, जो कभी बतकही में बोलती है और कभी लोकगीत में नाचती है। इस देह-व्याकरण में भारतीय लोक-रूपों का समावेश है। अभिनय की इस देह व्याकरण को अभिनेता की तैयारी और अभ्यास संभव बनाती है। विजय कुमार ने बताया कि उन्होनें वर्षों हर दिन अपने शरीर पर काम किया है, जो अभिनय के लिए अपने शरीर पर आवश्यक नियंत्रण देता है। विजय कुमार ने यक्षगान, कूडियाट्टम, योग, कलरीपायट्टु मार्शल आर्ट जैसी परंपराओं से प्रशिक्षण लेकर अपने अभिनय के इस देह व्याकरण और भाषिक संरचना निर्मित की है, जो नाटक के “नो फार्म” को सजीव करती है।
विजय कुमार का शारीरिक अभिनय पर उक्त नियंत्रण ही भारतीय रंगमंच में उस दुर्लभ क्षण का सृजन करता है, जब “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” में गति से नहीं, स्थिरता से ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यह केवल मुद्रा नहीं, बल्कि भाव का फिजिकल ट्रांसलेशन है। उनका शरीर विचार का विस्तार है। मंच पर वे किसी “क्यूब” या सीमित आयाम में बैठते-उठते जाते हैं। आरंभिक पांच मिनट में दर्शक कुछ असमंजस में रहता है, मानो कुछ हो नहीं रहा। मंच पर न कोई दौड़-भाग, न कोई लाइट की जुगलबंदी, न संगीत का उछाल। बस एक व्यक्ति, अपनी जगह पर स्थिर। लेकिन इसी स्थिरता में धीरे-धीरे एक गुरुत्वाकर्षण का ब्लैक-होल पैदा होता है और पाँचवें मिनट तक आते-आते दर्शक का सारा ध्यान और उसकी सारी बेचैनी उसी बिंदु पर केंद्रित हो जाती है।
यह वही क्षण है जहाँ रंग-संयम दर्शक को अपनी ओर खींचता है। मानो यह कोई “स्थिरता का अभिनयशास्त्र” हो, जिसमें अभिनेता स्वयं को सीमित करता है, ताकि दर्शक की चेतना विस्तृत हो सके। मंच पर यह न्यूनतमता एक प्रकार का ‘रंग-ध्यान’ बन जाती है। थिएटर के इस प्रयोग में “करना” से अधिक “रोकना” महत्वपूर्ण है। अभिनेता जितना स्थिर होता जाता है, उतना ही दर्शक भीतर से सक्रिय होता जाता है। पाँच मिनट के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन घटता है, जिसमें दर्शक अब अभिनय नहीं देख रहा होता, वह अनुभव कर रहा होता है और अंतत: अस्तित्व देखने लगता है।
चरित्र आरोपण का खेल
इस नाटक में कोई स्थायी पात्र नहीं है। इसमें अभिनेता एक साथ परसाई, कृष्ण, आम जन, प्रोफेसर, और भगवान तक के रूपों में रूपांतरित होता है और “कृष्ण,” “प्रोफेसर,” “पुंजीपति,” “विनोबा भावे,” “भगवान,” सभी एक-दूसरे में घुलते-मिलते हैं। पात्र अपने “स्वभाव” से नहीं, बल्कि संबंधों से परिभाषित होते हैं। विजय कुमार का कृष्ण तभी अर्थवान है, जब वह परसाई, जनता, प्रोफेसर और राजनेता से टकराता है। इस प्रकार, पात्र यहाँ संकेतों की श्रृंखला हैं, न कि व्यक्ति-विशेष।
इस चरित्र रूपांतरण में चरित्र निर्माण में “आरोपण” एक महत्वपूर्ण उपकरण है। विजय कुमार इस नाटक में एक चरित्र पर दूसरे का आरोपण इस प्रकार करते हैं कि दर्शक को एक सतह पर “प्रोफेसर” दिखता है, पर दूसरी सतह पर “राजनेता” , तीसरी पर “साधारण नागरिक” और चौथी पर “सत्ता का प्रतीक”।
उदाहरण के लिए, प्रोफेसर के व्यवहार में जब राजनेता के परिवार का आरोपण किया जाता है, तो वह केवल हास्य या व्यंग्य का साधन नहीं रहता। यहाँ परसाई का व्यंग्य मूल स्वरूप से आगे बढ़कर सांस्कृतिक संरचना का विश्लेषण बन जाता है। “प्रोफेसर साहब” के चरित्र में यह विस्तार और आरोपण स्पष्ट है। यह चरित्र अपने भीतर राजनेता के राजनीतिक चरित्र, मध्यवर्गीय शिक्षित अभिजात की मानसिकता और सामाजिक पाखंड — तीनों का आरोपण समेटे हुए है।
विजय कुमार के एकल अभिनय में चरित्रों का आरोपण केवल संवादों के माध्यम से नहीं, बल्कि देह के स्तर पर भी होता है। जब वे प्रोफेसर से चपरासी या साधू में बदलते हैं, तो देह की गति, स्वर की बनावट, और मुख-मुद्रा ये सभी एक-दूसरे पर आरोपित होकर मल्टी-लेयर प्रदर्शन रचते हैं।
यह “बहु-कोडित अभिनय” है, जहाँ एक ही देह अनेक अर्थ संकेतित करती है। अभिनेता का शरीर “संकेत” बनता है और प्रत्येक मुद्रा, स्वर या ठहराव अर्थ की नई परत खोलता है। यही कारण है कि दर्शक एक क्षण में प्रोफेसर को देखता है और अगले ही क्षण उसी में साधू, नेता, या पिता की उपस्थिति को महसूस करता है। यह अभिनय किसी यथार्थवादी रूपांतरण का नहीं, बल्कि बहु-कोडित अभिनय का परिणाम है।
भाषा और संवाद की संरचना: भाषिक कोरियोग्राफी
हरिशंकर परसाई के व्यंग्य की आत्मा “भाषिक विरोधाभास” में निहित है और विजय कुमार ने उसे नाट्य-रूप में संरचनात्मक उपकरण के रूप में प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए “जनता सेवा करने दे, नहीं बलात् सेवा होगा। सेवा का बलात्कार।”
यह वाक्य केवल हास्य नहीं, बल्कि भाषा की संरचना में उलटफेर है। यह “सेवा” शब्द को दो परस्पर विरोधी संकेतों में विभाजित करता है, जिसमें एक ओर लोक-हित है, दूसरी ओर सत्ता का शोषण। इस तरह नाटक की भाषा सपाट अर्थ नहीं देती, बल्कि संकेतों के संघर्ष के माध्यम से अर्थ को तोड़कर नये अर्थ पैदा करती है। और इस भाषा के साथ अभिनय दर्शक को एक साथ परस्पर-विरोधी भाव और ज्ञान का अनुभव कराती है।
दर्शक का टूटता तीसरा दीवार : नाटक का ओपेन स्ट्रक्चर
विजय कुमार ने दर्शकों को निष्क्रिय दर्शक नहीं रहने दिया। एक गीत “राजा जी” के दौरान जब दर्शकों से कोरस की तरह “हा” कहलवाया जाता है, तो दर्शक नाटक का अंग-अभिनेता बन जाता है। यह नाटक “एकल अभिनय” होने के बावजूद “बहु-स्वरता” (polyphony) को बनाए रखता है। एक अभिनेता अनेक पात्रों, परिस्थितियों और आवाज़ों को जीता है।
इस नाटक में दर्शक अंधेरे में नहीं रहते, दर्शक भी अभिनेता के साथ लाइट में रहते हैं। यह व्यवस्था मंच और दर्शक के बीच की तीसरी दीवार को समाप्त करती है, जिससे नाटक एक “सामूहिक अनुभव” बन जाता है। इस प्रकार नाटक में एक “ओपेन स्ट्रक्चर” विकसित होता है, जहाँ अर्थ केवल मंच पर नहीं, बल्कि मंच और दर्शक के बीच उत्पन्न होता है।
गीत की चाशनी में व्यंग्य की दवाई
गीत जैसे “समाजवाद धीरे-धीरे आई” या “अरे भाई धोखा हो गया” केवल मनोरंजन नहीं हैं। गीत यहाँ संक्रमण का कार्य करते हैं, वे दृश्यों के बीच पुल बनाते हैं। दरअसल नाटक की रचना किसी एक केंद्र से संचालित नहीं होती, और गीत अलग-अलग केंद्रों को जोड़ने का काम करती है।
“समाजवाद धीरे-धीरे आई” या “अरे भाई धोखा हो गया” जैसे गीतों के माध्यम से दृश्य के भाव भी बदलता है। एकल अभिनय में जब अभिनेता अपने शरीर और स्वर से पूरे समाज की आवाज़ बनता है, तब गीत वह बिंदु बन जाता है जहाँ दर्शक का मन उस अनुभव से जुड़ता है। “अरे भाई धोखा हो गया” जैसा गीत दर्शक के भीतर व्यंग्य नहीं, बल्कि एक साझा अपमान और पहचान की अनुभूति जगाता है।
ये गीत कथा की रैखिकता को तोड़ते हैं और दर्शक को जाग्रत दृष्टि में वापस लाते हैं। गीत स्थिर समय-संरचना को तोड़ते हैं, रोकते हैं, और कभी-कभी पीछे लौटाते हैं। विजय कुमार के नाटक में गीत कभी-कभी कथा को तोड़ते हैं। जब दर्शक किसी भाव में पूरी तरह डूब जाता है, तब अचानक कोई गीत उठता है, जैसे व्यंग्य का तीर, जो पूरे भाव को भंग कर देता है। यह भंग ही असली संरचनात्मक सौंदर्य है। विजय कुमार के इस नाटक में गीतों का महत्व इसी में निहित है कि वे दर्शक को केवल सुनने नहीं, सोचने और अनुभव करने की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। इस प्रकार गीत की चाशनी में व्यंग्य की दवाई नाटक दर्शक को देती है।
कथ्यगत संरचना: सत्ता, व्यंग्य और यथार्थ की त्रिवेणी
यह नाटक हरिशंकर परसाई के व्यंग्य से प्रेरित है, परंतु इसका रूपांतरण केवल पुनर्पाठ नहीं है; यह एक “संरचनात्मक पुनर्रचना” है। परसाई का व्यंग्य जहाँ शब्दों के माध्यम से सामाजिक सत्ता की परतें खोलता है, वहीं विजय कुमार उस सत्ता को मंच पर “जीवित भाषा” में बदल देते हैं।
इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है — मिथक का समकालीन पुनर्पाठ।
नाटक में हर चरित्र प्रोफेसर, साधु, नेता, पंडित और उद्योगपति सब सत्ता और भ्रष्टाचार के एक ही वृत्त में घूमते हैं। यह वृत्तीय संरचना एक सामाजिक संरचना का प्रतीक है, जो कभी टूटती नहीं, केवल चेहरे बदलते हैं। ये चरित्र मूलतः सीमित सामाजिक संदर्भों में जन्मे प्रतीक हैं।
उदाहरण के लिए, जब प्रोफेसर अपनी पत्नी के आग्रह पर कार खरीदता है और फिर परिवार सहित कार में बैठता है, तो यह दृश्य केवल एक परिवार पर व्यंग्य नहीं है। यह पूरे मध्यवर्गीय परिवार पर व्यंग्य है। यहाँ “कार” “पत्नी” के सामाजिक प्रदर्शन पर व्यंग्य है और “प्रोफेसर” का व्यवहार उस बौद्धिक वर्ग पर व्यंग्य है, जो अपनी चेतना को भौतिक सफलता में विलीन कर चुका है। प्रोफेसर जब कहता है, “मैं कायस्थ हूँ”, तो यह संवाद केवल जातिगत गर्व नहीं, बल्कि उस समाजिक विडंबना का उद्घाटन है जो शिक्षा और विवेक के बावजूद जाति के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता।
दूसरी तरफ भगवान वोट माँगने मंदिर जाते हैं और पंडित कहता है “ आपके दर्शन से जन्म सफल हुआ, मगर वोट तो जात को ही जाएगा”, तो व्यंग्य धर्म और राजनीति के गठजोड़ का तीखा रूप बन जाता है।
इसी प्रकार जब उद्योगपति कहता है कि“नेता के लिए पार्टी और विचार एक अंडरवियर की तरह होते हैं, जिसे बदलते रहना चाहिए,” तो पूँजी, सत्ता और विचारधारा का गठबंधन सामने आता है।
नाटक के अंत में जब भगवान राजनीति से विरक्त होकर भैंस पालने की बात करते हैं, तब यह केवल एक हास्य नहीं, बल्कि उस सामाजिक थकान का प्रतीक है जिसमें जनता अब राजनीति से विमुख हो चुकी है।
गुजरते समय ने नाटक में एक नया दोष उत्पन्न किया है। “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” का अधिकांश व्यंग्य परसाई के 1970 के दशक के राजनीतिक लेखन से आया है, और विजय कुमार ने नाट्यांतरण में 90 के दशक के राजनीतिक प्रसंग जोड़े हैं। मगर अब 2025 चल रहा है। इन्हें समझने के लिए दर्शक के पास उस कालखंड के राजनीतिक विवेक और सत्तर के दशक के राजनीतिक इतिहास की समझ होना आवश्यक है। नए काल के दर्शकों के लिए यह एक ऐतिहासिक नाटक की तरह प्रतीत होता है। इसे देखने की एक दृष्टि यह भी हो सकती है कि यदि नाटक के राजनीतिक संदर्भों को समकालीन राजनीति के प्रसंगों से बदला जाए, तो नए दर्शकों में इसकी ग्राह्यता और प्रभावशीलता दोनों और अधिक बढ़ सकते हैं।
कुल मिलाकर “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं” एक ऐसा नाटक है जो मंच पर नहीं, दर्शक की चेतना में घटित होता है। इस नाटक के स्वरूप में एक “व्यवस्थित अराजकता” है, जो किसी निश्चित प्रारूप में बंधा नहीं है, बल्कि “नो फार्म” की तरह है। यह स्वरूप ही नाटक को ‘जीवित रचनात्मक प्रक्रिया’ बनाती है, जिसमें अभिनेता की तैयारी और विवेकशील अभिनय के दम पर हर प्रस्तुति और मंच की जरूरत के अनुसार यह नाटक अपना रुप बदल लेता है, चाहे प्रस्तुति का वह मंच गांधी मैदान हो या लंदन का थियेटर हाल।
यही कारण है कि जब मंच पर एक व्यक्ति तीन फुट के क्यूब पर खड़ा होता है और पाँचवें मिनट तक दर्शक का सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है, तो समझ में आता है कि यह नाटक केवल एक प्रदर्शन नहीं, अभिनेता और दर्शक का आत्मसंवाद है, जो अपने भीतर के और हमारे भीतर के “बिहार” में चुनाव लड़ रहा है।
इस नाटक का विकास एक कलात्मक प्रक्रिया है, जिससे नाटक और अभिनेता के विकास को समझा जा सकता है। प्रक्रिया सृजन से बड़ी होती है और कलाकार के विकास का स्त्रोत है, यह विचार ही विजय कुमार के रंगकर्म और इस नाटक के केंद्र में है। और शायद यही कारण है कि इस नाटक के कोरस में ही पटना रंगमंच के वर्तमान का निर्माण हुआ है, वो चाहे रणधीर कुमार हों या पुंज प्रकाश या फिर पंकज त्रिपाठी या अन्य कई रंगकर्मी सभी इस नाटक के कोरस का हिस्सा सैकड़ों बार रहे हैं और आज भी पटना रंगमंच की पहचान पूरे देश में अलग-अलग तरीके से बना रहे हैं। यह ही शायद इस नाटक की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो इब्राहीम अलकाज़ी के सपने का एक अंश में पुरा होने जैसा है।
और शायद अगली बार जब लाइट्स जलेंगी, इस नाटक का 1000वाँ शो भी होगा…तब फिर मंच पर वही गहरी आवाज़ गूँजेगी, दर्शक की कानों को सुनाई देगा “हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं…”, मगर अभिनेता विजय कुमार के मन को सुनाई देगा “ इस शो में क्या होगा?”


