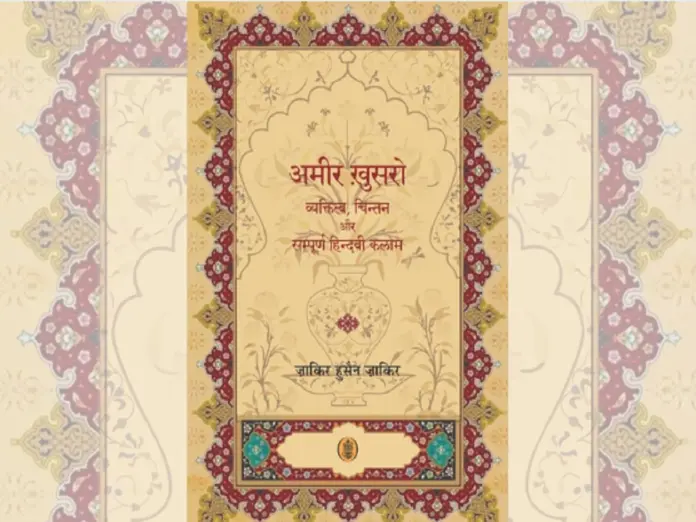किताब से ज्यादा मानीखेज है किताब की रीडिंग। यानी संवाद का पुल तैयार करने की बेचैनी। दो सदियों, दो संस्कृतियों, दो समयों और दो विचारधाराओं के बीच संवाद का पुल बनाए बगैर आप न मुकम्मल होने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, न अपनी ही चुनी हुई वीरानियों को दफ़्न कर सकते हैं। सोचती हूँ, किताब के पाठ के दौरान पाठक किससे मुखातिब होता है। लेखक से? या अपने समय-समाज-संस्कृति के प्रभाव को खाद-पानी की तरह इस्तेमाल कर एक नई संस्कृति और विचार-सौंदर्य के गवाक्ष खोलती तड़प से? सवाल यह भी है कि किताब के निश्चित फ्रेमवर्क में ढली टेक्स्ट महत्वपूर्ण है? या टेक्स्ट को डिकोड कर अपने युग तक लाती पाठक की संवेदनशील विचार-दृष्टि? सवालों के निश्चित जवाब नहीं होते। समय और कोण के अधीन वे गहरे लचीलेपन के साथ अपना रूप बदलते रहते हैं, लेकिन केंद्र में एक ही त्रिक् स्थित रहता है – कृति-कृतिकार और कृति का सहसर्जक भाष्यकर जिसे हम परंपरागत शास्त्रीय मान्यता के अनुरूप पाठक-आलोचक की निष्क्रिय भूमिका में बाँध देते हैं।
कहा जा सकता है कि पुस्तक-समीक्षा के सुनिश्चित फॉर्मेट में सैद्धांतिक विश्लेषण की उलझावभरी सुरंग के मुहाने खोले ही क्यों जाएं? पुस्तक-समीक्षा ‘रिव्यू’ है – ‘देखे’ हुए को लगभग उसी रूप में पुनः ‘दिखाने’ की परिचयात्मक प्रक्रिया। लेकिन जैसे ही कृति को अंतिम न मान कर टेक्स्ट में तब्दील करने की दृष्टि के साथ आप कृति का पाठ शुरू करते हैं, कृतिकार अपनी केंद्रीय सत्ता खोकर पाठ में तब्दील हो जाता है और पाठक की विश्लेषणात्मक पड़ताल का ऑब्जेक्ट बन जाता है। महत्वपूर्ण रहती है गहरी जुगलबंदी में बुने संवाद की प्रवाहमयता जो सदियों के अंतराल को पाट कर प्रभाव-ध्वनियों को इस खूबसूरती से अपने युग में ले आती है कि उनके जरिए मनुष्य-संस्कृति के विकास-सोपानों की यात्रा तय की जा सके। इसलिए जब मैं ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर की पुस्तक ‘अमीर खुसरो : व्यक्तित्व, चिंतन और संपूर्ण हिंदवी कलाम’ पढ़ती हूँ तो लेखक के बाध्यकारी अनुशासन को धता बताकर पाठ यानी हिंदवी कलाम के प्रभाव की पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर स्वीकार करते हैं कि यह पुस्तक कवि अमीर खुसरो (1253-1325 ई०) के साहित्यिक मूल्यांकन का मौलिक प्रयास नहीं है। इसकी अपेक्षा यदि यह एक स्तर पर 13-14वीं सदी के हिंदुस्तान के राजनीतिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश को समझने के लिए इतिहास की गलियों में चहलकदमी करती है, तो दूसरे स्तर पर उठापटक लड़ाइयों और साज़िशों की दरबारी राजनीति के बीच सर्वाइवल की कोशिश में अपने व्यक्तित्व को आकार देते महत्वाकांक्षी दरबारी कवि अमीर खुसरो पर समय-समय पर हुए शोध-कार्यों की प्रमुख स्थापनाओं को एक जगह संग्रहीत करती है।
लेखक चाहते हैं कि इस पुस्तक को अमीर खुसरो पर प्रकाशित सर्वाधिक प्रामाणिक पुस्तक ‘जवाहरे खुसरवी’ (1918) की परिवर्धित कड़ी माना जाए क्योंकि गत एक शताब्दी में कवि पर होने वाले तमाम शोध-कार्यों का समाहार इसमें कर लिया गया है। ज़ाहिर है इसलिए पुस्तक का पहला खंड परिचयात्मक होते हुए भी तीन दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक, अमीर खुसरो पर सूफी कवि निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक प्रभाव को पकड़ने की कोशिश में ‘तसव्वुफ़’ के वैचारिक दर्शन को बहुत विस्तार से स्पष्ट किया गया है। ‘तसव्वुफ़’ यानी सूफीवाद इस्लाम का वह रहस्यवादी मार्ग है जो लौकिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर अपने ‘मैं’ को खुदा के अंश के रूप में जानने की सर्जनात्मक बेचैनी है। इश्क और सादगी इस दर्शन की दो आंखें हैं और खुली हुई बाहों में सारे फलक को संतान की तरह समेट लेने की बेताबी। इसलिए वैचारिक औदार्य एवं संवेदनापरक सौहार्द इसे धर्म विशेष की कट्टरताओं तक महदूद नहीं रखते, साझा संस्कृति जैसा विचारशील पुल बनाकर धर्म, जाति, वर्ग-भेद से परे सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया की तरह सूफी संत नहीं हैं। वे कलंदर कवि हैं जो वैराग्यपूर्ण जीवन को अस्वीकार कर लौकिक जीवन भी जीता है और खुदा से सीधा संबंध भी जोड़े रखता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है मनुष्य के तौर पर अमीर खुसरो के व्यक्तित्व में पाए जाने वाले ढेर से अंतर्विरोधों और दुर्बलताओं को स्पष्ट करना। 1270-1325 ई० यानी 48 वर्ष तक दरबारी कवि के रूप में अमीर खुसरो ने सात सुल्तानों और तीन राजवंशों (मामुलक/ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश) के आश्रय में काम किया।
यह राजनीतिक अस्थिरता का वह दौर था जब तख्तनशीं सुल्तान को मौत के घाट उतार कर उसका कोई सगा-संबंधी, सिपहसालार या दुश्मन सत्ता हथिया लेता था। ऐसे में आश्चर्य होता है कि हर नया सुल्तान पुराने दरबार को ‘ठिकाने’ लगाने के दस्तूर के बावजूद अमीर खुसरो को क्यों बख़्श देता था। खुशवंत सिंह को उद्धृत करते हुए लेखक कहते हैं कि “डूबते सूरज की ओर पीठ करना और उगते सूरज की पूजा करना अगर किसी को आता था तो वह केवल अमीर खुसरो था।” इसलिए आश्चर्य नहीं कि जलालुद्दीन खिलजी के वफादार माने जाने वाले अमीर खुसरो ने उसकी नृशंस हत्या करके सुल्तान बन जाने वाले अलाउद्दीन खिलजी की ताबेदारी भी उसी निष्ठा से की और तख्नशीं होते ही तुरंत दरबार में हाजिर होकर चाटुकारितापूर्ण कसीदे भी पढ़े, मसनवियाँ भी लिखीं।
दोनों ध्रुवों को एक साथ साधने की कला में पारंगत अमीर खुसरो के व्यक्तित्व की एक और परत का उद्घाटन करते हुए लेखक बताते हैं कि कहीं-कहीं अपनी लोचशीलता के बावजूद वे फौलाद जितने मजबूत भी थे। जैसे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद गद्दीनशीं होने पर निजामुद्दीन औलिया से पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या के लिए 1000 टके पुरस्कार की घोषणा की, लेकिन इस दौरान अमीर खुसरो ने नियमपूर्वक शाम को औलिया की खानकाह में जाना कभी नहीं छोड़ा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु खुसरो के साहित्यिक व्यक्तित्व की पड़ताल है। ज़ाकिर हुसैन तमाम तरह की प्रशंसात्मक प्रवंचनाओं से बचते हुए एक वृहद साहित्यिक परंपरा में अमीर खुसरो के मूल्यांकन के हामी रहे हैं। वह अमीर खुसरो को उनके तमाम फारसी कसीदों, मसनवियों और ग़ज़लों की अपेक्षा ‘खालिक बारी’ के रचयिता के रूप में याद करते हैं। उनकी मान्यता है कि यदि उन्होंने ‘खालिक बारी’ की रचना न की होती तो वह फारसी के नक्काल कवि के रूप में याद किए जाते।
‘खालिक बारी’ आम लोगों की सुविधा के लिए रचा गया अरबी, फारसी, तुर्की और हिंदवी का अद्भुत शब्दकोश ही नहीं है, बल्कि चारों भाषाओं की व्यंजनात्मक विशिष्टताओं और शब्द-सौंदर्य को ध्वन्यात्मक लालित्य और काव्यात्मक प्रवाह में इस तरह पिरोया गया है कि काव्यात्मक आस्वाद के जरिए उन्हें समझना और स्मृति में संजोना आसान हो जाता है। जैसे : राह तरीक सबील पहचान/ अरथ तिहूँ का मारग जान”। या हिंदवी के ‘ससि’ (चाँद) शब्द के अरबी-फारसी पर्यायवाची पर आधारित यह शेर : “ससि है मह नैय्यर खुर्शीद/ काला उजला सफीद” या “अस्प घोड़ा, फील हाथी, शेर सींह/ गोश्त हेड़ा, चर्म चमड़ा, शहम पीह।”
इसके अतिरिक्त एक और मौलिकता जो उन्हें विशिष्ट बनाती है, वह है फारसी और हिंदवी में ग़ज़ल की एक-एक पंक्ति लिखकर अर्थ-विस्तार करना। यह काम दो अलहदा भाषा-संस्कृतियों को विचार-सौंदर्य के अटूट बंधन में बांधने के निमित्त किया गया जान पड़ता है। उल्लेखनीय है कि उनकी ऐसी ही एक महत्वपूर्ण ग़ज़ल के मुखड़े का उपयोग करके हिंदी सिनेमा में गीत भी लिखा गया है – “जिहाल मिस्की मकुन तुगाफल दोराय नैना बनाए बतियाँ
कि ताब-ए-हिज़्रां न दारम ए जां न लेहो काहे लगाए छतियाँ ।”
यही नहीं तद्युगीन हिंदुस्तान के प्रचलित प्रमुख व्यवसायियों जैसे रंगरेज़, हज्जाम, तेली, कहार, बढ़ई, कुम्हार, मोची, वैद्य, कलंदर, संन्यासी, तंबोली, लुहार आदि पर दोनों भाषाओं के मेल-जोल से 67 कताअ (पद्य) लिखे। वचनवक्रता, वाग्विदग्धता और काव्य-सौंदर्य इनमें देखते ही बनता है – “ख़ाल-ए-बरुख़श दीदम-ओ-गुफ़्तम कि तिलस्त
गुफ़्ता कि बिरी नीस्त दरई तिल तेले।”
(अर्थात् तेली के बेटे के हाथ और जीभ ऐसे चलते हैं कि बस! उसके गाल पर तिल देखकर मैंने कहा क्या यह तिल है? उसने कहा, अरे जाओ-जाओ, यह वह तिल नहीं जिसमें से तेल निकाला जा सके।)
दरअसल आमिर खुसरो तूती-ए-हिंद इसलिए कह जाते हैं कि वे न केवल हिंदुस्तान की सरज़मीं में जज्ब हुए, बल्कि इसकी रिवायतों और संस्कृति, भाषा और लोक को अपनाकर अद्वैत भी स्थापित किया। कहा जाता है कि उन्होंने दिल्ली में प्रचलित बोली में अरबी-फारसी की मुलायमियत घोल कर उसे हिंदवी बनाया, लेकिन सच यह है कि हिंदवी को गले लगा कर ही वे हिंदुस्तान का कंठहार बने हुए हैं। इसलिए दरबार के बाहर आकर जब अंतस का रूद्ध प्रवाह खोलते हैं, अमीर की तुर्रेदार पगड़ी उतार कर लोक से उसकी जुबान में बावस्ता होते हैं, उनकी परंपराओं और धार्मिक आस्थाओं को निष्कलुष उत्सुकता के साथ देखते-अपनाते हैं, तब उनके संवेदन, दृष्टि और वैचारिक-सौंदर्य का पाट चौड़ा हो जाता है।लिहाज़ा उनके हिंदवी काव्य के दो रूप मिलते हैं – लोक-काव्य और प्रेम-काव्य। गीत, सुखना, पहेलियाँ, मुकरियाँ, ढकोसला, निस्बत, कव्वाली शैलियों में रचित उनका लोक-काव्य संवाद, कौतूहल, वचन-विपर्यय, चुहलबाज़ी और मनोविनोद की ज़मीन पर खड़े होकर सीधा लोक-जीवन से तादात्मीकृत होता है, और उसके भीतर छिपे रस-स्रोत से रस लेकर कविता को अमृत से सींचता है। इसलिए हैरानी नहीं कि वह अब तक लोक-स्मृतियों में धंसा हैं और प्रत्येक सहृदय अपनी बाल्यावस्था में उन्हें सुन-सुनकर भारतीय संस्कृति और मेधा से परिचित होता रहा है।
अमीर खुसरो को याद करना उनकी कविता के रस में भींजना है। कुछेक उदाहरण द्रष्टव्य हैं। पहेलियाँ जो आज भी रोजमर्रा की जिंदगी में पैबस्त हैं, जैसे “हाथ में लीजे, देखा कीजे।” या “ एक थाल मोतियों भरा, सब के सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल, फिरे मोती उस से एक न गिरे।”
मुकरियाँ यानी कहकर मुकरना, जैसे “ वह आवे तब शादी होय, उस बिन दूजा और न कोय। मीठे लागें वाके बोल, ऐ सखी साजन न सखी ढोल।” सुखना यानी दो सवालों का एक उत्तर जैसे “घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों? (फेरा न था) या “अनार क्यों न चखा, वज़ीर क्यों न रखा?” (दाना न था) ढकोसला यानी बेमेल के तीन-चार शब्दों को काव्य-पंक्ति में पिरोकर रची गई चुहलबाज़ी जैसे “खीर पकाई जतन से, चरख़ा दिया चलाय है , आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाय।”
लेकिन उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है उनका सूफी कलाम – इश्क-इलाही और इश्क-मजाजी का अद्भुत संगम! अद्वैत की गाढ़ी ललक जो परमात्मा से मिलन के लिए तड़पती है, लेकिन परमात्मा सिर्फ वह नहीं जो दूर तारों के पार छुपकर कहीं मुस्कुरा रहा है, जो अपनी लाली-पगी किरणों के साथ नूर बरसा रहा है। परमात्मा वह भी है जो उसी नूर से भींज कर इंसानी शक्लो-रूह लिए मुफलिसी में जी रहा है। परमात्मा की इबादत इस भूखे-नंगे को तृप्ति और इज्जत देना भी है। इसलिए अपने फारसी कलाम में वे ऐलान करते हैं:
“काफ़िर इश्क़म मुसलमानी मोरा दरकार नीस्त/ हर रगे मन तार गश्ता हाजते जुन्नार नीस्त/ खल्क मी गोयद कि खुसरो बुतपरस्ती मी कुनद/ आरे आरे मी कुनम बा ख़्ल्क व दुनिया कार नीस्त।” अर्थात मैं इश्क़ का काफ़िर हूँ। मुझे मुसलमानी की आवश्यकता नहीं। मेरी प्रत्येक रग तार बन गयी है, मुझे जनेऊ की ज़रूरत नहीं। संसार कहता है कि ख़ुसरो मूर्तिपूजा करता है। हाँ-हाँ मैं करता हूँ, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं।”
तो हिंदवी कलाम में शब्दों की मितव्ययिता को चुप्पी में पिरो देते हैं –
“खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग।
तन मेरा मन पीउ को, दोउ भए एक रंग।”
या अनकही टीस में ढालते हैं – “भैया को दियो बाबुल महल दुमहले, हमको दियो परदेस
अरे, लखिय बाबुल मोरे काहे को ब्याहे बिदेस।”
या फिर दसों दिशाओं में गूँजता नाद बना देते हैं – “ छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के।”
इस प्रेम-काव्य में गंगा-जमुनी तहज़ीब में घुला प्रेम दो संस्कृतियों को जोड़ता है और निजामुद्दीन औलिया की मजार पर आज भी वसंत-पंचमी के दिन को गेंदे के पीले फूलों से “रंग-पर्व” के रूप में मनाता है। “सरस बन फूल रही सरसों” गीत में वे हिंदुओं के मदनोत्सव को उस समय आध्यात्मिक प्रेम की अटूट लय में बांध देते हैं जब गीत के अंतिम पद तक आते-आते कहते हैं – “तरह-तरह के फूल खिलाए, ले गढ़वा हाथन में आए,
निजामुद्दीन के दरवज्जे पर, आवन कह गए आशिक रंग
और बीत गए बरसों।”
यह खुसरो का कमाल है कि उनके काव्य की पंक्तियां न केवल आज आप्तवचन बनकर जन-जीवन में प्रयुक्त हो रही हैं बल्कि कबीर जैसे निरगुनियों, जायसी जैसे सूफियों और मीरा जैसी प्रेम-बावरी संत कवियों की वाणी में भी घुलमिल जाती हैं जैसे
“बहुत कठिन है डगर पनघट की”
“मैं तो पिया से नैन लगा आई रे”
“मोहे अपने ही रंग में रंग ले”
“तू तो साहब मोरा महबूबे इलाही”
“अम्मा मेरे बाबा को भेजो जी कि सावन आया”
“हाड़ जले जस लाकरी, केस जले जस घास। प्रीतम ऐसन मैं जलूँ, खुसरो लागी तोरी आस।”
“कागा सब तन खाइयो, चुन-चुन खाइयो मास
दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस”
और
–“ जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होय
नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोय।”
मैं कलाम में गहरी डूब रही हूँ, ज्यों विराट से साक्षात्कार कर रही हूँ। लगता है भीतर की ख़ाली गागर, जो हवा के एक झोंके से कंपकंपाकर इधर-उधर लड़खड़ाती डोलती थी, आनंद के आँसुओं से भर गई है। लबालब!
और उसके पार बहुत सी घाटियाँ और सुरंगें, अंतरिक्ष और पाताल, दिशाएँ और पगडंडियाँ साफ़-साफ़ दिखाई देने लगे हैं। दबे पाँव ‘विराट‘ के साथ चलते हुए उसकी एक-एक सांस, भंगिमा, रहस्य और रचनात्मकता को महसूसने की धीर गंभीरता क्लासिक साहित्य का बीज-स्वप्न है। विराट का साक्षात्कार अपने अंदर के कलुष और तमस को, संशय और स्खलन को, क्षमता और संभावनाओं को सीधी नज़र से देखना है। अस्तित्व के यक्ष-सवालों से दो-चार हो कर बदलते देश-काल में पुनर्विचार करना है। तपते हुए दिनों में जब खलक पर आंधियां छाईं हों और मोहब्बतों के पैग़ाम में साज़िशों की बू सूँघने का चलन बढ़ गया हो, अमीर खुसरो को शीरे की तरह अपनी रग-रग में बसा लेना सुकून और ठंडी हवाओं के संग जीना है। ऐसी तहज़ीब के संग जो आठ सौ साल से चली आ रही है, हेलमेल और इंसानियत का पाठ पढ़ा रही है, ताकीद भी करती है कि विरासतों की रखवाली हम सबको मिल कर करनी है, वरना नफरतों के बगूले तो सब कुछ निगलने को तैयार बैठे हैं।
मैं अमीर खुसरो को पुस्तक के पहले खंड में नहीं पाती। वे अपने कलाम में जिंदा हैं। लेकिन यह क्या? उनकी पेशानी पर फिक्र की मोटी लकीरें और आवाज में गम की गहरी गूंज – “चल खुसरो घर अपने रैन भई चहुं देस।” क्या यह प्रेम और विश्वास के उजालों के छीजने से पैदा हुआ दुख है? क्या यह निजी दुख की गझिन परत से छन कर आई चेतावनी है कि रैन (डार्क एज) का बंदोबस्त करने वाले हाकिम जब-जब गंगा-जमुनी तहज़ीब को खत्म करने के लिए खेतों में नफरतों के बीज बोने लगें, हम एकजुट होकर खरपतवार को नोच कर फेंक दें और यहाँ-वहाँ सब कहीं इश्क के सुनहरी बीज रोप दें।
अमीर खुसरो प्यार, सम्मान और सद्भाव का नाम ही तो है।
पुस्तक- ‘अमीर खुसरो : व्यक्तित्व, चिंतन और संपूर्ण हिंदवी कलाम’
लेखक – ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर
प्रकाशक- राजकमल प्रकाशन
मूल्य (पेपरबैक)-450 रुपये