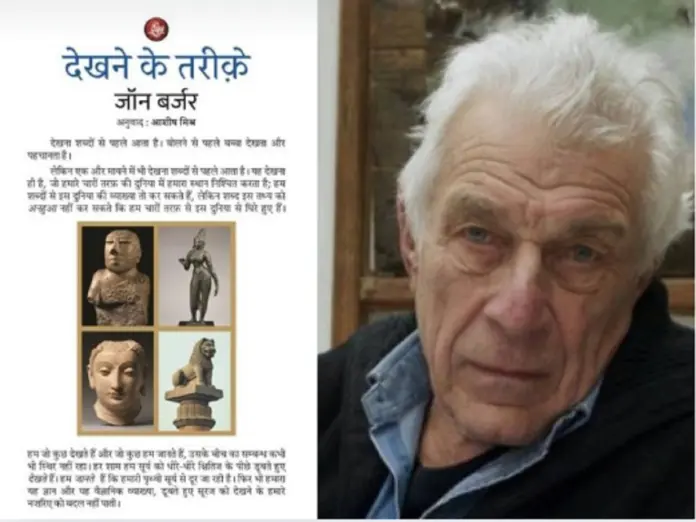“हम जो कुछ देखते हैं और जो कुछ हम जानते हैं, उसके बीच का सम्बन्ध कभी भी स्थिर नहीं रहा। हर शाम हम सूर्य को धीरे-धीरे क्षितिज के पीछे डूबते हुए देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर जा रही है। फिर भी हमारा यह ज्ञान और यह वैज्ञानिक व्याख्या, डूबते हुए सूरज को देखने के हमारे नज़रिए को बदल नहीं पाती।”-जॉन बर्जर
हमारे जानने और देखने के बीच जो भेद है, यह व्याख्या उसे बहुत आसानी से बयान करती है। जॉन बर्जर की ‘वेज़ ऑफ़ सीइंग’ इसी भेद को और साफ़ करके समझाने की मंशा से लिखी गई किताब है, जो वस्तुतः पूँजी और ताक़त के मेल की सत्ता क़ायम रखने के लिए कला के इस्तेमाल पर विस्तार से बात करती है। आधी सदी से भी पहले छपी इस किताब का हिंदी अनुवाद ‘देखने के तरीक़े’ ऐसे दौर में आया है, जब अपने नितांत एकांत में भी हम छवियों से घिरे रहने के आदी हो चले हैं। देखना जब कोई उद्देश्य या कुछ हासिल करने का विषय ही नहीं रह गया है; ट्रेन में, बस में, घर या दफ़्तर में, किसी महफ़िल या ज़रूरी बैठक में या फिर राह चलते हुए भी बहुसंख्य आबादी अपने आसपास को देखने-सुनने-महसूस करने के बजाय अपना मोबाइल फ़ोन देखते रहने की अभ्यस्त हो चुकी है, ऐसे समय में जब कद्दू (आप चाहें तो गंगाफल पढ़ सकते हैं) छीलने, टाई बाँधने या जूता पहनने की तरकीब सिखाने वाले वीडियो कई-कई लाख लोग देख डालते हों, यह किताब पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक हो जाती है। दृश्य संस्कृति की प्रचलित मान्यताओं-सिद्धांतों को चुनौती देने, बल्कि उन्हें ध्वस्त करने वाली यह किताब नए सिद्धांत नहीं गढ़ती, बल्कि पुरानों का विश्लेषण करके नई नज़र पैदा करने के सूत्र मुहैया करती है। तकनीकी में आए तमाम बदलावों के बावजूद जिसकी ज़रूरत कम नहीं हुई है।
यह किताब 1972 में छपी, मगर इससे पहले 8 जनवरी 1972 को ‘वेज़ ऑफ़ सीइंग’ कार्यक्रम बीबीसी से श्रंखला के तौर पर प्रसारित हुआ। आधे-आधे घंटे की यह साप्ताहिक श्रंखला चार हिस्सों में प्रसारित की गई- कैमरा एण्ड पेंटिंग, विमेन एण्ड आर्ट, पेंटिंग एण्ड पेज़ेशंस और फ़ाइन आर्ट्स एण्ड कॉमर्स। पहले एपिसोड के पहले ही फ़्रेम में इतालवी चित्रकार सैंड्रो बॉटिसेली की पेंटिंग ‘वीनस एण्ड मार्स’ के क़रीब पहुँचकर जॉन बर्जर जब अपनी पतलून की जेब से चाक़ू निकालकर वीनस का चेहरा अलग करते हुए दिखाई देते हैं तो पार्श्व में उनकी आवाज़ में सुनाई देती है—‘यह हमारे चार कार्यक्रमों में से पहला है, जिसमें मैं यूरोपीय चित्रकला की परंपरा के बारे में आम धारणाओं पर सवाल उठाना चाहता हूँ। वह परंपरा, जो लगभग 1400 में शुरू हुई थी, 1900 में ख़त्म हो गई। आज रात मेरी मंशा चित्रकला पर उतना ग़ौर करने की नहीं है, जितना कि इस पहलू पर कि आज हम उन्हें किस रूप में देखते हैं।’ इस पहले फ़्रेम ने ही तय कर दिया था कि ‘वेज़ ऑफ़ सीइंग’ कला को लेकर विचारहीन श्रद्धा और पवित्रता के बोध पर आघात है।
डिज़िटल का तसव्वुर तो ख़ैर जाने ही दीजिए, उस ज़माने में तो वीडियो कैसेट्स भी चलन में नहीं आए थे सो बीबीसी पर प्रसारण के बाद यह कार्यक्रम लोगों की पहुँच से बाहर हो गया। मगर उसी साल छपकर आ गई इस किताब ने न सिर्फ़ बर्जर की क्रांतिकारी दृष्टि के प्रसार में, बल्कि कला के प्रति लोगों के नज़रिये में मौलिक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाँच लोगों के विचारों से जन्मी यह किताब सात निबंधों का संग्रह है, जिनमें से तीन तो पूरी तरह से छवियों का ही संग्रह हैं। बाक़ी के चार निबंध शब्द और चित्रों का मेल हैं।
पहले अध्याय में जर्मन दार्शनिक वाल्टर बेंजामिन के ‘यांत्रिक पुनरुत्पादन के दौर में कलाकृतियाँ’ शीर्षक वाले निबंध में आए विचारों के हवाले से कला के मूल्य और यूरोपीय कला की सांस्कृतिक आलोचना है। यह अध्याय बर्जर के इस विचार का परिचय देता है कि देखना कोई तटस्थ क्रिया नहीं है, बल्कि यह किसी व्यक्ति के संचित ज्ञान, उसके सामाजिक-सांस्कृतिक विश्वासों और पूर्व अनुभवों से नियंत्रित होती है। उनका तर्क यह है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, वह कोई वस्तुनिष्ठ सच्चाई नहीं है, बल्कि हमारी अपनी जानकारियों से हवाले से व्यक्तिपरक व्याख्या है, और छवियों और कलाओं के मामले में यह बात ख़ास तौर पर खरी उतरती है।
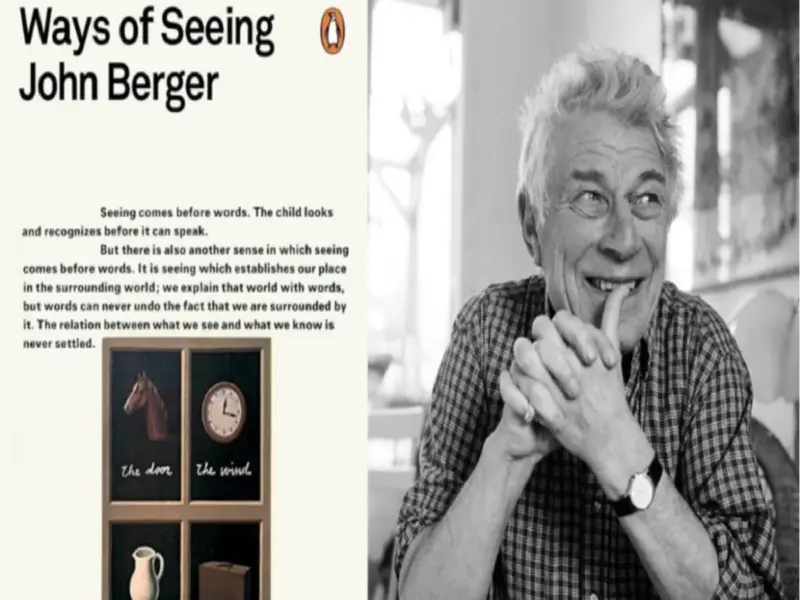
बर्जर यह भी समझाते हैं कि कैमरे के आविष्कार के बाद किसी कलाकृति की हूबहू प्रतिकृतियाँ तैयार करने और छवियों को दूर-दूर तक फैलाने की इसकी क्षमता ने मूल कलाकृतियों को देखने-समझने और महसूस करने का हमारा तरीक़ा बदल दिया है। कला के इतिहास की पड़ताल करते हुए बर्जर किसी कलाकृति में निहित सियासी नज़रिये को समझने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हैं। बताते हैं कि कला इतिहास की निर्मिति अक्सर उसी ‘रूप’, ‘स्थिति’, ‘सत्य’ या ‘सौंदर्य’ से होती है, जो कला के विद्वान इतिहासकार किसी पेंटिंग के लिए तय कर देते हैं। इसके उलट उनका तर्क है कि ये सारी मान्यताएँ अब तक बदल चुकी दुनिया की मान्यताओं से मेल ही नहीं खाती हैं, बल्कि, ये तो हमें बीते दौर की कलाकृतियों के वास्तविक प्रभाव से दूर करके, उनसे संवाद करने की लियाक़त भी हमसे छीन लेती हैं। वह उन्हें ऐसे पवित्र ‘सांस्कृतिक रहस्यवाद’ से घेर देती हैं, जो सत्ता में बैठे लोगों के फ़ायदे के लिए उनके ही विश्वास और मूल्यों को क़ायम रखता है।
दूसरे शब्दहीन अध्याय में कुछ पेंटिग्ज़, फ़ोटोग्राफ़ और विज्ञापन की कतरनें हैं। इन तस्वीरों की नारी छवियों में कुछ मशहूर चेहरे दिखाई देते हैं, विविध उत्पाद के विज्ञापनों में कुछ अनाम मॉडल भी, और इन सारी तस्वीरों का मकसद एक ही है—उनकी देह यष्टि के बहाने देखने वाले का ध्यान खींचना और उनमें आकर्षण पैदा करना। यहाँ कुछ लिखे बग़ैर ही वह ‘मर्द की दृष्टि-तुष्टि के लिए स्त्री शरीर को वस्तु में बदल देने’ और इस सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए बुने गए वाक् जाल को तार-तार करते हैं। यह अध्याय कला की दुनिया में पुरुष दृष्टि (मेल गेज़) की पड़ताल करते हुए तर्क देता है कि यूरोप की कला परंपराओं, ख़ास तौर पर तैल चित्रों, ने ऐतिहासिक रूप से औरतों को पुरुष के आनंद और मालिकाना हक़ वाली वस्तु के तौर पर पेश किया।
इस अध्याय से गुज़रते हुए हम अपने पूर्व अनुभवों से कितने ही प्रसंग याद कर डालते हैं। किताब में जो बातें यूरोप के विज्ञापनों के हवाले से कही गई हैं, उस लिहाज़ से भारतीय विज्ञापनों की दुनिया भी कोई अपवाद नहीं रही है। नारी की मोहक छवियों वाले कितने ही विज्ञापन निगाहों के सामने घूमने लगते हैं, गुज़रे दिनों की फ़िल्मों के पोस्टर (इधर तो बरसों से मैंने कोई फ़िल्म देखी नहीं और जहाँ-तहाँ पोस्टर लगाने की रवायत भी अब नहीं रही।) और एक ज़माने में धूम मचाने वाले किंगफ़िशर के कैलेण्डर भी। मोहन मीकिन के अध्यक्ष रहे कपिल मोहन का एक इंटरव्यू बार-बार याद आता रहा, जिसमें उन्होंने ‘ओल्ड मंक’ का विज्ञापन नहीं करने की वजहें गिनाई थीं।
तीसरा निबंध इसी बात को आगे बढ़ाता है, यह ‘निर्वस्त्रता’ (अपने लिए, अपने आप) और ‘नग्नता’ (दूसरों के द्वारा निर्वस्त्र और वस्तु के रूप में देखा जाना) के बीच के फ़र्क को विस्तार से रेखांकित करता है। कालजयी चित्रों और आधुनिक दौर के विज्ञापनों को एक साथ रखकर, बर्जर ऐसे चित्रण की निरंतरता बताते हैं और यह भी कि कैसे ये चित्रण महिलाओं को लगातार यह अहसास दिलाने में मददगार होते हैं कि वे दूसरों को कैसी दिखाई देती हैं। क्लासिक तैल चित्रों को नए ज़माने के विज्ञापनों के साथ रखकर, वह निष्कर्ष देते हैं कि स्त्री को वस्तु में तब्दील कर देने की यह अंतर्निहित गतिशीलता लगातार बनी हुई है, पेंटिग्ज़ में स्त्रियों को जिस तरह चित्रित किया जाता रहा था, वह नए दौर के प्रचार तंत्र में उनके प्रतिनिधित्व की प्रस्तावना से अलग हरगिज़ नहीं था। वह इस बात पर भी ज़ोर देते हैं कि इसका रिश्ता यक़ीनन यौनिकता से भी है।
चौथा अध्याय भी फ़ोटो निबंध है, जिसमें पुनर्जागरणकाल और उसके पहले के भी चित्रों की प्रतिकृतियाँ शामिल हैं। इनमें से ज़्यादातर आलंकारिक हैं, धार्मिक विषयों पर केंद्रित हैं, कुछ पौराणिक गाथाओं, मृत्यु और कुलीन वर्ग के प्रतिनिधियों का चित्रण हैं, और स्टिल-लाइफ़ के अध्ययन के भी। ये चित्र एक तरह से अगले अध्याय की पूर्व पीठिका तैयार करते हैं, जिसे दृश्य-प्रस्तावना और संसाधन दोनों ही रूपों में डिज़ाइन किया गया है। और जिसे पाँचवाँ अध्याय पढ़ लेने के बाद और बेहतर ढंग से समझने लिए एक बार फिर से देखा जा सकता है. कई ऐसे चित्र हैं, अगले अध्याय में निहित बर्जर के तर्कों को साबित करने के लिए जिनका इस्तेमाल बख़ूबी किया जा सकता है—मसलन बर्जर का यह दावा कि तैल चित्रकला का इस्तेमाल, शासक वर्ग की चापलूसी के साथ ही पूँजीवाद का एक आर्थिक, दार्शनिक और नैतिक तंत्र विकसित करके उसे वैधता दिलाने की ख़ातिर किया गया।
पाँचवें निबंध में बर्जर, पूँजीवाद, कला और यूरोपीय पेंटिग्ज़ के विषयों के आपसी रिश्तों की पड़ताल करते हैं। थोड़ा तल्ख़ी भरे व्यंग्य से इसकी शुरुआत में ही वह कहते हैं कि ‘तैलचित्र अमूमन वस्तुओं का चित्रण करते हैं,’ और फिर यह भी कि ये वस्तुएं कमोबेश ख़रीद-फ़रोख़्त के लायक़ होती हैं। शुरुआत में हालांकि उनकी यह निष्पत्ति इस लिहाज़ से भ्रमित करती है कि किसी वस्तु के चित्र का मालिक होना, उस वस्तु के मालिक होने की तरह हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि चित्रित वस्तु इस्तेमाल के सर्वथा अयोग्य है। मगर इस अध्याय में बर्जर विस्तार से इसकी व्याख्या करते हैं, वास्तविक ज़िंदगी में किसी चीज़ का मालिक होने और तैलचित्र की परंपरा में निहित देखने के तरीक़े के बीच एक जटिल समरूपता भी स्थापित करते हैं।
वैसे तो ऑयल पेंटिंग्ज़ पहले से ही चलन में रहीं, मगर बर्जर के मुताबिक 16वीं शताब्दी के यूरोप में कैनवस पर तैल रंगों से चित्र बनाने की एक विशिष्ट शैली और तकनीक का विस्तार शुरू हुआ, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में प्रभाववाद और क्यूबिज़्म का उद्भव होने तक जारी रहा; फ़ोटोग्राफ़ी के व्यापक चलन के बाद तैलचित्रण की इस परंपरा की ख़ूबी समझा जाने वाला ‘यथार्थवाद’ महत्व का नहीं रह गया। यों अपने उरूज के दौर में तैल चित्रकला की इस शैली ने ‘यथार्थवाद’ और ‘कलात्मक प्रतिभा’ जैसी रवायतों को परिभाषित किया, जो आज भी कला इतिहास का हिस्सा बनी हुई हैं। बर्जर रेखांकित करते हैं कि यह परंपरा इस विश्वास से जुड़ी है कि ‘कला समृद्ध तभी होती है, जब समाज में कला के प्रति प्रेम रखने वाले मौजूद हों’। और फिर वह इस सवाल के जवाब की तलाश करते हैं कि ‘कला के प्रति प्रेम क्या है?’
अगला यानी छठा अध्याय चित्रावली है, जो तैलचित्रों और तस्वीरों के हवाले से यह रेखांकित करता है कि कैसे कला ने ऐतिहासिक रूप से पूँजी, ताक़त और विचारधाराओं को वैध ठहराने का काम किया। इन तस्वीरों की उपयोगिता किताब पढ़ने वालों को समाज के वर्ग-भेद, नारी-देह को वस्तु की तरह बरतने और उन पर हक़ जताने के अंतर्निहित संदेशों का विश्लेषण करने के लिए उकसाने की है। यह अध्याय पहले पेंटिंग्ज़ और बाद में फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिये ख़ास तरह की अभिजात मान्यताओं को बढ़ावा देने का निष्कर्ष देता है।
सातवें और आख़िरी निबंध में, वह तस्वीरों की दुनिया बदलने में प्रचार और विज्ञापन की संस्कृति और लुभावनी-रंगीन छवियों के विकास के बीच संबंधों पर विचार करते हुए तर्क देते हैं कि ये ऑयल पेटिंग की दृश्य भाषा के ही परिष्कृत उत्तराधिकारी हैं। बर्जर बताते हैं कि विज्ञापन अपने उत्पादों के ज़रिये बदलाव का लुभावना वायदा करके मनुष्य को सिर्फ़ उपभोक्ता बन जाने के लिए ललचाते हैं, उसे यक़ीन दिलाते हैं कि ‘आप वही हैं जो आपके पास है’, और समाज में ईर्ष्या की भावना पैदा करते हैं, जो आधुनिक पूँजीवाद के विकास का ज़रूरी तत्व है। बक़ौल जॉन बर्जर, विज्ञापनों और निऑन साइनबोर्ड से जगमगाते शहरों की छवियों को अक्सर ‘मुक्त दुनिया’ का प्रतीक मान लिया जाता है.श। हालाँकि, चुनने-पसंद करने की यह आज़ादी भ्रामक है; उपभोक्ताओं को यह चुनने का विकल्प तो दिया जाता है कि वे कौन से उत्पाद खरीदें, लेकिन सच यह है कि उपभोग न करने का विकल्प हमारे पास है ही नहीं। वह कहते हैं कि विज्ञापनों की दुनिया की व्याख्या और वास्तविक दुनिया में बहुत विरोध है। विज्ञापन तो क्रान्ति तक का अनुवाद अपनी भाषा में कर देते हैं।
जेनेट विंटरसन ने इस किताब के बारे में अपनी राय देते हुए कहा कि बर्जर विचारों को उसी तरह सँभालते हैं जैसे एक कलाकार रंगों को सँभालता है। तो बर्जर के पैलेट के इन रंगों का जादू महसूस करने और निगाहों के सामने पड़ने वाले दृश्यों को देखने और उनके निहितार्थ समझने की लियाक़त पैदा करने के लिए यह एक ज़रूरी किताब हो जाती है।
किताबः देखने के तरीक़े
लेखकः जॉन बर्जर
अनुवादः आशीष मिश्र
विषयः कला-आलोचना
प्रकाशकः राजकमल पेपरबैक्स
क़ीमतः 299 रुपये