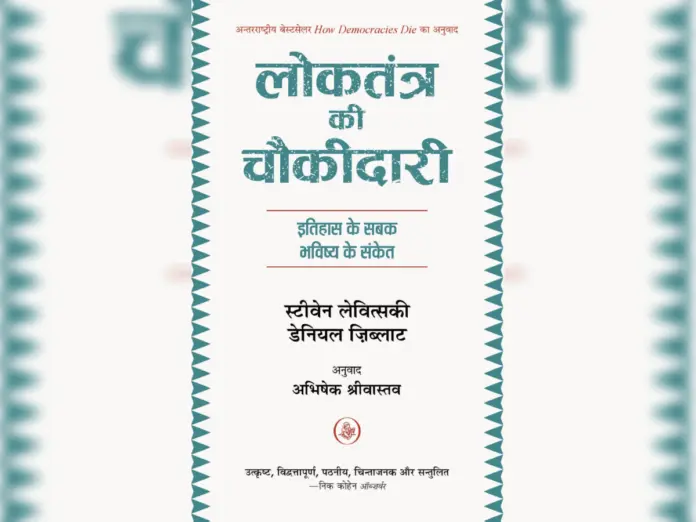प्लेटो ने अपनी पुस्तक ‘द रिपब्लिक’ में सामाजिक-न्याय के सवाल और राजनीति के आदर्श स्वरूप पर बात करते हुए गुणवत्ता और प्रभाव की दृष्टि से पांच तरह की राजनीतिक सरकारों पर विचार किया है।तर्क और संवेदना की आधारभूमि पर खड़े दर्शनशास्त्री सम्राट के नेतृत्व में बनने वाली सरकार एरिस्टोक्रेसी को उन्होंने सर्वश्रेष्ठ बताया, तो अराजकता को गर्भ में धारण करके उदित होने वाले लोकतंत्र को मनुष्य-अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती। प्लेटो की मान्यता थी कि मनुष्य तीन आदिम प्रवृत्तियों से संचालित होता है – रीज़न, स्पिरिट और भूख, जिन्हें भारतीय दर्शन में सत, रज, तम की त्रयी में भी अनूदित किया जा सकता है। अभिजात-तंत्र (सामाजिक-न्याय की पक्षधर संवेदनशील तर्क बुद्धि) से टाइरैनी (निरंकुशतंत्र) की यात्रा को वे सत्ता की अराजक भूख से संचालित होने वाली विघटनशील यात्रा मानते हैं जो पहले आजादी का भ्रम देकर वोट को सामूहिक पहचान के पॉप्युलिस्ट हथकंडे में बदलती है और फिर डेमोगॉग की प्रवाहपूर्ण लच्छेदार वक्तृता शैली में वोटर की तर्कबुद्धि को कैद कर लेती है। यह डेमोगॉग सोफिस्ट संस्कृति का उन्नायक है जो क्षरणशील भावुकतापूर्ण उन्माद और आत्ममुग्धतापूर्ण मूल्यों की प्रतिष्ठा कर रीज़न और स्पिरिट को हाशिए पर धकेल देता है। डेमोगॉग द्वारा प्रस्तावित नई मूल्य-व्यवस्था अनियंत्रित हो जाने पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को तहस-नहस कर निरंकुशता में ढल जाती है। पांचवी सदी ईसा पूर्व प्लेटो द्वारा व्यक्त की गई ये आशंकाएं समय के साथ कितनी सही साबित हुईं हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज भी विश्व अधिनायकवादी हिटलर और फासिस्ट मुसोलिनी की मनुष्यविरोधी बर्बर राजनीति की स्मृतियों से नहीं उबर पाया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हर बार लोकतंत्र का लबादा ओढ़ कर बर्बर राजनीति दबे पांव समाज में घुसपैठ करने आ जाती है। तो क्या एक बार फिर प्लेटो से इत्तेफाक रखकर हम यह मानें कि तानाशाह आम आदमी के अंतर्मन में सांस लेती निरंकुश भूख का ही परिणाम है, जो बहुसंख्यक समूह के रूप में लामबंद होकर इससे लाभान्वित होना चाहती है?
इस यक्ष-प्रश्न को सुलझाने के लिए समय-समय पर राजनीतिक चिंतकों, दर्शनशास्त्रियों और साहित्यकारों ने अनेक प्रयास किए हैं, और पाया है कि सत्ता का हर रूप अंततः भ्रष्ट होने के लिए अभिशप्त है। साथ ही यह भी स्वीकारा है कि तमाम खामियों के बावजूद लोकतंत्र ही राजनीति का सर्वाधिक मनुष्य-सहयोगी रूप है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व – ये तीन ऐसी मूलभूत विशिष्टताएं हैं जो आम आदमी की स्वायत्तता, गरिमा और प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने का वायदा करती हैं। अतः आज बहस इस बात पर नहीं कि लोकतंत्र का क्या विकल्प हो, बल्कि इस बात पर है कि लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए? कि लोकतंत्र में “लोक” यानी आम आदमी क्या सिर्फ एक निष्क्रिय मतदाता है या सत्ता का सक्रिय भागीदार? उसे सिर्फ नेतृत्व को चुनना है या नेतृत्व को सामाजिक न्याय की समतामूलक दार्शनिक अवधारणा के प्रति उत्तरदायी भी बनाना है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर स्टीवन लेवित्सकी और डेनियल जिब्लाट अपनी महत्वाकांक्षी पुस्तक “हाउ डेमोक्रेसीज़ डाई” में लोकतंत्र की रक्षा के इर्द-गिर्द ऐसे अनेक सवालों से जूझते हैं। अभिषेक श्रीवास्तव के शानदार अनुवाद के साथ हिंदी में यह पुस्तक “लोकतंत्र की चौकीदारी” शीर्षक से आई है जहां मुख्य रूप से तीन सवालों पर विचार किया गया है। एक, लोकतंत्र क्यों और कैसे कमजोर होता है? दो, लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व किस पर है – लोक पर या राजनीतिक दलों पर? तीन, लोकतंत्र की रक्षा के क्या उपाय हैं? दरअसल ये तीनों सवाल एक-दूसरे से जुड़े हैं और इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि जाहिरा तौर पर लोकतंत्र में लोक की प्रधानता होने के बावजूद लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व औसत मतदाता पर नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टी और राजनेता के चरित्र पर टिका हुआ है। यही वह बिंदु है जहां से राजनीति में डेमोगॉग की चुपचाप आहट होती है और परिस्थितियों का फायदा उठाकर वह तानाशाह बन बैठता है। लिहाजा इन पेचीदा सवालों का जवाब पाने के लिए लेखक-द्वय ने उत्तरी एवं लैटिन अमेरिका, यूरोप एवं कुछेक एशियाई देशों की सौ-डेढ़ सौ बरस पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का विशद अध्ययन किया है। साथ ही आंकड़ों एवं तथ्यों से भरी शोध-सामग्री को अधिक ग्राह्य बनाने हेतु जहां-तहां कुछ किस किस्सों-कहावतें को भी दर्ज किया है। सबसे पहले एक लोककथा। कहते हैं, एक बार हिरण और घोड़े में लड़ाई हुई। थका हुआ घोड़ा शिकारी के पास गया। शिकारी ने मदद का वायदा किया और कहा, बस मुझे तुम्हारे मुंह में लोहे से जुड़ी लगाम डालनी होगी और पीठ पर जीन कसनी होगी ताकि दुश्मन का पीछा और शिकार करने में मदद मिले। फिर जब जंग जीत ली गई और घोड़े ने जीन-लगाम हटाने को कहा तो जवाब मिला, “ऐसी भी क्या जल्दी है दोस्त! जैसे हो चुपचाप पड़े रहो।” किस्से का सच राजनीति का घिनौना दुःस्वप्न है। लेखक बताते हैं, विपक्ष की ताकत से घबराकर जब सत्तासीन दल किसी बाहरी ताकतवर संगठन को अल्पकाल के लिए सरकार बनाने का निमंत्रण देता है, तब वह क्षण लोकतंत्र की पराजय का क्षण होता है। कथन की पुष्टि के लिए वे बताते हैं कि इटली में 1922 के चुनाव में समाजवादी दल को प्रत्यक्षतया न हरा पाने की कसक लिए जब तत्कालीन सम्राट ने मुसोलिनी को प्रधानमंत्री की हैसियत से सरकार बनाने का न्योता दिया, तब उनके सामने फौरी लक्ष्य समाजवादियों को निपटाने का था। दूसरे, उन्होंने मुसोलिनी की ताकत को भी कमतर करके आंका। इसका कारण यह था कि मुसोलिनी को कुल 535 वोटों में से 35 वोट ही मिले। यानी माना गया कि अकेले अपने दम चुनाव जीतने का माद्दा उसमें नहीं। दूसरे, तीस हज़ार संख्या-बल के साथ गठित उसका गिरोह “ब्लैकशर्ट्स” देश भर में हिंसक उपद्रव करने के लिए कुख्यात था। यानी हिंसा फैलाने और हिंसा को नियंत्रित करने में उसका उपयोग किया जा सकता है।
ठीक यही स्थिति वेनेजुएला में 1992 में घटित हुई जब सेना के कनिष्ठ अधिकारी ह्यूगो चावेज़ और उसके साथियों को तख्तापलट की असफल कोशिश में गिरफ्तार किया गया। उस समय देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध असंतोष इतना अधिक फैल चुका था और जनता राजनीतिक दलों से इतनी अधिक संत्रस्त थी कि गिरफ़्तारी के बावजूद चावेज़ के प्रति उसकी सहानुभूति बनी रही। सत्ता पर पुनः क़ाबिज़ होने की अभिलाषा में पूर्व राष्ट्रपति राफेल काल्डेरा ने स्थिति का भरपूर फ़ायदा उठाया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर स्वयं को निष्पक्ष घोषित किया और राष्ट्रपति बनने के बाद चावेज़ की रिहाई का वादा कर जनता के ग़ुस्से को अपने लिए वोट में तब्दील कर लिया। उनके इस कदम ने उन्हें 1993 में सत्ता तो दिला दी, लेकिन 1994 में जेल से रिहा होकर सक्रिय राजनीति में भाग लेने वाले चावेज़ की छवि को इतना अधिक लोकप्रिय और संवैधानिक बना दिया कि अगले चुनाव में वह न केवल बहुमत से जीता, बल्कि मृत्युपर्यंत (2013) निरंकुश नीतियों के कारण वेनेजुएला से लोकतंत्र को स्थगित रखा।
लोकतंत्र संवेदना और जिम्मेदारी से भरी नाजुक राज्य व्यवस्था है। सत्ता की अनियंत्रित भूख और इस कारण की जाने वाली आत्मघाती संधियों की विवशता अक्सर पाॉपुलिज्म को भुनाने के चक्कर में छुपे हुए तानाशाह को नायक बना लेती है। इसलिए सबसे जरूरी है तानाशाह की पहचान। दोनों लेखकों ने तानाशाह के निरंकुश व्यवहार की पहचान की चार प्रमुख कसौटियाँ बताई हैं।
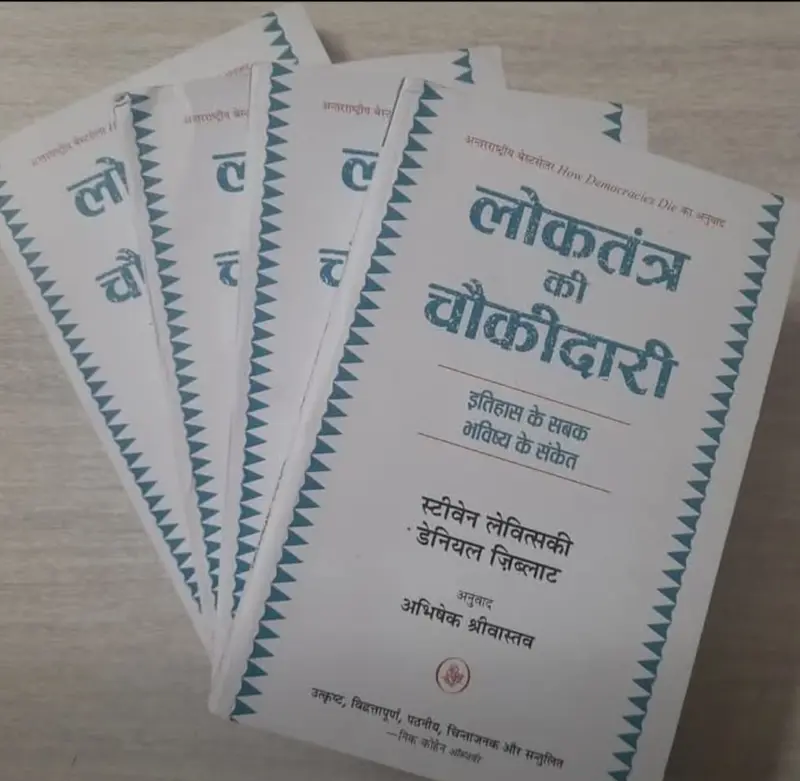
(१) क्या वे अपने आचार-व्यवहर और नीतिगत निर्णय के आधार पर लोकतंत्र को निरंतर कमजोर कर रहे हैं?
(२) क्या वे अपने राजनीतिक विरोधियों को देशद्रोही, विदेशी एजेंट या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं?
(३) क्या वे अपने समर्थकों द्वारा की गई राजनीतिक हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियों पर चुप रहते हैं और उन्हें दंडित करने से साफ इंकार करते हैं? क्या वे अपने सहयोगियों के जरिए प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक संगठनों पर प्रायोजित हमले करवाते हैं?
(४) क्या उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता (यानी अभिव्यक्ति के अधिकार, विरोध-प्रदर्शन के अधिकार, सरकार की आलोचना के अधिकार आदि) को बाधित करने के लिए दमनकारी उपाय या कानून बनाए हैं? क्या उन्होंने विपक्षी दलों, नागरिक समाज और मीडिया में अपने आलोचकों के खिलाफ कानूनी या दंडात्मक कार्यवाही करने की धमकी दी है?
दरअसल लोकतंत्र की परिचालक शक्ति है दोनों पक्षों के बीच परस्पर संवाद, सहयोग, विश्वास एवं सम्मान का भाव। यह भाव सहिष्णुता को पुष्ट करता है और चुनाव में हार-जीत को निजी प्रतिष्ठा का सवाल बनाने की बजाय लोकतंत्र एवं जनता के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखता है। लेकिन तानाशाह मूलतः संवाद और आलोचना के प्रति असहिष्णु होता है। अतः वह लोकतांत्रिक ढांचे में घुटन और अपमान महसूस करने लगता है। पुस्तक में लेखक-द्वय इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला, तुर्की आदि कई देशों से ढेर सारे उदाहरण देकर अपनी बात पुष्ट करते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूँगी -पेरू के फुज़िमोरी का, जो राष्ट्रपति बनने से पहले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सीनेटर बनने की चाह और टिकट न मिलने की असफलता ने उन्हें प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने को प्रेरित किया। व्यवस्था से बेहद नाराज लोगों ने “बाहरी” और “भले” समझे जाने वाले आदमी के रूप में फुज़िमोरी के वादों और दावों पर विश्वास कर चुनाव जिता दिया। फुज़िमोरी बुनियादी तौर पर तानाशाह नहीं था। लेकिन हर बार बिल पास कराने के लिए कांग्रेस के पास जाना, उसे कन्विंस करना और सहयोग की मांग करना उसे सुहाता नहीं था। रुष्ट होकर जब उसने विरोधियों को कायर और देशद्रोही बताया, संविधान को सख्त और बाध्यकारी कहा तो फुज़िमोरी की लोकतांत्रिक आस्था के प्रति सशंकित होकर कांग्रेस-मीडिया-अदालतों ने नकेल कसने की कोशिश की। लिहाज़ा कांग्रेस एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं से तनाव इतना बढ़ा कि 1992 में उन्होंने कांग्रेस और संविधान दोनों को भंग कर देश में विधिवत् लोकतांत्रिक-तानाशाही घोषित कर दी।
तानाशाहों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं – सत्ता का केंद्रीकरण, संविधान का दुरुपयोग, मानवाधिकारों का हनन, मीडिया एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा, विपक्ष का दमन, राष्ट्रवाद और उन्माद का प्रसार, सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता, और कल्ट (लार्जर दैन लाइफ यानी करिश्माई व्यक्तित्व) का निर्माण। लेखक-द्वय मानते हैं कि लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था का सबसे मजबूत प्रकार है। इसलिए आज के वैचारिक एवं प्रगतिशील युग में तानाशाह भी खुलकर असली चरित्र में सामने आने से कतराते हैं। लोकतंत्र की आड़ लेकर उन्हें अपनी लिबरल और प्रगतिशील छवि बनाए रखना जरूरी हो जाता है। लिहाज़ा इन्हें धीमे-धीमे कई चरणों में संपन्न किया जाता है। सबसे पहले मैच के रेफरी को अपनी ओर मिला लिया जाता है। यानी विपक्षी नेताओं और विरोधियों को राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कहकर, देश पर आतंकवाद और युद्ध के खतरों की तलवार लटका कर, हिंसा और नफ़रत के उन्माद में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी पहचान का मुद्दा पिरो कर धीरे-धीरे न्याय व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था, मीडिया और शिक्षा संस्थाएं, खुफिया एजेंसियाँ, कर नियमन एवं दंड अभिकरण नियंत्रित कर लिए जाते हैं। यह कार्रवाई इतने सुनियोजित और क्रमिक ढंग से होती है कि ठीक आंख के सामने संविधान को गुपचुप बदले जाने की प्रक्रियाएं भी अनदेखी रह जाती हैं।जिन नेताओं, जजों, कारोबारियों, पत्रकारों आदि को आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उन्हें “ख़रीदने” और “निबटाने” से लेकर मनोनुकूल नई भर्तियाँ भी की जाती हैं और ब्लैकमेलिंग के लिए उनके भ्रष्टाचार/अनैतिक कृत्यों की गुपचुप वीडियो फिल्म बना ली जाती है। राष्ट्रपति फुज़िमोरी का खुफिया सलाहकार व्लादिमिरो मोंटेसिनो इस काम में बेहद माहिर था। 1999 में एक वीडियो में उसने गर्वोन्नत भाव से कहा कि सारे टीवी चैनलों के मालिक “अब लाइन पर आ चुके हैं … मैं रोज उनके साथ साढ़े बारह बजे बैठक करके शाम के समाचारों की योजना बनाता हूँ।” संस्थानों पर पूरी तरह काबिज हो जाने के बाद विपक्ष की खबर ली जाती है। तानाशाह समूचे विपक्ष को एकमुश्त खत्म करने की बजाय सबसे ज्यादा ताकतवर विपक्षी नेता को टारगेट करता है। फिर उसका उपहास, अपमान, उपेक्षा करके या देशद्रोही, गद्दार, आतंकवादी कहकर उसकी छवि को निरंतर देश-विरोधी साबित किया जाता है। जैसे चुनाव कैम्पेन में बराक ओबामा को सेकुलर मुसलमान प्रचारित कर अंदेशा जताया गया कि उनके राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका पर समाजवादियों का कब्जा हो जाएगा। इसके बाद चुनाव व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया जाता है। जैसे मलेशिया में बहुसंख्यक मलय आबादी के वोट से चुनाव जीतने वाली सत्ताधारी यूएमएनओ पार्टी ने संसदीय क्षेत्र का परिसीमन इस प्रकार किया कि सत्तर प्रतिशत से ज्यादा क्षेत्र मलय-बहुल हो गए। हंगरी में 2010 में इसी तरह डेमोग्राफी के साथ छेड़छाड़ कर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। सबसे अंत में आती है संविधान से छेड़छाड़ या बदलने की मुहिम। यहाँ एक बार फिर फुज़िमोरी को सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है। 1992 में अपनी ही सत्ता का तख्तापलट कर “लोकतांत्रिक तानाशाह” बनते हुए फुज़िमोरी ने 1993 में नया संविधान बनाया, जनमत-संग्रह से इसे वैध बनाया और मनमानेपन से 1995 के बाद 2000 का चुनाव भी जीत लिया। हालांकि लोकतंत्र महज चुनावी लोकतंत्र में सीमित हो गया था और चुनाव का कोई महत्व भी नहीं रहा था, फिर भी तीसरी टर्म में हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए बहुमत जुटा तो लिया गया, लेकिन तब तक जनता के बीच अविश्वास, संत्रास और घुटन इतना अधिक बढ़ गया था कि फुज़िमोरी के दमन-तंत्र और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनाक्रोश जोर पकड़ने लगा। फुज़िमोरी को भाग कर जापान में शरण लेनी पड़ी। नई सरकार बनी और कोर्ट ने कई-कई मुकद्दमों की सुनवाई कर उसे पच्चीस साल की सजा सुनाई। पेरू सरकार के बार-बार आग्रह करने पर भी जापान ने फुज़िमोरी का प्रत्यर्पण करने से इनकार कर दिया। लेकिन 2005 में चिली-यात्रा के दौरान उसे कैद कर जेल में डाल दिया गया।
यह पुस्तक इस प्रश्न पर भी विचार करती है कि क्यों तानाशाह जनता के बीच लोकप्रिय होता है।
लच्छेदार वक्तृता शैली, जनता के मनोविज्ञान पर गहरी पकड़, भावनाओं का दोहन कर भय, उन्माद और घृणा भड़काने की क्षमता, स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाने और हवाई किले बांधने का कौशल, और स्वयं को जनता का समर्पित सेवक बताने की विनम्रता – ये कुछ सस्ते नुस्ख़े हैं जो तानाशाह के मुकुट का कोहिनूर बनते हैं। लेखक-द्वय अमरीकी राजनीति में विघटनकारी तत्वों की शिनाख्त करते समय 1978 में सीनेटर बने न्यूट गिंग्रिश पर दृष्टि केंद्रित करते हैं जो सदन में गाली-गलौजयुक्त अमर्यादित हिंसक भाषा के प्रयोग के लिए जाना जाता रहा है। उसकी दूसरी विशेषता थी – गोपैक नमक एक्शन कमेटी का गठन जो युवा कार्यकर्ताओं को हिंसा, नफरत और उन्माद का प्रशिक्षण देती थी। ये दोनों विशिष्टताएं ध्रुवीकरण की राजनीति को मजबूत करने में सफल रहीं। ध्रुवीकरण के दुष्परिणामों को दिखाने के लिए लेखक दो सर्वेक्षणों का उल्लेख करते हैं। सर्वेक्षण में पूछा गया, यदि आपके बच्चे किसी दूसरे राजनीतिक दल के समर्थक से विवाह करते हैं तो कैसा लगेगा? 1960 के सर्वेक्षण में चार प्रतिशत डेमोक्रेट्स और पांच प्रतिशत रिपब्लिन्स ने कहा कि उन्हें बुरा लगेगा, जबकि 2010 तक आते-आते यह प्रतिशत बढ़कर क्रमशः 35 और 49 हो गया। यानी लोकतंत्र का अपहरण कर तानाशाह समाज को देता है – अविश्वास, डर, घृणा, तनाव, संत्रास और सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता। तो सवाल उठता है कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए? लेखक-द्वय के पास इसका कोई रेडीमेड समाधान नहीं है। सिर्फ आशाएं और मंगलकामनाएँ हैं कि सभी राजनीतिक दल लोकतंत्र की रक्षा के लिए आत्म-सजग हो जाएं। दूसरे, राजनीतिज्ञों को देश की परंपरा और इतिहास का अवगाहन कर जानना चाहिए कि लोकतंत्र हमेशा दो मूल्यों पर केंद्रित रहता है – परस्पर उदारता और सांस्थानिक संयम। पारस्परिक उदारता यानी यह मान्यता कि विपक्षी दल हमारा प्रतिद्वंदी है, शत्रु नहीं। सांस्थानिक संयम का अर्थ है सहिष्णुता एवं आत्म-संयम। यानी लोकतंत्र को ऐसा खेल माना जाए जिसे हम अनंत काल तक खेलते रहना चाहते हैं। इसलिए जरूरी है कि पारस्परिक भाव से दोनों पालों के खिलाड़ियों की सुरक्षा और संतुलन का ख्याल रखा जाए। तीसरे, अतीत से सबक लेकर नई कूटनीतियाँ बनाना। चूँकि तानाशाही से लड़ाई जनता नहीं, विरोधी राजनीतिक दल ही लड़ सकते हैं, अतः उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि तानाशाही-लक्षणों से युक्त किसी भी उम्मीदवार को टिकट न दें। चौथे, यदि पार्टी में पनप रहे चरमपंथी तत्वों का सुराग मिलता है तो निर्ममतापूर्वक उनकी छंटनी करें। इससे पार्टी के जनाधार को थोड़ा नुकसान तो होगा, लेकिन देश को तानाशाह से बचाया जा सकेगा। इतिहास साक्षी है कि 1930 के दशक में स्वीडन ने ऐसा ही कड़ा कदम उठाकर कट्टरपंथियों का मुकाबला किया था। पांचवे, लोकतंत्र-समर्थक दलों को लोकतंत्र-विरोधी दलों और उम्मीदवारों के साथ किसी भी किस्म का गठबंधन नहीं करना चाहिए। तानाशाह के खिलाफ संगठित लड़ाई लड़ने के लिए विचारधारात्मक मतभेदों को भूलकर सभी विपक्षी राजनीतिक दलों को गठबंधन करना चाहिए। विपक्ष की सजगता और निरंकुश सत्ता से सांगठनिक दूरी जनता के बीच लोकतंत्र के पुनरुत्थान की गहरी आश्वस्ति पैदा करती है। जैसे 1920 के दशक में बेल्जियम और फिनलैंड में तथा 2016 में आस्ट्रिया के तानाशाह विरोधी राजनीतिक दलों ने आपसी मतभेद बुलाकर लोकतंत्र के पक्ष में संगठित लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। छठे, लोकतंत्र-समर्थक दलों को सजग रहना चाहिए कि वे ऐसा कोई काम/ बयान न दें जो चरमपंथी नेता की निरंकुश छवि को “सामान्य” बनाने या समर्थन देने का काम करती हो, जैसे 1930 के दशक के आरंभ में हिटलर के साथ जर्मनी के रूढ़िपंथियों की संयुक्त रैलियाँ या चावेज़ से सहानुभूति दर्शाने वाला काल्डेरा का भाषण।
लेकिन लोकतंत्र की रक्षा का अंतिम दायित्व तो स्वयं लोक का है – मताधिकार का सजग-सतर्क विवेकशील प्रयोग। प्लेटो की आशंका में छुपे भयावह सत्य से उसे कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही लोकतंत्र के अतिरिक्त किसी अन्य विकल्प को भी प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र ही उसे नागरिक, चेतन, स्वायत्त और समान मनुष्य बनता है। जाति, वर्ग, वर्ण, रंगभेद जैसे अमानुषिक विभाजन में बांटकर खंडित नहीं करता। इसलिए उसे वोट की अपील करते छद्म तानाशाहों द्वारा बार-बार बरगलाए जाने वाली लच्छेदार भावोत्तेजक भाषण-शैली से परहेज करना चाहिए जो जनशक्ति का सम्मान करने की आड़ में संविधान को बदलने की प्रचंड मंशा मन में पाले हुए हैं – “संविधान से ज्यादा ताकतवर एक चीज है … वह है आपकी (जनता की) इच्छा-शक्ति। वैसे भी संविधान होता क्या है? वह तो जनता की ही पैदा की हुई चीज है। सत्ता का पहला स्रोत जनता है, और अगर लोग चाहें तो संविधान को खत्म कर सकते हैं।”
यह लोक-लुभावन प्रलोभन दरअसल व्यक्ति को भेड़ और भीड़ में बदलने की साज़िश है, और लोकतंत्र व्यक्ति की नागरिक चेतना। समय की नब्ज़ पर उंगली रखे रहने के लिए ज़रूरी है कि इस किताब के सबक को कलियुग की सुमिरनी की तरह दिन-रात फिराया जाए।
पुस्तकः लोकतंत्र की चौकीदारी
लेखक- स्टीवेन लेवित्सकी
डेनियल ज़िब्लाट
अनुवाद- अभिषेक श्रीवास्तव
राजकमल प्रकाशन